UPSC Daily Current Affairs(Hindi): 29th November 2024 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly PDF Download
जीएस2/राजनीति
विकिपीडिया और ANI का मानहानि का मुकदमा
स्रोत: द हिंदू
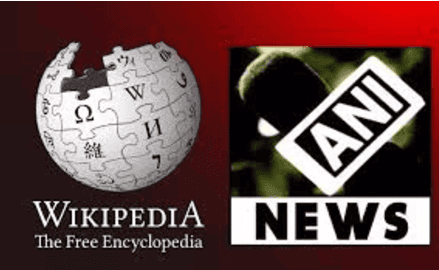
चर्चा में क्यों?
2024 की शुरुआत में, भारतीय समाचार एजेंसी एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल (एएनआई) ने विकिमीडिया फ़ाउंडेशन और तीन विकिपीडिया प्रशासकों के खिलाफ़ मानहानि का मुकदमा दायर किया। एएनआई ने दावा किया कि उसके विकिपीडिया पेज पर अपमानजनक बयानों ने उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने विकिमीडिया को इन प्रशासकों की पहचान उजागर करने का आदेश दिया है, जो मामले में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है।
एएनआई द्वारा लगाए गए मुख्य आरोप:
- मानहानिकारक बयान: एएनआई ने दावा किया कि उसके विकिपीडिया पृष्ठ पर निम्नलिखित आरोप लगाए गए हैं:
- केंद्र सरकार के लिए प्रचार साधन के रूप में कार्य करना।
- अविश्वसनीय समाचार साइटों से सामग्री फैलाना।
- घटनाओं को गलत ढंग से प्रस्तुत करना।
- संपादन संबंधी मुद्दे: एएनआई से जुड़े संपादकों द्वारा इन बयानों को सही करने के प्रयासों को या तो वापस ले लिया गया या स्वतंत्र संपादकों द्वारा इसमें बदलाव किया गया। इसके बाद, पेज को 'विस्तारित पुष्टि संरक्षण' के तहत रखा गया, जिसने एएनआई से जुड़े संपादकों द्वारा आगे संपादन को सीमित कर दिया।
- कानूनी आरोप: एएनआई ने तर्क दिया कि विकिमीडिया ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और आईटी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत सुरक्षित-बंदरगाह प्रावधानों का उल्लंघन किया है। उन्होंने अपमानजनक सामग्री के प्रसार के लिए विकिमीडिया और उसके प्रशासकों को जवाबदेह ठहराने की मांग की।
विकिपीडिया कैसे काम करता है?
- समुदाय-संचालित मंच: विकिपीडिया मुख्य रूप से स्वयंसेवकों द्वारा प्रबंधित किया जाता है जो सामग्री बनाते और संपादित करते हैं। इसकी संरचना में शामिल हैं:
- संपादकीय प्रक्रिया: कोई भी व्यक्ति लेखों को संपादित कर सकता है, बशर्ते कि उनके योगदान विश्वसनीय और सत्यापन योग्य स्रोतों द्वारा समर्थित हों। मूल शोध की अनुमति नहीं है, और अप्रकाशित तर्क या विश्लेषण हटा दिए जाते हैं।
- संपादन इतिहास: प्रत्येक पृष्ठ का संपादन इतिहास पारदर्शी है और इसे "इतिहास देखें" टैब के माध्यम से देखा जा सकता है।
- सुरक्षा उपाय: तटस्थता बनाए रखने के लिए विवादास्पद विषयों को 'पूर्ण सुरक्षा' के अंतर्गत रखा जा सकता है। 'विस्तारित सुरक्षा' संपादन को अनुभवी उपयोगकर्ताओं तक सीमित करती है, जबकि 'पूर्ण सुरक्षा' संपादन को केवल प्रशासकों तक सीमित रखती है।
- नियम और जिम्मेदारियाँ:
- प्रशासक: इनका चुनाव समुदाय द्वारा उनकी प्रतिष्ठा के आधार पर किया जाता है, तथा विकिमीडिया इनके चयन में कोई भूमिका नहीं निभाता है।
- विकिमीडिया की भूमिका: संगठन मंच के लिए तकनीकी ढांचा प्रदान करता है और संपादकों को समर्थन देता है, लेकिन सामग्री प्रबंधन में हस्तक्षेप नहीं करता है।
कानूनी एवं संरचनात्मक निहितार्थ:
- सुरक्षित बंदरगाह स्थिति: यह कानूनी प्रावधान विकिमीडिया जैसे मध्यस्थों को उपयोगकर्ता द्वारा निर्मित सामग्री के लिए उत्तरदायी होने से बचाता है। ANI के मुकदमे में इस स्थिति को चुनौती दी गई है, जिससे संभवतः विकिमीडिया विकिपीडिया की सामग्री के लिए उत्तरदायी हो सकता है।
- विकिपीडिया पर प्रभाव:
- गुमनामी की हानि: यदि संपादकों का विवरण उजागर हो जाता है, तो इससे प्रतिक्रिया के भय से स्वयंसेवक योगदान देने से हतोत्साहित हो सकते हैं।
- वैश्विक मिसालें: चीन, रूस और पाकिस्तान जैसे देशों ने विकिपीडिया पर सेंसरशिप लगा दी है, और भारत में भी इसी तरह की कार्रवाई से इसकी लोकतांत्रिक छवि को नुकसान पहुंच सकता है।
- प्रारंभिक निर्देश: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आरंभ में विकिमीडिया को अपने प्रशासकों का विवरण सीलबंद लिफाफे में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था।
- संभावित अवरोधन: न्यायालय ने संकेत दिया है कि उसके आदेशों का पालन न करने पर भारत में विकिपीडिया को अवरुद्ध किया जा सकता है।
व्यापक निहितार्थ:
- लोकतंत्र पर प्रभाव: विकिपीडिया का खुला और लोकतांत्रिक ढांचा मुक्त ज्ञान साझाकरण को बढ़ावा देता है। कोई भी न्यायिक या विधायी हस्तक्षेप इस सिद्धांत को खतरे में डाल सकता है।
- भारत की प्रतिक्रिया: भारत इस मामले को किस प्रकार से संभालता है, यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच संतुलन बनाने के उसके दृष्टिकोण को प्रदर्शित करेगा।
- अन्य देशों के साथ तुलना: अन्य देशों ने विकिपीडिया के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कदम उठाए हैं, जिसके कारण सेंसरशिप की स्थिति पैदा हुई है। भारत के भी इन प्रवृत्तियों के अनुरूप होने का जोखिम है।
निष्कर्ष:
यह मानहानि का मामला मध्यस्थ दायित्व, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विकिपीडिया जैसे समुदाय-संचालित प्लेटफ़ॉर्म के संचालन के बारे में आवश्यक प्रश्न उठाता है। जबकि ANI जवाबदेही चाहता है, विकिपीडिया के कामकाज और भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए व्यापक परिणाम महत्वपूर्ण हैं। विकिपीडिया जैसे प्लेटफ़ॉर्म की जवाबदेही और खुले चरित्र दोनों को बनाए रखने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण आवश्यक है।
जीएस2/शासन
जनगणना 2025 एक व्यापक नागरिक रजिस्ट्री के रूप में
स्रोत: द हिंदू
चर्चा में क्यों?
2025 की जनगणना एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय अभ्यास है जो राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को अद्यतन करने को एकीकृत करता है। यह भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरआईसी) की स्थापना की दिशा में पहला कदम है, जो नागरिकों को गैर-नागरिकों से अलग करने के लिए डिज़ाइन की गई एक आवश्यक पहल है, जिससे शासन और सुरक्षा के लिए एक ठोस ढांचा तैयार होता है। एनआरआईसी की उत्पत्ति, लक्ष्यों, प्रक्रियाओं और चुनौतियों की जांच करना महत्वपूर्ण है, साथ ही इसके कार्यान्वयन, डेटा गोपनीयता और बहिष्कार की संभावना से संबंधित चिंताओं को भी संबोधित करना है।
एनआरआईसी का ऐतिहासिक संदर्भ और विधायी आधार
- एनआरआईसी का विचार 1955 के नागरिकता अधिनियम से निकला है, जिसकी संकल्पना 1951 की जनगणना के बाद की गयी थी।
- 1999 में कारगिल युद्ध के बाद इस पर पुनः ध्यान दिया गया, जब सुब्रह्मण्यम समिति ने राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नागरिकों और गैर-नागरिकों का एक व्यापक डाटाबेस तैयार करने की वकालत की।
- इसके परिणामस्वरूप अधिनियम में धारा 14ए को शामिल किया गया, जिसके तहत नागरिक पंजीकरण और पहचान पत्र जारी करना अनिवार्य कर दिया गया।
- बहुउद्देश्यीय राष्ट्रीय पहचान पत्र (एमएनआईसी) और मछुआरा पहचान पत्र जैसी अनेक पायलट परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जो कार्यान्वयन चुनौतियों के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं।
एनआरआईसी के उद्देश्य और लाभ
- राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाना: NRIC का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय नागरिकों की सत्यापित रजिस्ट्री बनाए रखकर राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है। अवैध आव्रजन और पहचान धोखाधड़ी से भरे युग में, NRIC एक सुरक्षात्मक उपाय के रूप में कार्य करता है, जो संभावित सुरक्षा खतरों की पहचान करने के लिए नागरिकों को गैर-नागरिकों से स्पष्ट रूप से अलग करता है।
- पहचान सत्यापन को सरल बनाना: एक और महत्वपूर्ण लक्ष्य एक एकीकृत पहचान सत्यापन प्रणाली बनाना है, जिससे कई दस्तावेजों पर निर्भरता कम हो। यह एकरूपता नागरिकता की स्थिति को स्पष्ट करने में मदद करती है, जो कानूनी विवादों और संपत्ति के दावों में महत्वपूर्ण है।
- लक्षित कल्याण कार्यक्रमों को सुविधाजनक बनाना: एनआरआईसी यह सुनिश्चित करके कल्याणकारी योजनाओं की दक्षता बढ़ा सकता है कि संसाधन लक्षित लाभार्थियों तक पहुँचें। नागरिकों की सटीक पहचान सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को रोकने में मदद करती है, यह सुनिश्चित करती है कि सब्सिडी जैसे लाभ पात्र व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं।
- इसके अलावा, एक अच्छी तरह से क्रियान्वित एनआरआईसी एक विश्वसनीय और सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त पहचान दस्तावेज प्रदान करके शासन में जनता के विश्वास को बढ़ावा दे सकता है, तथा नागरिक सहभागिता को बढ़ा सकता है।
एनपीआर-एनआरआईसी प्रक्रिया और आधार बनाम एनआरआईसी बहस
- एनआरआईसी निर्माण प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं, जो जनगणना मकान सूचीकरण के दौरान जनसांख्यिकीय डेटा संग्रह से शुरू होता है, इसके बाद सटीकता के लिए बायोमेट्रिक डेटा संग्रह किया जाता है।
- एक महत्वपूर्ण पहलू में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक दावे और आपत्तियां आमंत्रित करना शामिल है, साथ ही निवासियों के लिए रिकॉर्ड को चुनौती देने या संशोधित करने हेतु सत्यापन प्रक्रिया भी शामिल है।
- नागरिकता स्थिति का सत्यापन किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप नागरिकता अधिनियम के अनुसार पहचान पत्र जारी किए जाते हैं।
- 2025 की जनगणना में संभवतः 2011 की जनगणना के डेटा संग्रहण पैटर्न को दोहराया जाएगा, जिसमें नाम, लिंग, राष्ट्रीयता और निवास जैसे जनसांख्यिकीय विवरण शामिल होंगे, हालांकि बायोमेट्रिक डेटा को छोड़ा जा सकता है क्योंकि यह पहले से ही आधार डेटाबेस में उपलब्ध है।
- एक आम सवाल यह है कि मौजूदा आधार प्रणाली के मद्देनजर NRIC की क्या ज़रूरत है। आधार सभी निवासियों को, चाहे उनकी नागरिकता कुछ भी हो, एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करता है, मुख्य रूप से सेवा तक पहुँच के लिए। इसके विपरीत, NRIC नागरिकता सत्यापन उपकरण के रूप में कार्य करता है, जिसके लिए नागरिकता के प्रमाण की आवश्यकता होती है और यह नागरिकों के लिए एक निश्चित रिकॉर्ड के रूप में कार्य करता है।
राष्ट्रव्यापी एनआरआईसी कार्यान्वयन की चुनौतियाँ:
- दस्तावेज़ीकरण संबंधी चुनौतियाँ: कई व्यक्तियों के पास, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, अपनी नागरिकता स्थापित करने के लिए उचित दस्तावेज़ों का अभाव हो सकता है, जो कि आदिवासी समुदायों और महिलाओं जैसे हाशिए पर पड़े समूहों के लिए विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण है।
- गोपनीयता और डेटा सुरक्षा: राष्ट्रव्यापी एनआरआईसी के लिए संवेदनशील जनसांख्यिकीय डेटा की विशाल मात्रा का संग्रह और प्रबंधन आवश्यक होगा, जिससे मजबूत सुरक्षा कानूनों के बिना डेटा के दुरुपयोग और अनधिकृत पहुंच के बारे में महत्वपूर्ण चिंताएं पैदा होंगी।
- बहिष्कार की आशंका: बड़े पैमाने पर सत्यापन से कमजोर आबादी अलग-थलग पड़ सकती है, जिससे सामाजिक अशांति और कानूनी चुनौतियां पैदा हो सकती हैं, जिससे एक समावेशी और पारदर्शी प्रक्रिया की आवश्यकता पर प्रकाश पड़ता है।
आगे बढ़ने का रास्ता
- कार्यान्वयन की चुनौतियों पर असम से सबक: असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के अनुभव से मूल्यवान सबक मिलते हैं। एनआरसी का उद्देश्य अवैध अप्रवासियों की पहचान करना था, लेकिन सख्त दस्तावेज़ आवश्यकताओं के कारण कई ग्रामीण निवासी इससे बाहर हो गए, जिससे निष्पक्षता और सटीकता को लेकर चिंताएँ पैदा हुईं।
- गोपनीयता संबंधी चिंताओं का समाधान: न्यायिक दिशा-निर्देशों के बावजूद गोपनीयता संबंधी मुद्दे महत्वपूर्ण बने हुए हैं। जनसांख्यिकीय डेटा के संभावित दुरुपयोग के कारण कड़े डेटा सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है।
- नागरिक सहभागिता और आगे बढ़ना: एनआरआईसी की सफलता के लिए नागरिकों की सक्रिय भागीदारी बहुत ज़रूरी है। जन जागरूकता अभियानों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी निवासियों को सूचित किया जाए और वे इस प्रक्रिया में शामिल हों, ताकि एनआरआईसी को समावेशी और प्रभावी बनाने के लिए बहिष्कार के डर को दूर किया जा सके।
निष्कर्ष:
- 2025 की जनगणना और एनआरआईसी पहल एक सत्यापित नागरिक रजिस्ट्री स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। हालाँकि यह बेहतर प्रशासन और राष्ट्रीय सुरक्षा का वादा करता है, लेकिन डेटा गोपनीयता, बहिष्कार और तार्किक निष्पादन से जुड़ी चुनौतियों को नज़रअंदाज़ नहीं किया जाना चाहिए।
- असम के अनुभव से सीखना तथा पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना सफलता के लिए महत्वपूर्ण होगा।
जीएस2/शासन
अमृत 2.0 की मुख्य विशेषताएं
स्रोत: पीआईबी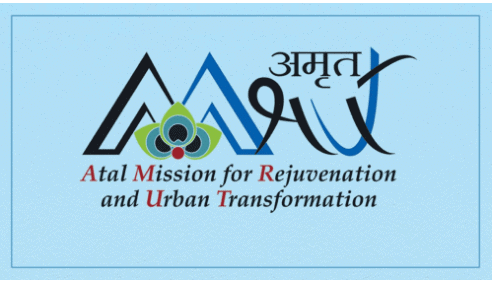
चर्चा में क्यों?
कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत) 2.0 1 अक्टूबर, 2021 को शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य भारतीय शहरों को आत्मनिर्भर और जल-सुरक्षित शहरी क्षेत्रों में बदलना है।
- यह मिशन मूल अमृत योजना का ही विस्तार है, जिसे जून 2015 में केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था।
- इसका प्राथमिक उद्देश्य शहरी बुनियादी ढांचे को बढ़ाना और शहरों और कस्बों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।
- इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक घर को विश्वसनीय नल जल आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन उपलब्ध हो।
- एक अन्य लक्ष्य शहरी क्षेत्रों में हरित क्षेत्रों को बढ़ाना तथा सार्वजनिक परिवहन और गैर-मोटर चालित परिवहन सुविधाओं को बढ़ावा देकर प्रदूषण को कम करना है।
- मिशन के लिए धनराशि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच समान फार्मूले के आधार पर 50:50 के अनुपात में आवंटित की जाती है, जिसमें 500 शहर और 100,000 से अधिक जनसंख्या वाले सभी नगर पालिकाएं शामिल हैं।
अमृत 2.0 के बारे में
- 1 अक्टूबर, 2021 को AMRUT 1.0 के उत्तराधिकारी के रूप में लॉन्च किया गया।
- मिशन का ध्यान शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार, विशेष रूप से अपशिष्ट जल प्रबंधन और जल निकायों के पुनरुद्धार पर केंद्रित है।
- मिशन की अवधि पांच वर्ष निर्धारित की गई है, जो वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक चलेगी।
मुख्य विशेषताएं और मिशन
- सार्वभौमिक कवरेज: इसका लक्ष्य 500 शहरों और 4,900 वैधानिक कस्बों में व्यापक जल आपूर्ति और सीवेज सेवाएं प्रदान करना है।
- चक्रीय अर्थव्यवस्था: जल पुनर्चक्रण, उपचारित मलजल का पुनः उपयोग और जल संरक्षण पर जोर देती है।
- प्रौद्योगिकी एकीकरण: उन्नत जल प्रबंधन प्रथाओं के लिए वैश्विक प्रौद्योगिकियों को शामिल किया गया है।
- पेयजल सर्वेक्षण: जल वितरण, अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग का मूल्यांकन करने तथा शहरों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया सर्वेक्षण।
इसका कार्यान्वयन और आगे की रूपरेखा
- परियोजना अनुमोदन: कुल 8,998 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनका अनुमानित व्यय 1,89,458.55 करोड़ रुपये है।
- धन वितरण: आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय (MoHUA) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को धन जारी करता है, जिसे बाद में शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को आवंटित किया जाता है।
- राज्य जल कार्य योजना (एसडब्ल्यूएपी): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मिशन के शुभारंभ के दो वर्ष के भीतर अपनी एसडब्ल्यूएपी पूरी करनी होगी तथा अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- भविष्य की योजनाएं: सतत जल प्रबंधन और अमृत 1.0 के लाभों को अतिरिक्त शहरों तक पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
जीएस3/रक्षा एवं सुरक्षा
के-4 बैलिस्टिक मिसाइल
स्रोत: इकोनॉमिक टाइम्स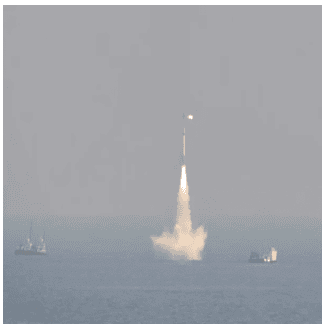
चर्चा में क्यों?
हाल ही में भारत ने विशाखापत्तनम तट पर स्थित पनडुब्बी आईएनएस अरिघाट से प्रक्षेपित K-4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया।
K-4 बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में:
- के-4 एक परमाणु-सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है।
- इसकी प्रभावशाली परिचालन सीमा लगभग 3,500 किलोमीटर है।
- यह मिसाइल ठोस ईंधन से चलती है, जिससे तीव्र प्रक्षेपण क्षमता प्राप्त होती है।
- हाल के वर्षों में जलमग्न प्लेटफार्मों पर इसका कम से कम पांच बार परीक्षण किया जा चुका है।
- के-4 मिसाइल के सफल प्रक्षेपण से भारत की परमाणु त्रिकोण शक्ति मजबूत हुई है, जिसमें भूमि आधारित मिसाइलें, हवा से प्रक्षेपित परमाणु हथियार और पनडुब्बी से प्रक्षेपित प्रणालियां शामिल हैं।
- के-4 मिसाइल का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा किया गया है।
महत्व:
- के-4 मिसाइल भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता और सामरिक सैन्य क्षमताओं में महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करती है।
आईएनएस अरिघाट के बारे में मुख्य तथ्य:
- आईएनएस अरिघाट को अगस्त 2024 में कमीशन किया जाएगा।
- यह आईएनएस अरिहंत के बाद भारत की दूसरी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी (एसएसबीएन) है।
- इस पनडुब्बी का निर्माण विशाखापत्तनम स्थित भारतीय नौसेना के जहाज निर्माण केंद्र (एसबीसी) में किया गया था।
- आईएनएस अरिघाट चार परमाणु-सक्षम K-4 पनडुब्बी-प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइलों (SLBMs) को ले जा सकता है, जिनमें से प्रत्येक की सीमा 3,500 किलोमीटर से अधिक है।
- वैकल्पिक रूप से, इसमें बारह पारंपरिक K-15 SLBMs को रखा जा सकता है, जिनकी रेंज लगभग 750 किलोमीटर है।
जीएस3/पर्यावरण
साइबेरियाई युवती खोपड़ी
स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया
चर्चा में क्यों?
साइबेरियाई डेमोइसेल क्रेन, जिसे प्यार से सुकपैक नाम दिया गया है, ने भारत के राजस्थान तक सबसे लम्बी प्रवासी उड़ान पूरी करके एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है, जिसमें उसने 3,676 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की है।
साइबेरियाई डेमोइसेल क्रेन के बारे में:
- यह प्रजाति सारसों में सबसे छोटी है और एकान्त तथा सामाजिक दोनों प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करती है।
- भारतीय संस्कृति में इस पक्षी का प्रतीकात्मक महत्व है और इसे आमतौर पर कूंज या कुरजा कहा जाता है।
- ये सारस अपनी प्रवासी प्रकृति के लिए जाने जाते हैं, जो अपने प्रजनन और शीतकालीन आवासों के बीच काफी दूरी तय करते हैं।
प्राकृतिक वास:
- साइबेरियाई डेमोइसेल क्रेन खेतों, रेगिस्तानों, मैदानों और मैदानों जैसे आवासों को पसंद करते हैं, जो आमतौर पर जल स्रोतों के पास पाए जाते हैं।
वितरण:
- ये सारस मुख्य रूप से मध्य यूरो साइबेरिया में पाए जाते हैं, तथा इनका क्षेत्र काला सागर से लेकर मंगोलिया और पूर्वोत्तर चीन तक फैला हुआ है।
प्रजनन क्षेत्र:
- वे मध्य यूरेशिया में, विशेष रूप से काला सागर क्षेत्र से लेकर उत्तर-पूर्व चीन और मंगोलिया तक प्रजनन करते हैं।
- सर्दियों के दौरान, वे भारतीय उपमहाद्वीप और उप-सहारा अफ्रीका की ओर प्रवास करते हैं।
- जबकि अधिकांश डेमोइसेल क्रेन आमतौर पर नेपाल के रास्ते हिमालय की घाटियों से होते हुए भारत में आते हैं, सुकपाक ने जैसलमेर के रास्ते भारत पहुंचने से पहले रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होकर एक अनोखा मार्ग अपनाया।
भारत में संरक्षण प्रयास:
- खीचन राजस्थान में प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव बन गया है और इसे भारत का पहला रिजर्व माना जाता है जो विशेष रूप से साइबेरियन डेमोइसेल क्रेन को समर्पित है।
संरक्षण स्थिति IUCN:
- साइबेरियाई डेमोइसेल क्रेन की संरक्षण स्थिति को IUCN द्वारा न्यूनतम चिंताजनक श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।
खतरे:
- इन सारसों को विभिन्न खतरों का सामना करना पड़ता है, जिनमें आर्द्रभूमि का जल निकास, आवास का विनाश, अवैध पालतू व्यापार और शिकार का दबाव शामिल हैं।
जीएस1/भूगोल
बाल्टिक सागर
स्रोत: न्यूयॉर्क टाइम्स

चर्चा में क्यों?
स्वीडिश प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समुद्र के नीचे केबलों से जुड़ी एक संदिग्ध तोड़फोड़ की घटना के बाद बाल्टिक सागर को "उच्च जोखिम" वाला क्षेत्र घोषित किया है। यह घोषणा नॉर्डिक और बाल्टिक देशों के नेताओं के साथ एक बैठक के दौरान की गई। प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र में दो फाइबर ऑप्टिक टेलीकॉम केबलों को नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार संभावित अपराधियों के बारे में अटकलें लगाने से परहेज किया। उल्लेखनीय है कि एक चीनी जहाज, यी पेंग 3, केबलों को काटे जाने के समय उनके पास मौजूद था और तब से 19 नवंबर से स्वीडन और डेनमार्क के बीच स्थित कैटेगट जलडमरूमध्य में लंगर डाले हुए है।
बाल्टिक सागर के बारे में
- बाल्टिक सागर अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है, जो दक्षिणी डेनमार्क से उत्तर की ओर आर्कटिक सर्कल की ओर फैला हुआ है।
- यह स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप और महाद्वीपीय यूरोप के बीच एक प्राकृतिक विभाजक के रूप में कार्य करता है।
सीमाएँ:
- पश्चिम: डेनमार्क और कैटेगाट जलडमरूमध्य से घिरा हुआ है, जो स्केगररक के माध्यम से उत्तरी सागर से जुड़ता है।
- उत्तर: स्वीडन और बोथनिया की खाड़ी से घिरा हुआ।
- पूर्व: इसमें फिनलैंड, रूस और फिनलैंड की खाड़ी शामिल हैं।
- दक्षिण: इसमें जर्मनी, पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया शामिल हैं।
बाल्टिक सागर के किनारे स्थित देश:
- डेनमार्क
- एस्तोनिया
- फिनलैंड
- जर्मनी
- लातविया
- लिथुआनिया
- पोलैंड
- रूस
- स्वीडन
बाल्टिक सागर की विशेषताएँ:
- बाल्टिक सागर का पानी खारा है, जो उत्तरी सागर के साथ सीमित जल विनिमय और नदियों से महत्वपूर्ण मात्रा में मीठे पानी के प्रवाह के कारण है।
- समुद्र तट पर ऊबड़-खाबड़ परिदृश्य है जिसमें अनेक द्वीप, प्रायद्वीप और उल्लेखनीय खाड़ियाँ हैं, जिनमें बोथनिया की खाड़ी और फिनलैंड की खाड़ी शामिल हैं।
बाल्टिक सागर में बहने वाली प्रमुख नदियाँ:
- विस्तुला नदी (पोलैंड)
- या नदी (जर्मनी/पोलैंड)
- नेवा नदी (रूस)
- दौगावा नदी (लातविया)
शिपिंग और व्यापार:
- बाल्टिक सागर एक महत्वपूर्ण शिपिंग मार्ग के रूप में कार्य करता है जो मध्य और पूर्वी यूरोप को वैश्विक बाज़ार से जोड़ता है।
- ग्दान्स्क (पोलैंड), तेलिन (एस्टोनिया) और सेंट पीटर्सबर्ग (रूस) जैसे प्रमुख बंदरगाह व्यापार गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- स्टॉकहोम, हेलसिंकी और रीगा जैसे तटीय रिसॉर्ट और ऐतिहासिक शहर हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।
जीएस2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध
AUKUS क्या है?
स्रोत: द हिंदू
चर्चा में क्यों?
न्यूजीलैंड में चीनी राजदूत ने चेतावनी दी है कि AUKUS में न्यूजीलैंड की भागीदारी से चीन के साथ उसके संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
AUKUS 2021 में यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच गठित एक त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी है। इसका प्राथमिक उद्देश्य इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में प्रौद्योगिकी साझाकरण को बढ़ाना है। इस गठबंधन को इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में चीनी आक्रामकता और उसकी आकांक्षाओं का मुकाबला करने के उद्देश्य से एक रणनीतिक प्रतिक्रिया के रूप में माना जाता है।
यह साझेदारी दो मुख्य स्तंभों पर आधारित है:
- स्तंभ 1: AUKUS ऑस्ट्रेलिया को पारंपरिक रूप से सशस्त्र, परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों का पहला बेड़ा प्राप्त करने में सहायता करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समझौते में ऑस्ट्रेलिया को परमाणु हथियार हस्तांतरित करने की बात नहीं है।
- स्तंभ 2: यह स्तंभ आठ उन्नत सैन्य क्षमताओं में सहयोग पर केंद्रित है, जिनमें शामिल हैं:
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)
- क्वांटम टेक्नोलॉजीज
- नवाचार
- जानकारी साझाकरण
- साइबर संचालन
- पानी के नीचे का युद्ध
- हाइपरसोनिक और काउंटर-हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकियां
- इलेक्ट्रानिक युद्ध
पनडुब्बी घटक: AUKUS का लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली हमलावर पनडुब्बियों (SSN) से लैस करना है। ऑस्ट्रेलिया को कुल मिलाकर नई परमाणु पनडुब्बियाँ मिलने की उम्मीद है, जिन्हें SSN-AUKUS नाम दिया गया है। ये पनडुब्बियाँ ब्रिटिश डिज़ाइन पर आधारित होंगी, लेकिन इनमें अमेरिकी तकनीक और लड़ाकू प्रणाली शामिल होंगी।
AUKUS के परिणामस्वरूप, ऑस्ट्रेलिया विश्व स्तर पर परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों वाला सातवाँ देश बन जाएगा, यूनाइटेड किंगडम के बाद, जो दूसरा देश है (यूके के बाद) जिसके साथ संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस तकनीक को साझा किया है। यह साझेदारी इंडो-पैसिफिक में ऑस्ट्रेलिया की समुद्री क्षमताओं में उल्लेखनीय रूप से सुधार करेगी, यह देखते हुए कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियाँ निम्नलिखित लाभ प्रदान करती हैं:
- विस्तारित परिचालन सीमा
- अधिक सहनशीलता
- उन्नत गुप्त क्षमताएं
इन प्रगतियों के बावजूद, शामिल देशों ने स्पष्ट किया है कि उनका इरादा नई पनडुब्बियों को हथियारबंद करने का नहीं है, क्योंकि वे परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में ऑस्ट्रेलिया की प्रतिबद्धता का पालन कर रहे हैं, जो परमाणु हथियारों के अधिग्रहण या तैनाती पर प्रतिबंध लगाती है।
जीएस2/शासन
जापानी इन्सेफेलाइटिस क्या है?
स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स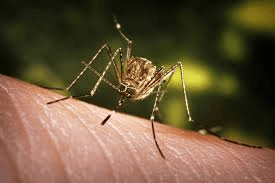
चर्चा में क्यों?
आधिकारिक सूत्रों ने हाल ही में बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में जापानी इंसेफेलाइटिस का एक "पृथक" मामला सामने आया है।
जापानी इंसेफेलाइटिस के बारे में:
- जापानी इंसेफेलाइटिस एक संभावित गंभीर वायरल जूनोटिक रोग है जो जापानी इंसेफेलाइटिस (बी) वायरस के कारण होता है।
हस्तांतरण
- यह वायरस पशुओं, विशेषकर सूअरों और आर्डेइडे परिवार के पक्षियों, जैसे कि मवेशी बगुले और तालाब बगुले से, विष्णुई समूह के क्यूलेक्स मच्छर के काटने के माध्यम से मनुष्यों में फैलता है।
- इस वायरस का मानव-से-मानव संचरण नहीं होता है।
- यह रोग एशिया के ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक प्रचलित है, विशेषकर मानसून के मौसम में जब स्थितियाँ मच्छरों के प्रजनन के लिए अनुकूल होती हैं।
लक्षण
- जापानी इंसेफेलाइटिस मुख्य रूप से मस्तिष्क को प्रभावित करता है, जिसके कारण बुखार, सिरदर्द और उल्टी जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं।
- भ्रम, दौरे और पक्षाघात सहित तंत्रिका संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।
- यद्यपि वायरस से संक्रमित कई व्यक्तियों में हल्के लक्षण या कोई लक्षण नहीं दिखाई देते, लेकिन गंभीर मामलों में स्थायी मस्तिष्क क्षति या यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है।
रोकथाम और उपचार:
- जापानी इंसेफेलाइटिस की रोकथाम के लिए टीकाकरण सबसे प्रभावी रणनीति है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां यह रोग स्थानिक है।
- प्रारंभिक निदान और सहायक देखभाल से लक्षणों के प्रबंधन में मदद मिल सकती है, लेकिन इस रोग के लिए कोई विशिष्ट एंटीवायरल उपचार उपलब्ध नहीं है।
- केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, 2013 से टीके की दो खुराकें सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम का हिस्सा रही हैं।
जीएस2/राजनीति
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड
स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स

चर्चा में क्यों?
जम्मू क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि के जवाब में, गृह मंत्रालय (एमएचए) ने जम्मू शहर में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) के लिए एक स्थायी केंद्र स्थापित किया है। इस पहल का उद्देश्य संभावित बड़े हमलों के लिए त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना है। हाल के महीनों में कठुआ, डोडा, किश्तवाड़, उधमपुर, राजौरी, पुंछ और रियासी सहित कई जिलों में आतंकवादी घटनाओं में वृद्धि देखी गई है।
नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिसे अक्सर ब्लैक कैट्स के नाम से जाना जाता है, एक प्रमुख संघीय बल है जिसे आतंकवाद विरोधी अभियानों को सटीकता के साथ संभालने की अपनी क्षमता के लिए जाना जाता है। एनएसजी को विशेष रूप से विशिष्ट स्थितियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित और सुसज्जित किया जाता है और गंभीर आतंकवादी खतरों का मुकाबला करने के लिए केवल महत्वपूर्ण परिदृश्यों में ही तैनात किया जाता है।
गठन और पृष्ठभूमि:
- एनएसजी का गठन 16 अक्टूबर 1984 को आतंकवाद द्वारा उत्पन्न चुनौतियों, विशेषकर ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद उत्पन्न चुनौतियों के प्रत्यक्ष प्रत्युत्तर के रूप में किया गया था।
- यह बल ब्रिटिश स्पेशल एयर सर्विस और जर्मनी के जीएसजी 9 से प्रेरित था।
विधान:
- एनएसजी की स्थापना राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम 1986 के माध्यम से औपचारिक रूप दी गई।
क्षेत्राधिकार:
- एनएसजी भारत के गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
भर्ती:
- एनएसजी के कार्मिक भारतीय सेना और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल दोनों से लिये जाते हैं।
आदर्श वाक्य:
- एनएसजी का आदर्श वाक्य "सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा" है, जिसका अर्थ है "सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा।"
प्रमुख ऑपरेशन:
- 1988: ऑपरेशन ब्लैक थंडर - स्वर्ण मंदिर में आतंकवाद विरोधी अभियान चलाया गया।
- 1999: आईसी-814 अपहरण - इस घटना के दौरान एनएसजी को स्टैंडबाय पर रखा गया था, लेकिन विमान को कंधार, अफगानिस्तान ले जाने के कारण वह हस्तक्षेप करने में असमर्थ रही।
- 2002: अक्षरधाम मंदिर हमला - गुजरात में इस घटना के दौरान एनएसजी ने आतंकवादियों को सफलतापूर्वक निष्प्रभावी कर दिया।
- 2008: मुंबई आतंकवादी हमला (26/11) - एनएसजी ने आतंकवादियों को खत्म करने और ताज होटल और नरीमन हाउस जैसे प्रमुख स्थानों को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
जीएस2/शासन
जारवा जनजाति
स्रोत: निकोबार टाइम्स

चर्चा में क्यों?
एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जारवा जनजाति को मतदाता सूची में पंजीकरण के साथ औपचारिक रूप से भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में एकीकृत किया गया है। जारवा जनजाति के कुल 19 सदस्यों को नामांकित किया गया है, जो इस समुदाय के व्यक्तियों के चुनावी प्रक्रिया में शामिल होने का पहला अवसर है।
- जरावा दक्षिण और मध्य अंडमान द्वीप समूह के पश्चिमी तट पर स्थित एक स्वदेशी जनजाति है। उनकी वर्तमान जनसंख्या 250 से 400 व्यक्तियों के बीच होने का अनुमान है। ऐतिहासिक रूप से, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान उनकी संख्या में नाटकीय कमी आई थी, लेकिन उसके बाद से वे स्थिर हो गए हैं।
- विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के रूप में पहचाने जाने वाले जारवा की पहचान उनकी छोटी आबादी, आदिम तकनीक का उपयोग और मुख्यधारा के समाज से सापेक्ष अलगाव है।
- जारवा जनजाति की अपनी विशिष्ट भाषा है, जो ओन्गान भाषा परिवार से संबंधित है, जो इसे अंडमान द्वीपसमूह में बोली जाने वाली अन्य भाषाओं से अलग करती है।
जीवन शैली:
- शिकारी-संग्राहक: जारवा पारंपरिक रूप से शिकारी-संग्राहक के रूप में रहते हैं। वे जंगली सूअरों और मॉनिटर छिपकलियों का शिकार करने के लिए धनुष और तीर का उपयोग करते हैं, और वे तटीय जल में मछली भी पकड़ते हैं।
- आहार: उनके आहार में जंगली फल, जड़ें, शहद और मछली शामिल हैं। यह जनजाति अपने उत्कृष्ट पोषण स्वास्थ्य और मजबूत शारीरिक स्थिति के लिए जानी जाती है।
- आवास: वे अपने शिविरों के लिए अस्थायी झोपड़ियों का निर्माण करते हैं और नदियों और खाड़ियों को पार करने के लिए साधारण बेड़ों का उपयोग करते हैं।
- बाहरी लोगों से संपर्क:
- ऐतिहासिक अलगाव: ऐतिहासिक रूप से, 1990 के दशक तक जारवा लोग बाहरी लोगों के साथ मेलजोल से बचते रहे।
- हाल की अंतर्क्रियाएं: 1990 के दशक से, स्थायी आबादी के साथ संपर्क में वृद्धि हुई है, तथा कुछ जनजाति सदस्य निकटवर्ती शहरों और बस्तियों में भी जाते हैं।
जीएस3/पर्यावरण
बार-टेल्ड गॉडविट क्या है?
स्रोत: द हिंदू
चर्चा में क्यों?
एक असामान्य घटना में, हाल ही में एक प्रकृतिविज्ञानी ने पुलिकट झील में पांच बार-टेल्ड गॉडविट्स देखे।
बार-टेल्ड गॉडविट के बारे में:
- यह एक प्रवासी समुद्री पक्षी है जो प्रवास के दौरान अपनी उल्लेखनीय सहनशीलता के लिए जाना जाता है।
- वैज्ञानिक नाम: लिमोसा लैपोनिका
वितरण
बार-टेल्ड गॉडविट प्रजाति कहाँ पाई जाती है?
- उत्तरी यूरोप और एशिया
- पश्चिमी अलास्का
- अफ्रीका
- फ़ारस की खाड़ी
- भारत
- दक्षिण पूर्व एशिया
- चीन
- ऑस्ट्रेलिया
- ये पक्षी आर्कटिक क्षेत्र में प्रजनन करते हैं।
- भारत में, इन्हें सर्दियों के दौरान विभिन्न राज्यों में पाया जा सकता है, जिनमें शामिल हैं:
- Gujarat
- महाराष्ट्र
- Karnataka
- गोवा
- केरल
- तमिलनाडु
- आंध्र प्रदेश
- ओडिशा
- पश्चिम बंगाल
- त्रिपुरा
- अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह
असाधारण प्रवास
- बार-टेल्ड गॉडविट्स के नाम बिना रुके उड़ान भरने का विश्व रिकॉर्ड है।
- उनके बारे में यह प्रमाणित किया गया है कि उन्होंने अलास्का से तस्मानिया तक 13,500 किलोमीटर की प्रभावशाली दूरी मात्र 11 दिनों में तय की।
- इस यात्रा के दौरान, वे 50 किमी/घंटा से अधिक की औसत गति बनाए रखते हैं, और इस प्रक्रिया में अपने शरीर का लगभग आधा वजन खो देते हैं।
विशेषताएँ:
- बार-टेल्ड गॉडविट्स बड़े जलचर पक्षी हैं, जिनमें मादाएं नर से बड़ी होती हैं।
- इनके शरीर के ऊपरी भाग पर धब्बेदार भूरा रंग तथा निचले भाग पर हल्का, अधिक एकसमान पीला रंग होता है।
- इनके निचले पंख गहरे सफेद रंग के होते हैं।
- इनके पास एक लम्बी, थोड़ी ऊपर की ओर उठी हुई चोंच होती है।
- जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, उनकी पूंछ भूरे रंग की पट्टियों के साथ एक विशिष्ट सफेद रंग की होती है।
आईयूसीएन लाल सूची
- स्थिति : निकट संकटग्रस्त
|
3127 docs|1043 tests
|





















