UPSC Daily Current Affairs(Hindi): 27th November 2024 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly PDF Download
जीएस2/राजनीति
संभल मस्जिद विवाद: कानूनी विवाद और सांप्रदायिक तनाव
स्रोत: द हिंदू
चर्चा में क्यों?
उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए जिला अदालत के आदेश के बाद हिंसा भड़क उठी, जिसके परिणामस्वरूप कम से कम चार लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए।
About the Sambhal Mosque Dispute:
- पृष्ठभूमि:
- संभल जिला अदालत में एक याचिका दायर कर आरोप लगाया गया कि 16वीं शताब्दी की जामा मस्जिद का निर्माण एक प्राचीन मंदिर, हरि हर मंदिर के स्थल पर किया गया था।
- यह दावा वाराणसी, मथुरा और धार की अन्य मस्जिदों के बारे में किए गए दावों जैसा ही है।
- याचिकाकर्ताओं ने इस स्थल के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण का अनुरोध किया।
- शाही जामा मस्जिद प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के अंतर्गत संरक्षित स्थल है और इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- यह कानूनी स्थिति मामले को कानूनी और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील बनाती है।
- न्यायालय द्वारा आदेशित सर्वेक्षण और परिणामस्वरूप उत्पन्न अशांति:
- स्थानीय प्राधिकारियों और मस्जिद समिति के सदस्यों की भागीदारी से न्यायालय द्वारा आदेशित फोटोग्राफिक और वीडियोग्राफिक सर्वेक्षण प्रारंभ में सुचारू रूप से किया गया।
- हालांकि, बाद में हुए सर्वेक्षण के दौरान हिंसक झड़पें हुईं, जब एक याचिकाकर्ता नारे लगाते समर्थकों के साथ वहां पहुंचा, जिससे मस्जिद के पास विरोध प्रदर्शन भड़क उठे।
- पुलिस गोलीबारी के आरोप सामने आए, जिसके परिणामस्वरूप किशोरों सहित पांच व्यक्तियों की मौत हो गई, स्थानीय निवासियों ने पुलिस पर अत्यधिक बल प्रयोग और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया, हालांकि पुलिस ने इन दावों का खंडन किया है।
- स्थानीय लोगों का आरोप:
- इस बात पर चिंता व्यक्त की गई कि याचिका दायर होने के तुरंत बाद ही सर्वेक्षण आदेश जारी कर दिया गया, जिसमें हिंदू पक्ष को उच्च न्यायालय में अपना दावा पेश करने का मौका नहीं दिया गया।
- किसी भी औपचारिक चुनौती से पहले ही सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया, जिसमें आवश्यक प्रक्रियागत सुरक्षा की अनदेखी की गई।
जामा मस्जिद का ऐतिहासिक संदर्भ:
- निर्माण:
- जामा मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट बाबर (1526-1530) के शासनकाल के दौरान उसके सेनापति मीर हिंदू बेग द्वारा किया गया था और यह प्रारंभिक मुगल वास्तुकला का एक उल्लेखनीय उदाहरण है।
- यह बाबर के शासन के दौरान निर्मित तीन मस्जिदों में से एक है, अन्य दो मस्जिदें पानीपत की मस्जिद और अयोध्या की बाबरी मस्जिद हैं, जिन्हें 1992 में ध्वस्त कर दिया गया था।
- वास्तुकला विशेषताएँ:
- यह मस्जिद सम्भल के मध्य में एक पहाड़ी पर स्थित है और इसमें एक बड़ा वर्गाकार मेहराब कक्ष है जिसके शीर्ष पर मेहराबों द्वारा समर्थित एक गुंबद है।
- इसका निर्माण पत्थर की चिनाई और प्लास्टर का उपयोग करके किया गया था, जो बदायूं जैसी अन्य मस्जिदों से मिलता जुलता है।
- 17वीं शताब्दी में जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण मरम्मत कार्य किया गया।
- ऐतिहासिक बहस:
- कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह मस्जिद संभवतः तुगलक युग की है, जिसमें बाबर द्वारा कुछ संशोधन किए गए थे।
- स्थानीय परम्पराओं के अनुसार मस्जिद में विष्णु मंदिर के अवशेष हैं, जिसके बारे में माना जाता है कि यह स्थल भगवान विष्णु के दसवें अवतार कल्कि के आगमन से जुड़ा है।
जामा मस्जिद का कानूनी संदर्भ:
- उपासना स्थल अधिनियम, 1991:
- इस विवाद ने पूजा स्थल अधिनियम के बारे में चर्चा को फिर से छेड़ दिया है, जिसका उद्देश्य बाबरी मस्जिद मामले को छोड़कर सभी स्थलों के धार्मिक चरित्र को वैसा ही बनाए रखना है जैसा वे 15 अगस्त, 1947 को थे।
- मुख्य प्रावधान: अधिनियम की धारा 3 पूजा स्थलों को विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों के स्थलों में बदलने पर रोक लगाती है।
- इस अधिनियम का उद्देश्य धार्मिक स्थलों पर भविष्य में होने वाले विवादों को रोकना तथा भारत की धर्मनिरपेक्ष अखंडता को बनाए रखना है।
- अधिनियम की चुनौतियाँ:
- संभल में दायर याचिका में मस्जिद की धार्मिक स्थिति को चुनौती दी गई है, जो 1991 के अधिनियम की शर्तों के विरुद्ध है।
- याचिकाकर्ताओं ने न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की 2022 में की गई टिप्पणियों का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि किसी धार्मिक स्थल के चरित्र का निर्धारण करना अधिनियम का उल्लंघन नहीं हो सकता है।
- वर्तमान में, इस अधिनियम पर सवाल उठाने वाली चार याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं, साथ ही वाराणसी, मथुरा, धार और अब संभल में भी विवाद लंबित हैं।
संभल मस्जिद विवाद के व्यापक निहितार्थ:
- कानूनी मिसालें:
- बढ़ती चुनौतियों और कानूनी विवादों के बीच 1991 के अधिनियम की व्याख्या महत्वपूर्ण है।
- ऐतिहासिक जवाबदेही:
- पुरातात्विक अध्ययनों को सांप्रदायिक सद्भाव की अनिवार्यता के साथ संतुलित करने की अत्यंत आवश्यकता है।
- सांप्रदायिक शांति:
- हिंसा की रोकथाम सुनिश्चित करना तथा विविध समुदायों के बीच सह-अस्तित्व को बढ़ावा देना आवश्यक है।
निष्कर्ष:
- संभल मस्जिद विवाद भारत के विविध समाज में ऐतिहासिक आख्यानों, कानूनी ढांचे और सामाजिक सामंजस्य के बीच जटिल संबंधों को उजागर करता है।
जीएस2/राजनीति
भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में मदद करने वाली महिलाएं
स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस
चर्चा में क्यों?
संविधान दिवस (26 नवंबर) पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत की संविधान सभा में महिलाओं द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिकाओं पर जोर दिया।
- 299 सदस्यों वाली विधानसभा में 15 महिलाएं शामिल थीं (जिनमें से दो ने बाद में इस्तीफा दे दिया), जो विभिन्न क्षेत्रों और दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती थीं। सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी और विजया लक्ष्मी पंडित जैसी उल्लेखनीय हस्तियों के साथ कई कम चर्चित महिलाएं भी थीं जिन्होंने लिंग, जाति और आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लिया।
अम्मू स्वामीनाथन: संविधान सभा में महिलाओं की अग्रणी आवाज़
- अम्मू स्वामीनाथन का जन्म केरल के पलक्कड़ में हुआ था, और उन्होंने अपनी किशोरावस्था में ही सुब्बाराम स्वामीनाथन से विवाह कर लिया था, क्योंकि उन्हें दैनिक जीवन में स्वतंत्रता की आवश्यकता थी।
- उनके बच्चों में कैप्टन लक्ष्मी सहगल भी थीं, जो आजाद हिन्द फौज की एक प्रमुख हस्ती थीं।
- उनकी राजनीतिक भागीदारी उनकी मां द्वारा सामना की गई प्रतिबंधात्मक विधवा प्रथाओं का विरोध करने के उनके अनुभवों से प्रेरित थी।
- स्वामीनाथन ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और संविधान सभा की सदस्य के रूप में उन्होंने हिंदू कोड बिल और लैंगिक समानता का समर्थन किया, बावजूद इसके कि उन्हें मुख्य रूप से पुरुष प्रधान सभा से प्रतिरोध का सामना करना पड़ा।
- स्वतंत्रता के बाद, वह डिंडीगुल, तमिलनाडु से चुनी गईं और रूस, चीन और अमेरिका सहित विभिन्न देशों में भारत की सद्भावना राजदूत के रूप में कार्य किया।
एनी मास्कारेन: सार्वभौमिक मताधिकार और स्थानीय स्वायत्तता की समर्थक
- 1902 में त्रावणकोर में एक लैटिन ईसाई परिवार में जन्मी एनी मास्कारेन को सामाजिक बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने शैक्षणिक रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और कानून की पढ़ाई की, बाद में एक शिक्षिका बन गईं।
- वह त्रावणकोर में उथल-पुथल के दौरान राजनीतिक रूप से सक्रिय थीं, तथा स्थानीय राजघरानों द्वारा शुरू किए गए जाति और लिंग सुधारों से प्रभावित थीं।
- मस्कारेन अखिल त्रावणकोर संयुक्त राजनीतिक कांग्रेस और बाद में त्रावणकोर राज्य कांग्रेस में शामिल हो गए, तथा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की वकालत की तथा विरोधियों की हिंसा को सहन किया।
- संविधान सभा में उन्होंने एक मजबूत केन्द्रीय सरकार का समर्थन किया तथा स्थानीय सरकार की स्वायत्तता की भी वकालत की।
- गुटबाजी के कारण कांग्रेस छोड़ने के बाद, उन्होंने 1952 में तिरुवनंतपुरम से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में सफलतापूर्वक चुनाव लड़ा, जो भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी।
बेगम कुदसिया ऐजाज़ रसूल: राजनीति में एक अग्रणी महिला
- बेगम कुदसिया ऐजाज़ रसूल का जन्म पंजाब के एक शाही परिवार में हुआ था और उन्होंने विरोध का सामना करने के बावजूद औपचारिक शिक्षा प्राप्त की, जिसमें कॉन्वेंट शिक्षा के खिलाफ फतवा भी शामिल था।
- नवाब ऐजाज़ रसूल से शादी करने के बाद, उन्होंने पर्दा प्रथा को तोड़ दिया और राजनीति में प्रवेश किया, तथा रूढ़िवादी विरोध के बावजूद 1936 में गैर-आरक्षित सीट से जीत हासिल की।
- मुस्लिम लीग की सदस्य के रूप में उन्होंने महिला अधिकारों के लिए अभियान चलाया और धार्मिक रूप से पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का विरोध किया।
- प्रारंभ में, उन्हें पाकिस्तान के विचार में संभावित लाभ दिखाई दिए, लेकिन अंततः विभाजन के बाद गरीब मुसलमानों के कल्याण के लिए चिंतित होकर उन्होंने भारत में ही रहने का निर्णय लिया।
- बाद में वह कांग्रेस में शामिल हो गईं और 1952 में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में रहीं, उन्होंने भारत में महिला हॉकी को बढ़ावा देने में भी योगदान दिया।
दाक्षायनी वेलायुधन: दलित अधिकारों और समानता के लिए एक अग्रदूत
- दक्षायनी वेलायुधन कोचीन में विज्ञान में स्नातक करने वाली पहली दलित महिला थीं और उन्होंने कोचीन विधान परिषद में सेवा की थी।
- पुलाया समुदाय से होने के कारण, जिसे "दास" माना जाता था, उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा, जिसमें कॉलेज में व्यावहारिक प्रयोगों से बहिष्कार भी शामिल था।
- अंततः उन्होंने एक सामाजिक कार्यकर्ता से एक सादे समारोह में विवाह कर लिया, जिसका आयोजन एक कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति ने किया था, तथा इस समारोह में महात्मा गांधी और कस्तूरबा भी उपस्थित थे।
- 1946 में संविधान सभा के सदस्य के रूप में उन्होंने अंबेडकर के पृथक निर्वाचिका मंडल के आह्वान का विरोध किया और तर्क दिया कि इससे विभाजन को बढ़ावा मिलेगा और राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न होगी।
- यद्यपि वित्तीय कठिनाइयों ने उनके राजनीतिक जीवन को सीमित कर दिया, फिर भी वे दलित आंदोलन में सक्रिय रहीं और 1971 में राजनीति में लौट आईं, हालांकि वे स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनावों में चौथे स्थान पर रहीं।
रेणुका रे: महिला अधिकारों की अग्रदूत
- रेणुका रे का जन्म पबना (अब बांग्लादेश में) के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था और 1920 में महात्मा गांधी से प्रेरित होकर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गईं।
- उन्होंने जमीनी स्तर पर प्रयासों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाई और साबरमती आश्रम में कुछ समय बिताया, बाद में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अध्ययन किया, जहां उनकी मुलाकात उनके भावी पति सत्येंद्र नाथ रे से हुई।
- भारत लौटने पर वह महिला अधिकारों की प्रबल समर्थक बन गईं, विशेष रूप से तलाक और उत्तराधिकार कानूनों पर उनका ध्यान केन्द्रित था।
- रे ने 1943 में केन्द्रीय विधान सभा में महिला संगठनों का प्रतिनिधित्व किया और 1946 में संविधान सभा में शामिल हुईं।
- उन्होंने हिंदू कोड बिल का समर्थन किया और विधायिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का विरोध किया, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसे उपाय महिलाओं की प्रगति में बाधा हैं।
- यद्यपि वे 1952 में हुगली से आम चुनाव हार गयीं, परन्तु 1957 में उन्होंने जीत हासिल की और सामाजिक कार्यों में लौटने से पहले बंगाल में शासन में योगदान दिया, जो महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय के प्रति उनकी आजीवन प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
जीएस3/पर्यावरण
गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी
स्रोत : द वीक

चर्चा में क्यों?
सकल राष्ट्रीय खुशी की अवधारणा को शुरू करने के लिए जाना जाने वाला भूटान एक "माइंडफुलनेस सिटी" स्थापित करने की महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम कर रहा है। "गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी" (जीएमसी) वर्तमान में इस अभिनव शहरी विकास को शुरू करने के लिए धन जुटाने के चरण में है।
गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी (जीएमसी) का अवलोकन
- जीएमसी भूटान में एक अग्रणी शहरी विकास अवधारणा है, जिसकी परिकल्पना महामहिम राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने की थी।
- स्थान: गेलेफू में स्थित है, जो भूटान के दक्षिण-मध्य क्षेत्र में है।
- क्षेत्रफल: यह परियोजना 2,500 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, जो इसे भूटान की सबसे महत्वपूर्ण शहरी विकास पहलों में से एक बनाती है।
- विशेष प्रशासनिक क्षेत्र (एसएआर): जीएमसी भूटान का प्रथम एसएआर होगा, जिसे कार्यकारी स्वायत्तता और कानूनी स्वतंत्रता प्राप्त होगी।
जीएमसी की मुख्य विशेषताएं
- जागरूकता और स्थिरता: शहर को आर्थिक विकास को जागरूकता, समग्र जीवन और स्थिरता के सिद्धांतों के साथ मिलाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- आर्थिक केंद्र: दक्षिण एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया और चीन के बीच रणनीतिक रूप से स्थित, जीएमसी क्षेत्रीय संपर्क और आर्थिक आदान-प्रदान का एक प्रमुख केंद्र बनने के लिए तैयार है।
- शून्य कार्बन शहर: इसका लक्ष्य "शून्य कार्बन" शहर बनना है, जो सतत विकास प्रथाओं के प्रति भूटान के समर्पण को दर्शाता है।
- बुनियादी ढांचा: शहर में उन्नत बुनियादी ढांचा होगा, जिसमें रहने योग्य पुल, एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं शामिल होंगी, जो पश्चिमी और पारंपरिक चिकित्सा दोनों को एकीकृत करती हैं।
- संरक्षित क्षेत्र: डिजाइन में एक राष्ट्रीय उद्यान और एक वन्यजीव अभयारण्य शामिल है, जो जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देता है।
जीएमसी का विजन और मूल्य
- सकल राष्ट्रीय खुशी (जीएनएच): यह विकास जीएनएच के सिद्धांतों पर आधारित है, जो सचेत और टिकाऊ व्यावसायिक प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करने को प्रोत्साहित करता है।
- बौद्ध विरासत: भूटान की समृद्ध आध्यात्मिक परंपराओं से प्रेरित होकर, जीएमसी का लक्ष्य सचेतन जीवन जीने के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देना है।
- व्यावसायिक वातावरण: उद्यमों का मूल्यांकन और स्वागत भूटानी सांस्कृतिक मूल्यों के पालन, सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता और राष्ट्रीय संप्रभुता के प्रति सम्मान के आधार पर किया जाएगा।
जीएस2/शासन
भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई)
स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया
चर्चा में क्यों?
भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपनी अर्धवार्षिक शिकायत रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें विशेष रूप से रियल एस्टेट और अपतटीय सट्टेबाजी क्षेत्रों में भ्रामक और अवैध विज्ञापनों की महत्वपूर्ण घटनाओं पर प्रकाश डाला गया है।
भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) के बारे में:
- एएससीआई भारत में विज्ञापन उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाला एक स्वैच्छिक स्व-नियामक संगठन है।
- 1985 में स्थापित, यह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 25 के तहत एक गैर-लाभकारी संस्था के रूप में पंजीकृत है।
- यह संगठन उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए विज्ञापन में स्व-नियमन को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है।
- एएससीआई यह सुनिश्चित करता है कि विज्ञापन उसके स्व-नियमन संहिता के अनुरूप हों, जिसके अनुसार विज्ञापन कानूनी, सभ्य, ईमानदार, सत्यनिष्ठ और हानिकारक न हों, साथ ही प्रतिस्पर्धा में निष्पक्षता को बढ़ावा दें।
- यह प्रिंट, टेलीविजन, रेडियो, होर्डिंग्स, एसएमएस, ईमेल, वेबसाइट, उत्पाद पैकेजिंग, ब्रोशर, प्रचार सामग्री और बिक्री केन्द्रों सहित विभिन्न मीडिया में विज्ञापनों से संबंधित शिकायतों का समाधान करता है।
संरचना:
- संगठन का संचालन एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा किया जाता है, जिसमें प्रतिष्ठित व्यवसायों, मीडिया एजेंसियों और विज्ञापन क्षेत्रों से 16 सदस्य शामिल होते हैं।
- उपभोक्ता शिकायत परिषद (सीसीसी) शिकायतों की जांच करने तथा यह निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है कि विज्ञापन एएससीआई के मानकों के अनुरूप हैं या नहीं।
- महासचिव के नेतृत्व में एक सचिवालय एएससीआई के दिन-प्रतिदिन के कार्यों का प्रबंधन करता है।
- यद्यपि ASCI एक सरकारी निकाय नहीं है, फिर भी इसके प्रभाव को मान्यता प्राप्त है; उदाहरण के लिए, 2006 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने यह अनिवार्य कर दिया था कि भारत में सभी टेलीविजन विज्ञापन ASCI के नियमों का पालन करें।
- एएससीआई अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन स्व-विनियमन परिषद (आईसीएएस) की कार्यकारी समिति का भी हिस्सा है।
जीएस2/राजनीति
भारत का संघीय दृष्टिकोण
स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?
26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया भारतीय संविधान, संविधान में परिभाषित संघीय ढांचे पर विचार करने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह संरचना एकता और विविधता, विकेंद्रीकरण और लोकतांत्रिक शासन को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
पृष्ठभूमि :
- भारतीय संघवाद एक संवैधानिक विकल्प है जो एकता और विविधता के बीच संतुलन को दर्शाता है, तथा विकेंद्रीकरण और लोकतांत्रिक निर्णय लेने को बढ़ावा देता है।
भारत के संघवाद की अनूठी विशेषताएं
- भारत को 'अर्ध-संघीय' गणराज्य कहा जाता है, जिसमें संघीय और एकात्मक दोनों विशेषताएं समाहित हैं।
- संघीय ढांचा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है, तथा लचीले शासन के लिए एकात्मक विशेषताओं को शामिल करता है।
संविधान द्वारा स्थापित प्रमुख संघीय विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
- दोहरी राजनीति: शासन प्रणाली में एक केन्द्रीय संघ सरकार और राज्य सरकारें शामिल होती हैं।
- संवैधानिक सर्वोच्चता: सभी अधिनियमित कानून संविधान के अनुरूप होने चाहिए।
- कठोर संशोधन प्रक्रियाएं: संविधान कठोर संशोधन प्रक्रियाओं के माध्यम से अपने संघीय ढांचे की सुरक्षा करता है।
- शक्तियों का विभाजन: संविधान की सातवीं अनुसूची केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों को तीन सूचियों में विभाजित करती है:
तीन सूचियाँ
- संघ सूची: संघीय संसद के लिए अनन्य विषय, जिनमें रक्षा और विदेशी मामले शामिल हैं।
- राज्य सूची: राज्य विधानमंडल के अधीन विषय, जैसे पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य और कृषि।
- समवर्ती सूची: ऐसे विषय जिन पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, तथा विवाद की स्थिति में संघ के कानून लागू होंगे। उदाहरण के लिए शिक्षा और विवाह।
यह ढांचा किसी भी सरकारी स्तर पर सत्ता के संकेन्द्रण को रोकता है।
तीन सूचियों में किये गए परिवर्तन
- समय के साथ, बदलती शासन आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए तीनों सूचियों में समायोजन किए गए हैं।
- संविधान में शुरू में संघ सूची में 98 विषय, राज्य सूची में 66 विषय और समवर्ती सूची में 47 विषय शामिल थे। वर्तमान में, ये संख्या क्रमशः 100, 59 और 52 हो गई है, जो पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण बदलावों को दर्शाता है।
- 1976 का 42वां संशोधन अधिनियम विशेष रूप से प्रभावशाली था, जिसने शिक्षा और वन जैसे प्रमुख विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया।
समवर्ती सूची में स्थानांतरित किये गये विषयों के उदाहरण
- शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल करने का उद्देश्य देश भर में शैक्षिक गुणवत्ता को मानकीकृत करना था, जिससे केंद्र सरकार को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 जैसी राष्ट्रीय नीतियों को लागू करने में मदद मिले।
- पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए वनों को समवर्ती सूची में भी डाल दिया गया, जिससे केंद्र सरकार को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 जैसे कानून बनाने की अनुमति मिल गई।
समकालीन चुनौतियाँ
- सातवीं अनुसूची में व्यक्त शक्तियों का विभाजन शासन की आवश्यकताओं के अनुरूप केन्द्रीयकरण और क्षेत्रीय स्वायत्तता के बीच संतुलन स्थापित करने में अनुकूलनशीलता को प्रदर्शित करता है।
- जलवायु परिवर्तन और साइबर अपराध जैसी नई चुनौतियाँ क्षेत्रीय सीमाओं को पार कर रही हैं, जिसके लिए राज्य और केंद्र सरकारों के बीच सहयोगात्मक प्रयास आवश्यक हो गए हैं।
जीएस3/पर्यावरण
चक्रवात फेंगल
स्रोत: इकोनॉमिक टाइम्स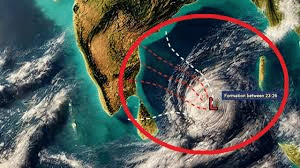
चर्चा में क्यों?
बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम में बना मौसमी दबाव एक गहरे दबाव में तब्दील हो गया है, जिसके आगे चलकर चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की आशंका है। यह तीव्रता समुद्र की सतह के ऊंचे तापमान (एसएसटी) वाले क्षेत्रों की मौजूदा निकटता से समर्थित है।
'फेंगल' नाम की उत्पत्ति
- 'फेंगल' नाम सऊदी अरब द्वारा सुझाया गया था और इसकी जड़ें अरबी भाषा में हैं।
- यह नाम भाषाई विरासत और सांस्कृतिक पहचान का मिश्रण दर्शाता है।
चक्रवात नामकरण प्रक्रिया:
- उत्तरी हिंद महासागर में चक्रवातों का नामकरण विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) और एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (UNESCAP) द्वारा किया जाता है।
- इस नामकरण पैनल में बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान सहित 13 सदस्य देश शामिल हैं।
- प्रत्येक भागीदार देश संभावित चक्रवातों के नामों की एक सूची प्रस्तुत करता है, जिनका उपयोग क्षेत्र में तूफान आने पर क्रमिक रूप से किया जाता है।
- यह व्यवस्थित दृष्टिकोण 2004 से लागू है, जिससे जनता को तूफानों की स्पष्ट पहचान और उनके बारे में प्रभावी संचार की सुविधा मिलती है।
चक्रवात क्या हैं?
- चक्रवातों को वायु प्रणालियों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर अंदर की ओर घूमती हैं।
श्रेणियाँ:
- उष्णकटिबंधीय चक्रवात (तापमान भिन्नताओं के कारण) और शीतोष्ण चक्रवात (अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय वायु द्रव्यमान प्रभावों से निर्मित)।
भौगोलिक कारण
- उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बनने के लिए विशिष्ट पर्यावरणीय परिस्थितियों की आवश्यकता होती है:
- समुद्र की सतह का तापमान 27°C से अधिक होना।
- घूर्णन में सहायता के लिए कोरिओलिस बल।
- चक्रवात निर्माण को आरंभ करने के लिए पहले से मौजूद निम्न दबाव प्रणालियाँ।
- न्यूनतम ऊर्ध्वाधर पवन गति अंतर.
- तूफान के विकास को बढ़ावा देने के लिए ऊपरी वायु विचलन।
विशेषताएँ
- चक्रवात गर्म जल निकायों के ऊपर उत्पन्न होते हैं, तथा क्यूम्यलोनिम्बस बादलों में गर्म पानी के संघनन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं।
- कोरिओलिस बल वायु के घूर्णन को प्रभावित करता है, जिसके परिणामस्वरूप:
- उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त घूर्णन।
- दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त घूर्णन।
- चक्रवाती गतिविधि आमतौर पर 30° अक्षांश के आसपास समाप्त हो जाती है, जहां चक्रवात के पोषण के लिए आवश्यक गर्मी कम हो जाती है।
जीएस3/अर्थव्यवस्था
राष्ट्रीय दुग्ध दिवस
स्रोत : इंडिया टुडे

चर्चा में क्यों?
राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को डॉ. वर्गीस कुरियन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्हें 'भारत का दूधवाला' कहा जाता है। उन्होंने भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
के बारे में
- भारत के डेयरी क्षेत्र और श्वेत क्रांति में डॉ. वर्गीस कुरियन के महत्वपूर्ण योगदान के सम्मान में 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है।
- यह दिन भारत के विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बनने की यात्रा का प्रतीक है।
वर्गीस कुरियन द्वारा दिया गया योगदान
- डॉ. ए.एस. कुरियन का जन्म 26 नवंबर, 1921 को केरल के कोझिकोड में हुआ था।
- उन्होंने 1949 में अमूल की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त डेयरी ब्रांड में बदल दिया।
- उन्होंने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के प्रथम अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।
- डॉ. कुरियन ने ऑपरेशन फ्लड का नेतृत्व किया, जो एक अभूतपूर्व पहल थी जिसने भारत के डेयरी उद्योग में क्रांति ला दी और दूध उत्पादन में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित की।
- उन्हें अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें 1963 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी शामिल है।
भारत में श्वेत क्रांति और दूध उत्पादन के बारे में
- श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 में ऑपरेशन फ्लड के साथ हुई, जिसका उद्देश्य दूध उत्पादन को बढ़ावा देना और दूध पाउडर के आयात पर निर्भरता कम करना था।
- इस पहल ने दूध उत्पादन के लिए सहकारी मॉडल को बढ़ावा देकर डेयरी किसानों को सशक्त बनाया।
- 1990 के दशक के अंत तक भारत संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बन गया।
- दूध उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो 1968-69 में 21.2 मिलियन टन से बढ़कर 1991-92 में 55 मिलियन टन से अधिक हो गया।
- इस पहल से दूध आपूर्ति श्रृंखला, प्रसंस्करण संयंत्र और भंडारण सुविधाओं सहित आवश्यक बुनियादी ढांचे की स्थापना में भी मदद मिली, जिससे जनता के लिए दूध अधिक सुलभ हो गया।
- इससे ग्रामीण किसानों की आय और आजीविका में उल्लेखनीय वृद्धि हुई तथा रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में योगदान मिला।
- वर्ष 2022-23 तक, भारत दूध उत्पादन में विश्व स्तर पर पहले स्थान पर है, जो विश्व के कुल उत्पादन में 24% का योगदान देता है, तथा इसका उत्पादन 230.58 मिलियन टन है।
जीएस2/राजनीति
भारत का संविधान दिवस
स्रोत: एनडीटीवी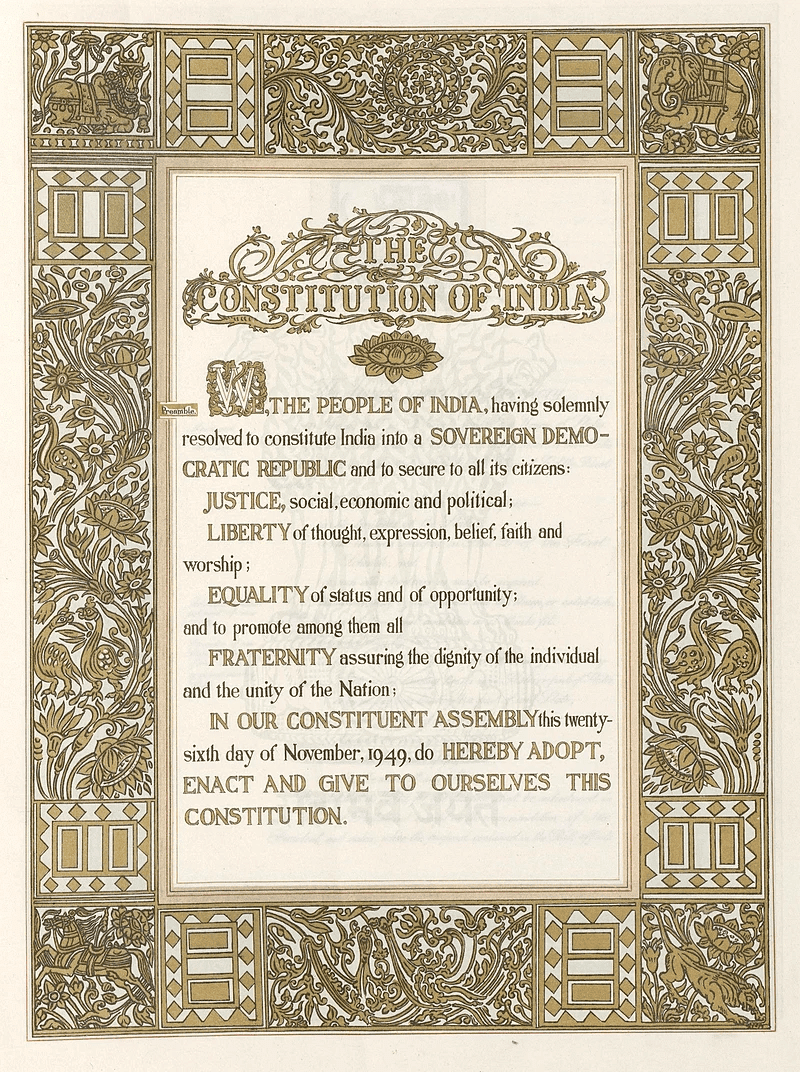
चर्चा में क्यों?
संविधान दिवस, जिसे संविधान दिवस के रूप में भी जाना जाता है, हर साल 26 नवंबर को 1949 में संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अपनाने की याद में मनाया जाता है। यह वर्ष 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है, जो भारत की संवैधानिक यात्रा और इसके मूल सिद्धांतों को दर्शाने वाला एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
- भारत का संविधान 26 नवंबर, 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ, जिसने भारत को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित किया। संविधान के मुख्य निर्माता डॉ. बीआर अंबेडकर ने भारत की स्वतंत्रता और संविधान में निहित मूल्यों को बनाए रखने की क्षमता के बारे में आशा और चिंता दोनों व्यक्त की।
- 2015 में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की घोषणा के बाद भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया। इस दिन का उद्देश्य नागरिकों को संविधान और न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के इसके मूलभूत मूल्यों के बारे में शिक्षित करना है। डॉ. अंबेडकर ने प्रसिद्ध रूप से कहा था कि यदि नए संविधान के तहत कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो यह किसी त्रुटिपूर्ण दस्तावेज़ के कारण नहीं बल्कि मानवता की विफलताओं के कारण होगा।
- 26 नवंबर, 2024 को भारत संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर, मंत्री, सांसद और अन्य गणमान्य व्यक्ति संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस समारोह के लिए एकत्र हुए।
प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के मुख्य अंश:
- श्रद्धांजलि और महत्व: प्रधानमंत्री मोदी ने 75वां संविधान दिवस मनाया, संविधान सभा के सदस्यों और 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के पीड़ितों को सम्मानित किया और आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
- संविधान की अनुकूलनशीलता: उन्होंने संविधान को एक "जीवित, विकासशील मार्गदर्शिका" बताया जो भारत की चुनौतियों के अनुरूप ढलती है, तथा जम्मू एवं कश्मीर में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद इसकी प्रासंगिकता का उल्लेख किया।
- विकसित भारत का विजन: उन्होंने सामाजिक-आर्थिक न्याय पर जोर दिया तथा कल्याणकारी कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला, जिनके तहत 53 करोड़ बैंक खाते, 4 करोड़ पक्के मकान, 10 करोड़ गैस कनेक्शन तथा 12 करोड़ नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं।
- बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी: उपलब्धियों में 2.5 करोड़ घरों तक बिजली पहुंचाना और दूरदराज के क्षेत्रों में 4जी/5जी सेवाओं के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाना, अंडमान और निकोबार में पानी के नीचे ब्रॉडबैंड और पीएम स्वामित्व योजना के तहत भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण शामिल है।
- आधुनिक अवसंरचना विकास: प्रगति मंच के माध्यम से त्वरित ₹18 लाख करोड़ की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा का उद्देश्य समय पर पूरा करना और राष्ट्रीय प्रगति करना है।
- राष्ट्रीय एकता: उन्होंने अखंडता और राष्ट्रीय हित का आह्वान करते हुए अपने भाषण का समापन किया तथा भावी पीढ़ियों के लिए संविधान को कायम रखने के लिए "राष्ट्र प्रथम" की भावना पर बल दिया।
भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के भाषण के मुख्य अंश:
- न्यायपालिका की रक्षा: मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति बाहरी प्रभावों से मुक्त होकर निष्पक्ष निर्णय सुनिश्चित करने के लिए की जाती है, उन्होंने न्यायाधीशों द्वारा वोट के लिए प्रचार करने के खतरों के प्रति चेतावनी दी।
- न्यायिक स्वतंत्रता: उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि न्यायिक स्वतंत्रता सरकारी शाखाओं के बीच समन्वय के लिए एक सेतु का काम करती है, जबकि उनकी पृथकता भी बनी रहती है, तथा न्यायाधीश केवल संविधान और कानून द्वारा निर्देशित होते हैं।
- आलोचना को संतुलित करना: न्यायाधीशों को अपने निर्णयों के प्रति मिश्रित प्रतिक्रियाएं प्राप्त होती हैं तथा वे कार्यकुशलता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए रचनात्मक फीडबैक से लाभान्वित होते हैं।
- पारदर्शिता और जवाबदेही: न्यायपालिका अकुशलताओं की पहचान करने और अपनी प्रणालियों में सुधार करने के लिए खुलेपन को महत्व देती है, तथा जन-केंद्रित और पारदर्शी होने के महत्व पर बल देती है।
- वैश्विक स्थिति: भारत के संवैधानिक न्यायालयों को विश्व स्तर पर शक्तिशाली माना जाता है, लेकिन उनके अधिदेश और यथास्थिति के पालन के संबंध में अलग-अलग राय हैं।
- लंबित मामलों की संख्या: मुख्य न्यायाधीश ने लंबित मामलों की संख्या पर प्रकाश डाला तथा निपटान दरों में प्रगति की बात कही: वर्ष 2024 तक जिला न्यायालयों के लिए यह दर 101.74% तथा सर्वोच्च न्यायालय के लिए 97% होगी।
- न्यायपालिका की भूमिका: न्यायाधीश जनता की सेवा करने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और आलोचनाओं का प्रभावी ढंग से समाधान करने को प्राथमिकता देते हैं।
जीएस3/पर्यावरण
वैश्विक मैचमेकिंग प्लेटफॉर्म
स्रोत: डीटीई

चर्चा में क्यों?
हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूएनआईडीओ) और क्लाइमेट क्लब ने ग्लोबल मैचमेकिंग प्लेटफॉर्म (जीएमपी) लॉन्च किया।
ग्लोबल मैचमेकिंग प्लेटफॉर्म के बारे में:
- जीएमपी का उद्देश्य उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में उच्च उत्सर्जन उत्पन्न करने वाले उद्योगों की डीकार्बोनाइजेशन प्रक्रिया में तेजी लाना है।
- इस पहल की परिकल्पना दिसंबर 2023 में 28वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP28) के दौरान की गई थी, जो जलवायु क्लब के शुभारंभ के साथ ही हुई थी।
- यह तकनीकी विशेषज्ञता और वित्तीय सहायता सहित देशों की विशिष्ट आवश्यकताओं और वैश्विक संसाधनों के बीच संबंधों को सुगम बनाता है, जिसका उद्देश्य उन क्षेत्रों में उत्सर्जन को कम करना है जो महत्वपूर्ण ऊर्जा की खपत करते हैं और उत्सर्जन उत्पन्न करते हैं।
- यह मंच देशों को साझेदारों के विविध नेटवर्क से जोड़ता है जो औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन प्रयासों को समर्थन देने के लिए व्यापक तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं।
- ये डिलीवरी पार्टनर कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे:
- प्रभावी उत्सर्जन न्यूनीकरण रणनीतियों की दिशा में देशों का मार्गदर्शन करने के लिए नीति विकास।
- नवीन प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण जो उत्सर्जन को कम करने में सहायक हो सकती हैं।
- कम उत्सर्जन वाली औद्योगिक प्रथाओं में परिवर्तन के लिए आवश्यक निवेश को सुविधाजनक बनाना।
- राष्ट्रीय उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्यों को बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान करना।
- यह तंत्र देशों को अपने डीकार्बोनाइजेशन दृष्टिकोण को अनुकूलित करने में सक्षम बनाता है, साथ ही साझेदार संगठनों से संसाधनों और मार्गदर्शन तक पहुंच को सरल बनाता है, जिससे उत्सर्जन में महत्वपूर्ण कमी आती है।
- जीएमपी को जलवायु क्लब के तहत एक सहायक ढांचे के रूप में स्थापित किया जा रहा है, जिसका सचिवालय यूएनआईडीओ द्वारा प्रबंधित किया जाएगा।
- इसके अलावा, इसके संचालन को क्लाइमेट क्लब अंतरिम सचिवालय द्वारा समर्थन प्राप्त है, जिसका सह-संचालन आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) द्वारा किया जाता है।
जीएस2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध
डिजाइन कानून संधि
स्रोत: आउटलुक इंडिया
चर्चा में क्यों?
लगभग दो दशकों की बातचीत के बाद, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) के सदस्य देशों ने ऐतिहासिक डिजाइन कानून संधि (डीएलटी) को अपनाया।
डिज़ाइन कानून संधि के बारे में:
- डीएलटी का उद्देश्य औद्योगिक डिजाइन संरक्षण से संबंधित प्रक्रियाओं को मानकीकृत करना है, ताकि विभिन्न देशों में पंजीकरण प्रक्रिया अधिक कुशल और सुलभ हो सके।
- इस संधि को प्रभावी बनाने के लिए 15 संविदाकारी पक्षों के अनुसमर्थन की आवश्यकता है।
प्रमुख विशेषताऐं
- किसी डिज़ाइन के प्रथम बार खुलासा होने के बाद 12 महीने की छूट अवधि दी जाती है, जिसका अर्थ है कि इस प्रारंभिक खुलासे से पंजीकरण के लिए डिज़ाइन की वैधता कम नहीं होगी।
- आवेदकों को ऐसे राहत उपाय प्राप्त होते हैं जो लचीलापन प्रदान करते हैं, तथा समय-सीमा चूक जाने के कारण उनके अधिकारों की हानि को रोकते हैं।
- यह संधि डिजाइन पंजीकरण के नवीनीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाती है।
- यह डिजाइन पंजीकरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग प्रणाली और प्राथमिकता दस्तावेजों के डिजिटल आदान-प्रदान को अपनाने को प्रोत्साहित करता है।
- संधि को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद के लिए विकासशील और अल्पविकसित देशों को तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी।
फ़ायदे
- डीएलटी का उद्देश्य सुव्यवस्थित डिजाइन सुरक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाना है, तथा इसका मुख्य उद्देश्य लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई), स्टार्टअप्स और स्वतंत्र डिजाइनरों को समर्थन प्रदान करना है।
- डिजाइन पंजीकरण के लिए आवश्यकताओं को मानकीकृत करके, डीएलटी प्रशासनिक बोझ को कम करता है, तथा डिजाइन में वैश्विक नवाचार को बढ़ावा देता है।
- स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम और स्टार्टअप बौद्धिक संपदा संरक्षण (एसआईपीपी) योजना जैसी पहलों के संयोजन में, ये उपाय स्टार्टअप्स और एसएमई को सशक्त बनाने के लिए तैयार किए गए हैं, जिससे उन्हें वैश्विक स्तर पर डिजाइन अधिकार हासिल करने में मदद मिलेगी, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी और बाजार विस्तार को बढ़ावा मिलेगा।
- भारत ने हाल ही में इस संधि के अंतिम अधिनियम पर हस्ताक्षर किये हैं।
|
3127 docs|1043 tests
|
FAQs on UPSC Daily Current Affairs(Hindi): 27th November 2024 - Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly
| 1. संभल मस्जिद विवाद क्या है और इसके पीछे का इतिहास क्या है ? |  |
| 2. भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में महिलाओं की भूमिका क्या थी ? |  |
| 3. गैलेफू माइंडफुलनेस सिटी की विशेषताएँ क्या हैं ? |  |
| 4. भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) का क्या कार्य है ? |  |
| 5. चक्रवात फेंगल के प्रभाव क्या थे ? |  |
















