UPSC Daily Current Affairs(Hindi): 26th November 2024 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly PDF Download
जीएस3/पर्यावरण
पुनर्योजी कृषि
स्रोत: द हिंदू बिजनेस लाइन
चर्चा में क्यों?
ओडिशा सरकार ने आईसीआरआईएसएटी के सहयोग से पुनर्योजी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'पुनर्योजी कृषि का संग्रह' प्रस्तुत किया है।
यह संग्रह टिकाऊ खेती सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए पांच मौलिक सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है:
- मृदा व्यवधान को न्यूनतम करना
- फसल विविधता को अधिकतम करना
- वर्ष भर मृदा आवरण बनाए रखना
- पूरे वर्ष मिट्टी में जीवित जड़ें बनाए रखना
- कृषि प्रणालियों में पशुधन को एकीकृत करना
पुनर्योजी कृषि, खेती के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है जो पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य की बहाली और वृद्धि पर जोर देती है।
मूल सिद्धांत:
- मृदा स्वास्थ्य: मुख्य रूप से बिना जुताई वाली खेती, कवर क्रॉपिंग और फसल चक्र जैसी विधियों के माध्यम से मृदा स्वास्थ्य को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जो मृदा संरचना और उर्वरता को संरक्षित करने में मदद करते हैं।
- जैव विविधता: विभिन्न प्रकार की फसलों और पशुधन को शामिल करके जैव विविधता को प्रोत्साहित करना। यह विविधता प्राकृतिक कीट नियंत्रण और प्रभावी पोषक चक्रण में सहायता करती है।
- जल प्रबंधन: जल प्रतिधारण में सुधार लाने और अपवाह को न्यूनतम करने के लिए रणनीतियों का क्रियान्वयन, जैसे मल्चिंग और कृषि वानिकी तकनीकें।
- कार्बन पृथक्करण: मिट्टी की कार्बन को अवशोषित करने की क्षमता को बढ़ाना, जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके जलवायु परिवर्तन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
अभ्यास:
- कवर फसल: मिट्टी को संरक्षित और समृद्ध करने के लिए ऑफ-सीजन के दौरान कवर फसलें लगाने की प्रथा, जिससे मुख्य फसलों की खेती न होने पर इसकी गुणवत्ता में सुधार होता है।
- कम्पोस्ट बनाना: कम्पोस्ट बनाने के माध्यम से मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ मिलाना, जिससे मिट्टी की संरचना और उर्वरता बढ़ती है, तथा पौधों की स्वस्थ वृद्धि को बढ़ावा मिलता है।
- कृषि वानिकी: जैव विविधता को बढ़ावा देने और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को बढ़ाते हुए वैकल्पिक आय स्रोत प्रदान करने के लिए कृषि प्रणालियों के भीतर पेड़ों और झाड़ियों का एकीकरण।
- समग्र प्रबंधन: टिकाऊ परिणामों के लिए मिट्टी, पौधों, जानवरों और मनुष्यों के बीच संबंधों को ध्यान में रखते हुए खेतों को परस्पर जुड़े पारिस्थितिक तंत्र के रूप में प्रबंधित करना।
फ़ायदे:
- मृदा स्वास्थ्य में सुधार: स्वस्थ मृदा से फसल की पैदावार बेहतर होती है, रासायनिक इनपुट की आवश्यकता कम होती है, तथा चरम मौसम की स्थिति के प्रति लचीलापन बढ़ता है।
- संवर्धित जैव विविधता: विविध पारिस्थितिकी तंत्र अधिक लचीलेपन और उत्पादकता में योगदान देते हैं, तथा लाभकारी कीटों और वन्य जीवन के लिए आवास का निर्माण करते हैं।
- जलवायु शमन: कार्बन को एकत्रित करके, पुनर्योजी कृषि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- आर्थिक व्यवहार्यता: किसान टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाकर इनपुट लागत में कटौती कर सकते हैं और लाभप्रदता बढ़ा सकते हैं।
जीएस3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी
मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरीमेंट (MACE) टेलीस्कोप
स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स
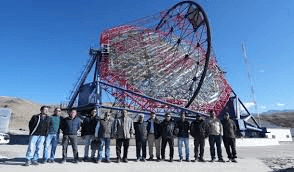
चर्चा में क्यों?
मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरीमेंट (MACE) दूरबीन का उद्घाटन 4 अक्टूबर को हानले, लद्दाख में किया गया।
मेस टेलीस्कोप के बारे में:
- यह दुनिया का सबसे ऊंचा इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप है, जो लद्दाख के हानले में समुद्र तल से 4.3 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है।
- इस दूरबीन में 21 मीटर चौड़ा दर्पण-डिश है, जो इसे एशिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा दूरबीन बनाता है।
- एमएसीई को भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बीएआरसी), टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान (टीआईएफआर), इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल) और भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (आईआईए) सहित संस्थानों के एक संघ द्वारा विकसित किया गया था।
- दूरबीन चेरेनकोव विकिरण को कैप्चर करके काम करती है, जो एक माध्यम में आवेशित कणों के प्रकाश की गति से अधिक होने पर उत्सर्जित होने वाली नीली रोशनी है। इस विकिरण को दर्पणों का उपयोग करके एकत्र किया जाता है और फोटोमल्टीप्लायर ट्यूब (पीएमटी) के साथ विश्लेषण किया जाता है।
- एमएसीई अपनी अवलोकन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक उच्च-रिज़ॉल्यूशन कैमरा और एक चल आधार से सुसज्जित है।
एमएसीई के लक्ष्य एवं उद्देश्य:
- एमएसीई को उच्च ऊर्जा वाली गामा किरणों का पता लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, विशेष रूप से 20 गीगा-इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक ऊर्जा वाली किरणों का, जो विभिन्न ब्रह्मांडीय घटनाओं द्वारा उत्पन्न होती हैं।
- इसका उद्देश्य डार्क मैटर अनुसंधान में सहायता के लिए कमजोर रूप से परस्पर क्रिया करने वाले विशाल कणों (डब्ल्यूआईएमपी) की पहचान करना है।
- यह दूरबीन बहु-संदेशवाहक खगोल विज्ञान में योगदान देगी तथा अन्य खगोलीय प्रेक्षणों के साथ-साथ पूरक डेटा भी उपलब्ध कराएगी।
डीएनए उत्परिवर्तन में गामा किरणें कैसे काम करती हैं?
- गामा किरणें आयनीकरण का कारण बनती हैं, जो डीएनए में रासायनिक बंधनों को तोड़ सकती हैं, जिससे आनुवंशिक उत्परिवर्तन हो सकता है।
- यदि इनकी मरम्मत नहीं की गई तो इन उत्परिवर्तनों के परिणामस्वरूप कैंसर या आनुवंशिक विकार हो सकते हैं।
- गामा किरणों से होने वाली क्षति गुणसूत्र संबंधी असामान्यताएं पैदा कर सकती है और कैंसर के विकास में योगदान दे सकती है।
जीएस2/राजनीति
सर्वसम्मति वाला गणतंत्र: संविधान सभा से आज के सांसदों के लिए एक सबक
स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस
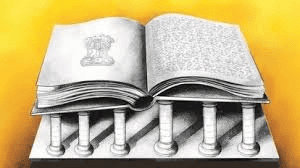
चर्चा में क्यों?
26 नवंबर, 2024 को भारत अपने संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा, जो एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है जिसने देश के लोकतांत्रिक शासन के लिए रूपरेखा तैयार की। इस महत्वपूर्ण दस्तावेज को तैयार करने वाली संविधान सभा के प्रयास वर्तमान राजनीतिक प्रथाओं को प्रेरित और निर्देशित करते रहते हैं। जैसे-जैसे यह महत्वपूर्ण तिथि निकट आ रही है, उस समय स्थापित किए गए मूलभूत आदर्शों पर विचार करना और संसद के वर्तमान और भविष्य के कामकाज के लिए सबक प्राप्त करना महत्वपूर्ण है।
संविधान सभा की भावना
संवाद और आम सहमति निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता
- संविधान सभा की पहचान संवाद और आम सहमति को बढ़ावा देने के प्रति समर्पण से थी।
- सदस्य विभिन्न वैचारिक, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय पृष्ठभूमि से आये थे, जिससे बहुलवादी और समावेशी वातावरण बनाने में मदद मिली।
- इस विविधता ने अव्यवस्था पैदा करने के बजाय संविधान की प्रारूपण प्रक्रिया को बढ़ाया।
- 25 नवम्बर 1949 को अपने समापन भाषण में बी.आर. अम्बेडकर ने कठोर दलीय नीतियों से बचने की सभा की क्षमता को स्वीकार किया।
- उन्होंने असहमतिपूर्ण विचारों के महत्व पर जोर दिया तथा माना कि इससे बहस समृद्ध होती है तथा संवैधानिक सिद्धांत स्पष्ट होते हैं।
वर्तमान संसदीय संस्कृति से एकदम विपरीत
- यह सम्मानजनक जुड़ाव आज के संसदीय माहौल से बिल्कुल विपरीत है, जो अक्सर ध्रुवीकरण और व्यवधान से ग्रस्त रहता है।
- असहमति को परिष्कार के लिए एक मूल्यवान उपकरण के रूप में अम्बेडकर का दृष्टिकोण आधुनिक विधायकों के लिए वैचारिक मतभेदों को शासन में बाधा के बजाय विकास के अवसर के रूप में देखने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।
पिछले कुछ दशकों में भारतीय संसदीय लोकतंत्र का विकास
संसदीय लोकतंत्र: एक लुप्त होती विरासत
- भारत का संसदीय लोकतंत्र, जिसे कभी शासन का मूलभूत पहलू माना जाता था, हाल के दशकों में इसकी कार्यक्षमता और प्रासंगिकता में उल्लेखनीय गिरावट आई है।
- संविधान सभा के मूल आदर्श, जैसे सशक्त बहस और सामूहिक कल्याण को प्राथमिकता देना, पक्षपात और प्रक्रियागत अकुशलता के कारण लुप्त हो गए हैं।
- यह गिरावट विभिन्न पहलुओं में स्पष्ट है, जिसमें बैठकों की आवृत्ति, बहस की गुणवत्ता और निर्णय लेने की पारदर्शिता शामिल है।
संसदीय बैठकों में गिरावट
- स्वतंत्र भारत के प्रारंभिक वर्षों में संसदीय सत्र अधिक नियमित होते थे तथा बहसें अधिक व्यापक होती थीं।
- पहली लोक सभा (1952-57) 677 दिनों तक चली, जिसमें विधायी चर्चाओं पर काफी समय व्यतीत हुआ।
- इसके विपरीत, हाल के दशकों में संसदीय बैठकों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है।
- 1990 के दशक से, पांच वर्ष के कार्यकाल में लोकसभा के सत्र औसतन केवल 345 दिन ही चले हैं, तथा 17वीं लोकसभा अपने पूरे कार्यकाल में केवल 274 दिन ही बैठी।
विधायी जांच का क्षरण
- संसद की महत्वपूर्ण भूमिका कानून की जांच करना और उसे परिष्कृत करना है।
- यह कार्य पारंपरिक रूप से विधेयकों को संसदीय समितियों को भेजकर किया जाता था, जिससे गहन विश्लेषण और हितधारकों की सहभागिता का अवसर मिलता था।
केंद्रीय बजट पर बहस कम होती जा रही है
- आर्थिक नियोजन के लिए महत्वपूर्ण केन्द्रीय बजट पर पहले भी संसद में व्यापक ध्यान दिया गया है।
- 1990 से पहले, बजट चर्चा औसतन 120 घंटे तक चलती थी, जिससे राजकोषीय नीतियों पर गहन बहस का अवसर मिलता था।
- हाल ही में, यह समय घटकर मात्र 35 घंटे रह गया है, क्योंकि कुछ बजट बिना किसी चर्चा के ही पारित कर दिए गए, जिससे संसद की राजकोषीय निगरानी की भूमिका कमजोर हो गई।
व्यवधान और ध्रुवीकरण
- संसदीय कार्यवाही दलीय विवादों के कारण तेजी से बाधित हो रही है, जिसके कारण समय और संसाधनों की बर्बादी हो रही है।
- उदाहरण के लिए, 15वीं लोकसभा में व्यवधानों के कारण निर्धारित समय का 37% समय नष्ट हुआ, जबकि 16वीं लोकसभा में 16% समय नष्ट हुआ।
- ये व्यवधान वैचारिक ध्रुवीकरण और रचनात्मक संवाद में शामिल होने की इच्छा की कमी से उत्पन्न होते हैं।
संविधान सभा से आज के सांसदों के लिए सबक
आम सहमति और राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता
- संविधान सभा के सदस्यों ने अपनी जिम्मेदारियों के महत्व को पहचाना और अपनी भिन्न-भिन्न मान्यताओं के बावजूद राष्ट्रीय एकता के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई।
- उनकी चर्चाएँ व्यक्तिगत या पार्टी हितों से ऊपर उठकर सामान्य भलाई पर केंद्रित थीं।
- इसके विपरीत, वर्तमान संसदीय सत्र अक्सर ध्रुवीकरण और विरोधी राजनीति से प्रभावित रहते हैं।
रचनात्मक संवाद और सम्मानजनक असहमति को अपनाना
- संविधान सभा के सदस्यों में प्रायः तीव्र मतभेद होते थे, फिर भी उनकी बहस सम्मानजनक होती थी और व्यक्तिगत हमलों के बजाय विचारों पर केंद्रित होती थी।
- असहमति व्यक्त करने वाले योगदानकर्ताओं को स्वीकार करने से, भले ही वे बहुमत से भिन्न हों, चर्चा समृद्ध हुई और संविधान के प्रावधानों में सुधार हुआ।
- आज के सांसदों को यह समझना चाहिए कि सम्मानजनक असहमति प्रगति को गति दे सकती है, क्योंकि व्यवधान और शत्रुतापूर्ण बयानबाजी की वर्तमान प्रवृत्तियां बहस की गुणवत्ता को कम कर रही हैं।
वैचारिक विभाजन को पाटना
- संविधान सभा ने भारत की विविधता का प्रतिनिधित्व किया तथा देश के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण तैयार करने में सफल रही।
- यह सफलता सदस्यों द्वारा वैचारिक मतभेदों के ऊपर राष्ट्र निर्माण को प्राथमिकता देने के कारण थी।
- आज के जटिल राजनीतिक माहौल में इन विभाजनों को पाटना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।
निष्कर्ष
- भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ न केवल एक ऐतिहासिक उपलब्धि का उत्सव है, बल्कि कार्रवाई का आह्वान भी है।
- संविधान सभा के चरित्र से सीख लेकर वर्तमान सांसद भारत की संसदीय संस्कृति में उभरी लोकतांत्रिक कमियों से निपट सकते हैं।
- सम्मानजनक असहमति, सामूहिक दृष्टिकोण और राष्ट्र-निर्माण की विरासत भारत के लोकतंत्र के भविष्य की पुनर्कल्पना के लिए एक रोडमैप प्रदान करती है।
जीएस3/अर्थव्यवस्था
भारत का व्यापार घाटा अनिवार्यतः कमज़ोरी क्यों नहीं है?
स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस
चर्चा में क्यों?
भारत का चल रहा व्यापार घाटा, जहाँ आयात का मूल्य निर्यात से अधिक है, को कमज़ोर विनिर्माण के संकेत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसके बजाय, यह सेवा क्षेत्र में भारत की ताकत और विदेशी निवेश के लिए एक गंतव्य के रूप में इसके आकर्षण को रेखांकित करता है। इन ताकतों को देखते हुए, यह उम्मीद की जाती है कि माल व्यापार घाटा जारी रहेगा। भारतीय विनिर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए, केवल निर्यात पर निर्भर रहने के बजाय घरेलू मांग को बढ़ाने पर ज़ोर दिया जाना चाहिए।
प्रसंग
- भारत का सतत व्यापार घाटा ऐसी स्थिति से चिह्नित है जहां आयात लगातार निर्यात से अधिक होता है।
- यह परिदृश्य विनिर्माण क्षमताओं में कमी का संकेत नहीं देता है, बल्कि भारत के मजबूत सेवा क्षेत्र और अनुकूल निवेश स्थान के रूप में इसकी स्थिति को उजागर करता है।
पूंजी प्रवाह और चालू खाता घाटे के बीच संबंध
- चालू खाता घाटा (सीएडी) तब होता है जब किसी देश का माल और सेवाओं का आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाता है, जिससे शुद्ध आयात की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
- भारत का चालू खाता घाटा (सीएडी) 2024-25 की पहली तिमाही में थोड़ा बढ़कर 9.7 बिलियन डॉलर (जीडीपी का 1.1%) हो गया, जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही में 8.9 बिलियन डॉलर (जीडीपी का 1.0%) था।
विदेशी निवेश और चालू खाता घाटा
- विदेशी निवेश और चालू खाता घाटा आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं; निवेश आकर्षित करने वाले देशों को या तो चालू खाता घाटा उठाना होगा या विदेशी मुद्रा भंडार का निर्माण करना होगा।
- यह संतुलन सुनिश्चित करता है कि देश में आने और देश से बाहर जाने वाले धन का कुल प्रवाह बराबर बना रहे।
- जब विदेशी निवेश आता है, तो उसके बराबर मात्रा में विदेशी निवेश भी आवश्यक होता है, जो प्रायः वस्तुओं और सेवाओं के आयात के रूप में प्रकट होता है।
- गणितीय रूप से, इस संबंध को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है: पूंजी प्रवाह = चालू खाता घाटा + आरक्षित निधि में वृद्धि।
पूंजी प्रवाह के प्रति भारत का दृष्टिकोण
- भारत का लक्ष्य घरेलू बचत बढ़ाने के लिए विदेशी निवेश को आकर्षित करना है, जिससे उच्च निवेश को समर्थन मिलेगा तथा त्वरित आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
- यह रणनीति भारत के व्यापक विकासात्मक उद्देश्यों के अनुरूप है।
विदेशी मुद्रा भंडार की भूमिका और लागत
- विदेशी मुद्रा भंडार आर्थिक उतार-चढ़ाव, जैसे तेल की कीमतों में उछाल, के विरुद्ध सुरक्षात्मक बफर के रूप में कार्य करता है, तथा चालू खाता घाटे के प्रबंधन में लचीलापन प्रदान करता है।
- हालाँकि, इन भंडारों को बनाए रखने में लागत आती है, क्योंकि भारत अपने भंडारों से अर्जित आय की तुलना में विदेशी निवेशकों को अधिक रिटर्न देता है।
पूंजी प्रवाह और चालू खाता घाटा
- पूंजी का प्रवाह चालू खाता घाटे और आरक्षित निधियों के संचय के योग के अनुरूप होना चाहिए।
- चूंकि भारत को व्यापक आरक्षित निधि संचय की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये अंतर्वाह सीधे चालू खाता घाटे से जुड़े हैं।
- इसका तात्पर्य यह है कि विदेशी निवेश को आकर्षित करने का अर्थ स्वाभाविक रूप से वस्तुओं और सेवाओं के शुद्ध आयात को स्वीकार करना है।
भारत की संतुलित नीति
- भारत चालू खाता घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 2% पर बनाए रखने की सतर्क नीति अपनाता है, जिसे समतुल्य पूंजी प्रवाह द्वारा संतुलित किया जाता है, जो एक निवेश केंद्र के रूप में इसके आकर्षण को उजागर करता है।
भारत के चालू खाता घाटे की संरचना: वस्तुएँ और सेवाएँ
- भारत में चालू खाता घाटा मुख्यतः निर्यात की तुलना में अधिक आयात के कारण है।
- यह घाटा विभिन्न क्षेत्रों, विशेषकर सेवाओं में भारत की तुलनात्मक बढ़त से नियंत्रित होता है।
- भारत सेवाओं का शुद्ध निर्यातक है, तथा आईटी, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है, जिससे उसके आयात व्यय की भरपाई करने में मदद मिलती है।
- परिणामस्वरूप, जबकि भारत अधिक वस्तुओं का आयात करता है, इसका मजबूत सेवा निर्यात समग्र चालू खाता घाटे को प्रबंधनीय बनाए रखता है।
विनिर्माण और तुलनात्मक लाभ
- भारत के विनिर्माण निर्यात, विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल्स और ऑटो घटकों में, चालू खाता घाटे को बनाए रखने के लिए पर्याप्त हैं।
- यह सफलता वियतनाम या बांग्लादेश जैसे देशों की तुलना में विनिर्माण उत्पादकता में कमी के कारण नहीं, बल्कि इन क्षेत्रों में भारत की तुलनात्मक बढ़त के कारण है।
- सेवाओं में भारत की बढ़त उसके विनिर्माण लाभ पर भारी पड़ रही है, जिससे व्यापार संतुलन प्रभावित हो रहा है।
विनिर्माण क्षेत्र में तीव्र वृद्धि की संभावना
- यद्यपि भारत का विनिर्माण क्षेत्र अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, फिर भी इसमें तीव्र वृद्धि की सम्भावना बनी हुई है।
- इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए घरेलू मांग में वृद्धि आवश्यक है।
- यदि घरेलू खपत बढ़ती है और चालू खाता घाटा स्थिर रहता है, तो मांग में यह वृद्धि घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देगी, जिससे विनिर्माण क्षेत्र में तीव्र वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।
- इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत के विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार केवल निर्यात अवसरों पर निर्भर होने के बजाय आंतरिक बाजार की गतिशीलता से निकटता से जुड़ा हुआ है।
जीएस2/शासन
पैन 2.0 परियोजना
स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया
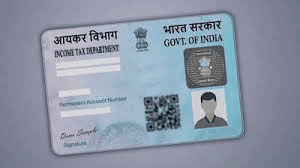
चर्चा में क्यों?
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने पैन 2.0 परियोजना को मंजूरी दे दी है।
पैन 2.0 परियोजना के बारे में:
- पैन 2.0 परियोजना एक ई-गवर्नेंस पहल है जिसका उद्देश्य पैन/टैन सेवाओं में प्रौद्योगिकी आधारित सुधार के माध्यम से करदाता पंजीकरण सेवाओं को पुनः तैयार करना है, जिससे करदाताओं के लिए डिजिटल अनुभव में वृद्धि होगी।
- यह परियोजना मौजूदा PAN/TAN 1.0 पारिस्थितिकी तंत्र का उन्नयन दर्शाती है, जो PAN/TAN से संबंधित मुख्य और गैर-मुख्य दोनों गतिविधियों को समेकित करती है, साथ ही PAN सत्यापन सेवाओं में सुधार करती है।
- इसका नेतृत्व आयकर विभाग द्वारा किया जाता है।
पैन 2.0 परियोजना के लाभ:
- सेवाओं की बेहतर पहुंच और तीव्र वितरण, जिससे समग्र गुणवत्ता में वृद्धि होगी।
- सत्य के एकल स्रोत की स्थापना, जिससे सभी क्षेत्रों में आंकड़ों की एकरूपता सुनिश्चित हो सके।
- लागत अनुकूलन प्रयासों के साथ-साथ पर्यावरण अनुकूल प्रक्रियाओं को अपनाना।
- परिचालन कुशलता बढ़ाने के लिए उन्नत सुरक्षा उपाय और बुनियादी ढांचे का अनुकूलन।
यह पहल डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में निहित सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो नामित सरकारी एजेंसियों द्वारा नियोजित विभिन्न डिजिटल प्रणालियों में एक सामान्य पहचानकर्ता के रूप में पैन के उपयोग को सुविधाजनक बनाती है।
स्थायी खाता संख्या (पैन) क्या है?
- पैन आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाने वाला दस अक्षरों वाला अल्फ़ान्यूमेरिक पहचान-पत्र है।
- यह पहचान-पत्र किसी भी "व्यक्ति" को आवेदन करने पर दिया जाता है, या विभाग द्वारा बिना किसी औपचारिक अनुरोध के सीधे आवंटित किया जा सकता है।
- आयकर विभाग किसी व्यक्ति से संबंधित सभी लेन-देन को ट्रैक करने और लिंक करने के लिए पैन का उपयोग करता है, जिसमें कर भुगतान, टीडीएस/टीसीएस क्रेडिट, आयकर रिटर्न, विशिष्ट लेनदेन और आधिकारिक संचार जैसी गतिविधियां शामिल हैं।
जीएस3/अर्थव्यवस्था
राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार
स्रोत: ईटीवी भारत
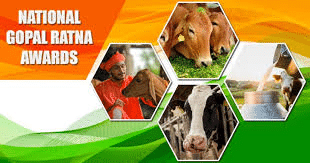
चर्चा में क्यों?
हाल ही में पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) ने वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार (एनजीआरए) के विजेताओं की घोषणा की।
राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार के बारे में:
- राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार पशुधन और डेयरी क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है।
- ये पुरस्कार राष्ट्रीय दुग्ध दिवस समारोह के दौरान प्रदान किये जाते हैं।
- इन पुरस्कारों का उद्देश्य पशुपालन और डेयरी उद्योगों में विभिन्न हितधारकों के प्रयासों को मान्यता देना और बढ़ावा देना है, जिनमें शामिल हैं:
- किसान देशी नस्ल के पशु पाल रहे हैं।
- कृत्रिम गर्भाधान (एआई) तकनीशियन।
- डेयरी सहकारी समितियां, दूध उत्पादक कंपनियां, और डेयरी किसान उत्पादक संगठन।
- पुरस्कारों को तीन मुख्य क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है:
- सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान स्वदेशी मवेशी/भैंस नस्लों का पालन करते हैं।
- सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (एआईटी)।
- सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी/दूध उत्पादक कंपनी/डेयरी किसान उत्पादक संगठन।
- इस वर्ष, पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) राज्यों के लिए तीनों पुरस्कार श्रेणियों में एक विशेष पुरस्कार श्रेणी शुरू की गई है ताकि उस क्षेत्र में डेयरी विकास गतिविधियों को प्रोत्साहित और बढ़ाया जा सके।
जीएस1/इतिहास और संस्कृति
500 साल पहले इसी दिन पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त की थी
स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस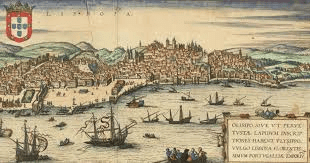
चर्चा में क्यों?
25 नवंबर को, 500 साल से भी अधिक पहले, पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला क्षेत्रीय कब्ज़ा स्थापित किया, जिससे इस क्षेत्र में उनके 400 साल के औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई, जो 1961 में समाप्त हो गया। यह घटना भारत से बाहर जाने वाली अंतिम औपनिवेशिक शक्ति का प्रतीक है।
पुर्तगाली गोवा क्यों आये?
- 1498 में वास्को-डि-गामा की यात्रा ने हिंद महासागर में जीवंत व्यापार नेटवर्क का खुलासा किया।
- पुर्तगालियों का उद्देश्य इन व्यापार मार्गों से धन कमाना था।
- मुस्लिम-नियंत्रित व्यापार मार्गों के साथ प्रतिस्पर्धा ने पुर्तगालियों को इस क्षेत्र में सैन्य प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रेरित किया।
- पुर्तगाली भारत राज्य की औपचारिक स्थापना वास्को-डि-गामा के आगमन के छह वर्ष बाद 1505 में हुई।
- फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पहले वायसराय बने और उन्होंने फोर्ट मैनुअल (अब कोच्चि) में प्रारंभिक बेस स्थापित किया।
- पुर्तगालियों ने बोम बाहिया (बाद में बॉम्बे) पर तब तक नियंत्रण बनाए रखा जब तक कि इसे 1661 में इंग्लैंड को नहीं सौंप दिया गया।
अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा पर कैसे विजय प्राप्त की?
- अल्बुकर्क, जो 1509 से 1515 तक वायसराय के रूप में कार्यरत थे, ने समुद्री व्यापार मार्गों को नियंत्रित करने के लिए गोवा के सामरिक महत्व को पहचाना।
- गोवा पर आक्रमण करने का उनका निर्णय तिम्मय्या से प्रभावित था, जिसे या तो मालाबारी समुद्री डाकू या विजयनगर साम्राज्य से जुड़ा एक कुलीन व्यक्ति बताया जाता है।
- फरवरी-मार्च 1510 में गोवा पर अपने पहले हमले के दौरान, अल्बुकर्क को हिंदू आबादी के बीच सुल्तान यूसुफ आदिल शाह की अलोकप्रियता के कारण सफलता मिली, जिनमें से कई ने पुर्तगालियों का समर्थन किया था।
- मानसून के दौरान चुनौतियों का सामना करने के बाद, अल्बुकर्क को पुर्तगाल से सुदृढीकरण प्राप्त हुआ।
- नवंबर 1510 में, अतिरिक्त सेना के साथ, उन्होंने गोवा पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया।
तिम्मैया कौन थे?
- तिम्मय्या गोवा की विजय में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जिसका वर्णन विभिन्न ऐतिहासिक वृत्तांतों में किया गया है।
- कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वह कुलीन वंश से थे और विजयनगर नौसेना में महत्वपूर्ण पद पर थे।
- हालाँकि पुर्तगाली उसे एक समुद्री डाकू के रूप में देखते थे, लेकिन वास्तव में वह विजयनगर साम्राज्य की ओर से प्रतिद्वंद्वी व्यापारी जहाजों को निशाना बनाकर आदेशों का पालन कर रहा था।
- इतिहासकार इस बात पर बहस करते हैं कि अल्बुकर्क के हमले के समय पर तिम्मय्या का कितना प्रभाव था; कुछ का मानना है कि उसने पहले से मौजूद योजना को और मजबूत किया।
तिम्मय्या गोवा पर विजय क्यों चाहते थे?
- विजयनगर शासकों की गोवा पर लंबे समय से लालच था, खासकर तब जब यह बीजापुर के सुल्तान के अधीन हो गया।
- तिम्मय्या की प्रेरणा संभवतः विजयनगर साम्राज्य के रणनीतिक हितों से प्रेरित थी, ताकि आर्थिक रूप से मूल्यवान क्षेत्र पर पुनः नियंत्रण प्राप्त किया जा सके।
जीएस1/इतिहास और संस्कृति
राजा राजा चोल प्रथम
स्रोत: द हिंदू
चर्चा में क्यों?
महान चोल सम्राट राजा राज चोल प्रथम की जयंती हर वर्ष तमिलनाडु के तंजावुर में साध्या विज्हा के दौरान मनाई जाती है।
राजा राज चोल प्रथम के बारे में:
- 947 ई. में अरुलमोझी वर्मन के रूप में जन्मे, वे इतिहास के सबसे सम्मानित और दूरदर्शी शासकों में से एक बन गये।
- उन्हें राजा राजा महान के नाम से जाना जाता है, उन्हें अपने पूर्वजों से एक समृद्ध विरासत विरासत में मिली थी और उन्होंने एक ऐसे साम्राज्य का निर्माण किया जो सैन्य और सांस्कृतिक दोनों दृष्टि से समृद्ध था।
शासन:
- उनका शासनकाल 985 से 1014 ई. तक चला, जो उल्लेखनीय सैन्य उपलब्धियों और नवीन प्रशासनिक रणनीतियों के लिए जाना जाता है।
सैन्य विजय:
- उनके शासन के तहत, चोल राजवंश ने दक्षिण भारत से परे काफी विस्तार किया, जिसका क्षेत्र दक्षिण में श्रीलंका से लेकर उत्तर में कलिंग तक फैला हुआ था।
- उन्होंने कई नौसैनिक अभियान चलाये और मालाबार तट, मालदीव और श्रीलंका पर सफलतापूर्वक कब्ज़ा कर लिया।
शीर्षक:
- पांड्यों को पराजित करने के बाद उन्होंने "पांड्य कुलाशनी" की उपाधि धारण की, जो पांड्य वंश के लिए वज्रपात का प्रतीक है।
- उन्होंने "मुम्मुडी" की उपाधि भी ग्रहण की, जिसका अर्थ है "वह चोल जो तीन मुकुट पहनता है।"
वास्तुकला उपलब्धियां:
- 1010 में, राजराजा ने भगवान शिव को समर्पित तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया।
- यह मंदिर और राजधानी शहर धार्मिक भक्ति और आर्थिक गतिविधियों दोनों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र बन गए।
सांस्कृतिक योगदान:
- उनके शासनकाल के दौरान, महत्वपूर्ण साहित्यिक कृतियाँ संकलित की गईं, जिनमें तमिल कवियों अप्पार, संबंदर और सुंदरार के ग्रंथ शामिल थे, जिन्हें थिरुमुरई नामक एकल संग्रह में संपादित किया गया था।
जीएस1/भारतीय समाज
#AbKoiBahanaNahi Campaign
स्रोत : डेक्कन हेराल्ड

चर्चा में क्यों?
महिलाओं को सशक्त बनाने और लिंग आधारित हिंसा को समाप्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत नई दिल्ली में की गई।
द्वारा लॉन्च किया गया:
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- ग्रामीण विकास मंत्रालय
- संयुक्त राष्ट्र महिला से समर्थन
लक्ष्य और उद्देश्य
- लिंग आधारित हिंसा को समाप्त करना: पूरे भारत में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए जागरूकता और तत्परता बढ़ाना।
- गरिमा और समानता: महिलाओं को हिंसा की रिपोर्ट करने और उनके अधिकारों की वकालत करने के लिए सशक्त बनाना, तथा उनकी गरिमा को बढ़ावा देना।
- अर्थव्यवस्था में लैंगिक समानता: विकसित भारत में योगदान देने के लिए सभी क्षेत्रों में महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करना।
कार्यान्वयन और संरचनात्मक अधिदेश
- राष्ट्रीय कार्रवाई आह्वान: सभी हितधारकों - जिसमें नागरिक, गैर सरकारी संगठन और सरकारी एजेंसियां शामिल हैं - से लिंग आधारित हिंसा को समाप्त करने के प्रयासों में सक्रिय रूप से शामिल होने की सामूहिक अपील।
- वैश्विक अभियानों के साथ संरेखण: यह पहल संयुक्त राष्ट्र की #NoExcuse वैश्विक पहल के अनुरूप है, जो बढ़ती हिंसा के खिलाफ जवाबदेही और कार्रवाई की मांग करती है।
- सहायक हस्तक्षेप: सरकार की पहल का उद्देश्य महिलाओं के कठिन परिश्रम को कम करना, वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना, लैंगिक डिजिटल विभाजन को पाटना और महिलाओं के लिए सुरक्षित स्थान बनाना है।
- महत्व
- सम्मान के लिए सशक्तिकरण: यह अभियान महिलाओं को सामाजिक बंधनों से मुक्त होकर अपनी गरिमा स्थापित करने का अधिकार देता है।
- राष्ट्रीय विकास में महिलाओं की भूमिका: इस बात पर बल दिया गया कि 2047 तक भारत की प्रगति के लिए लैंगिक समानता प्राप्त करना महत्वपूर्ण है।
- महिला अधिकारों को समर्थन: लिंग-संवेदनशील कानून, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और आर्थिक अवसरों सहित महिला अधिकारों के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की वकालत करना।
जीएस3/पर्यावरण
ग्लोबल मैचमेकिंग प्लेटफॉर्म (जीएमपी)
स्रोत : डीटीई

चर्चा में क्यों?
ग्लोबल मैचमेकिंग प्लेटफ़ॉर्म (GMP) को संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (UNIDO) ने क्लाइमेट क्लब के सहयोग से लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य भारी उत्सर्जन वाले उद्योगों, विशेष रूप से उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में कार्बन मुक्त करने की प्रक्रिया को तेज़ करना है, और इसे भागीदार देशों और महत्वपूर्ण दाता संगठनों की उपस्थिति में आयोजित एक कार्यक्रम में पेश किया गया।
चाबी छीनना
- जीएमपी को उन उद्योगों में डीकार्बोनाइजेशन प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
- उद्देश्य और लक्ष्य
- डीकार्बोनाइजेशन: जीएमपी का मुख्य उद्देश्य उन उद्योगों से कार्बन उत्सर्जन में तेजी से कमी लाना है जो प्रमुख ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जक हैं।
- तकनीकी और वित्तीय समाधान: यह मंच राष्ट्रों को तकनीकी और वित्तीय संसाधनों से जोड़ता है जिसका उद्देश्य ऊर्जा-गहन क्षेत्रों में उत्सर्जन को न्यूनतम करना है।
यह काम किस प्रकार करता है
- सिंगल-पॉइंट गेटवे: जीएमपी एक केंद्रीकृत मंच के रूप में कार्य करता है, जो विकासशील देशों की सरकारों को अनुकूलित अनुरोध प्रस्तुत करने और वैश्विक स्तर पर अग्रणी तकनीकी और वित्तीय समाधान खोजने की अनुमति देता है।
- मैचमेकिंग प्रक्रिया: यह एक ऐसी प्रक्रिया को सुगम बनाती है, जिसमें देशों की विशिष्ट आवश्यकताओं को साझेदार संगठनों से उपयुक्त तकनीकी और वित्तीय सहायता के साथ संरेखित किया जाता है।
- पायलट परियोजनाएं: अर्जेंटीना, कोलंबिया, चिली, मिस्र, इंडोनेशिया, केन्या, मोरक्को और कंबोडिया सहित कई देशों में पायलट परियोजनाओं के लिए प्रारंभिक चर्चा पहले से ही चल रही है।
समर्थन और भागीदारी
- जलवायु क्लब: जीएमपी जलवायु क्लब के लिए एक सहायक तंत्र के रूप में कार्य करता है, जिसका सचिवालय यूएनआईडीओ में स्थित है।
- वितरण भागीदार: इस पहल को क्रियान्वित करने में शामिल महत्वपूर्ण भागीदारों में जलवायु निवेश कोष, जर्मन विकास सहयोग (जीआईजेड), यूएनआईडीओ और विश्व बैंक शामिल हैं।
- प्रारंभिक वित्तपोषण: इस मंच को जर्मन संघीय आर्थिक सहयोग और जलवायु कार्रवाई मंत्रालय (BMWK) से प्रारंभिक वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है।
जीएस3/अर्थव्यवस्था
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई)
स्रोत: बिजनेस स्टैंडर्ड

चर्चा में क्यों?
उद्यम पोर्टल के हालिया आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) ने पिछले 15 महीनों में लगभग 10 करोड़ नए रोजगार सृजित किए हैं। यह पंजीकृत एमएसएमई की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है, जो पिछले वर्ष के अगस्त से 2.33 करोड़ से बढ़कर 5.49 करोड़ हो गई है। इसी समयावधि के दौरान इन उद्यमों द्वारा रिपोर्ट की गई नौकरियों की संख्या भी नाटकीय रूप से 13.15 करोड़ से बढ़कर 23.14 करोड़ हो गई है।
परिभाषा और वर्गीकरण
- सूक्ष्म उद्यम: इन्हें ऐसे उद्यम के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिनका संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश 1 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है और वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।
- लघु उद्यम: लघु उद्यम वे हैं जिनके संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश ₹10 करोड़ तक है और जिनका वार्षिक कारोबार ₹50 करोड़ से अधिक नहीं है।
- मध्यम उद्यम: मध्यम उद्यमों को ऐसे उद्यमों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जिनका संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश 50 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है और वार्षिक कारोबार 250 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।
महत्व
- आर्थिक योगदान: एमएसएमई भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 30% का योगदान देते हैं। वे आर्थिक विकास और स्थिरता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- रोजगार सृजन: ये उद्यम महत्वपूर्ण रोजगार सृजनकर्ता हैं, जो देश भर में लाखों व्यक्तियों को आजीविका प्रदान करते हैं।
- नवाचार और उद्यमिता: एमएसएमई नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे अक्सर नए उत्पादों और सेवाओं का सृजन होता है जो विविध बाजार आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।
सरकारी सहायता
- बजट आवंटन में वृद्धि: भारत सरकार ने एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए उल्लेखनीय प्रयास किए हैं, 2024-25 के केंद्रीय बजट में एमएसएमई मंत्रालय को 22,137.95 करोड़ रुपये का पर्याप्त आवंटन किया गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 41.6% की वृद्धि दर्शाता है।
- डिजिटल पहल: प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और एमएसएमई को सहायता प्रदान करने के लिए उद्यम पंजीकरण और एमएसएमई संबंध पोर्टल जैसी पहल शुरू की गई हैं।
- चैम्पियंस प्लेटफॉर्म: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया चैम्पियंस प्लेटफॉर्म एमएसएमई और नए उद्यमियों को समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करता है, जिससे उनकी वृद्धि और सफलता में सहायता मिलती है।
|
3127 docs|1043 tests
|















