UPSC Daily Current Affairs(Hindi): 19th November 2024 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly PDF Download
जीएस2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध
पूर्वी समुद्री गलियारा (ईएमसी) क्या है?
स्रोत: इकोनॉमिक टाइम्स

चर्चा में क्यों?
बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री ने कहा कि चेन्नई-व्लादिवोस्तोक पूर्वी समुद्री गलियारा हाल ही में चालू हो गया है, जिससे तेल, खाद्य और मशीनरी का परिवहन सुगम हो गया है।
पूर्वी समुद्री गलियारे (ईएमसी) का अवलोकन
- चेन्नई को व्लादिवोस्तोक से जोड़ने वाली ईएमसी का उद्देश्य भारत और रूस के बीच समुद्री व्यापार को बढ़ाना है।
- यह गलियारा माल परिवहन के समय को काफी कम कर देता है, अर्थात इसमें 16 दिन तक की कमी आती है।
- दूरी लगभग 40% कम हो जाती है, जिससे परिवहन दक्षता में सुधार होता है।
वर्तमान मार्ग तुलना
- मुंबई से सेंट पीटर्सबर्ग तक का पारंपरिक मार्ग 8,675 समुद्री मील (16,066 किमी) लंबा है।
- वर्तमान में, एक बड़े कंटेनर जहाज को यूरोप के रास्ते रूस के सुदूर पूर्व तक पहुंचने में लगभग 40 दिन लगते हैं।
- इसके विपरीत, चेन्नई से व्लादिवोस्तोक तक ईएमसी मार्ग केवल 5,647 समुद्री मील (10,458 किमी) का है।
तार्किक लाभ
- ईएमसी से दूरी में 5,608 किमी की पर्याप्त बचत होती है, जिससे परिवहन लागत में कमी आती है।
- इस सुधार से भारत, रूस और अन्य एशियाई देशों के बीच माल परिवहन की दक्षता बढ़ेगी।
भौगोलिक मार्ग विवरण
- ईएमसी महत्वपूर्ण जल निकायों से होकर गुजरता है, जिनमें शामिल हैं:
- जापान सागर
- पूर्वी चीन का समुद्र
- दक्षिण चीन सागर
- Malacca Straits
- अंडमान सागर
- बंगाल की खाड़ी
मार्ग में संभावित पड़ाव
- यदि आवश्यक हो तो मार्ग में विभिन्न ठहरावों की अनुमति है, जिनमें शामिल हैं:
- डेलियन
- शंघाई
- हांगकांग
- हो ची मिन्ह सिटी
- सिंगापुर
- क्वालालंपुर
- बैंकाक
- ढाका
- कोलंबो
- चेन्नई
जीएस2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध
रियो में जी-20 शिखर सम्मेलन शुरू
स्रोत : इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?
जी-20 शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो के आधुनिक कला संग्रहालय में शुरू हुआ, जिसकी मेज़बानी ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुईज़ इनासियो लूला दा सिल्वा ने की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन और चीन के शी जिनपिंग सहित प्रमुख नेता व्यापार, जलवायु परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित चर्चाओं में शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 'सामाजिक समावेशन और भूख और गरीबी के खिलाफ़ लड़ाई' पर केंद्रित उद्घाटन सत्र को संबोधित किया।
प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए भाषण के मुख्य अंश
- अवलोकन
- जी-20 यूरोपीय संघ सहित 19 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों का गठबंधन है, जिसकी स्थापना 1999 में हुई थी।
- 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के प्रत्युत्तर में, इसे 2008 में राज्य एवं सरकार प्रमुखों के लिए एक मंच के रूप में उन्नत किया गया।
- यह एक विधायी निकाय के बजाय एक मंच के रूप में कार्य करता है, जिसका अर्थ है कि इसके समझौतों और निर्णयों को कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं है, लेकिन वे राष्ट्रीय नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा दे सकते हैं।
- सदस्यों
- जी-20 में 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं, जिनमें शामिल हैं:
- अर्जेंटीना
- ऑस्ट्रेलिया
- ब्राज़िल
- कनाडा
- चीन
- फ्रांस
- जर्मनी
- भारत
- इंडोनेशिया
- इटली
- जापान
- मेक्सिको
- रूस
- सऊदी अरब
- दक्षिण अफ़्रीका
- दक्षिण कोरिया
- टर्की
- यूनाइटेड किंगडम
- संयुक्त राज्य अमेरिका
- विशेष आमंत्रितों में अतिथि राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व बैंक जैसे संगठन शामिल हैं जो जी-20 शिखर सम्मेलनों में भाग लेते हैं।
- जी-20 में 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं, जिनमें शामिल हैं:
- लक्ष्य/उद्देश्य
- आर्थिक स्थिरता: वैश्विक आर्थिक विकास और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना।
- सतत विकास: जलवायु परिवर्तन से निपटने और समान विकास को बढ़ावा देने वाली नीतियों को आगे बढ़ाना।
- संकट प्रबंधन: वित्तीय और स्वास्थ्य संकटों, जैसे कि COVID-19, के प्रति प्रतिक्रियाओं का समन्वय करना।
- वैश्विक सहयोग: व्यापार, निवेश और नवाचार पर बहुपक्षीय सहयोग बढ़ाना।
- समावेशिता: उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण, दोनों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।
- उपलब्धियां (उदाहरण)
- वित्तीय संकट शमन (2008): वैश्विक वित्तीय संकट से निपटने और गहरी मंदी को रोकने के लिए समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयास।
- पेरिस समझौता समर्थन (2015): जलवायु परिवर्तन उद्देश्यों पर अंतर्राष्ट्रीय आम सहमति बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
- विकासशील देशों के लिए ऋण राहत (2020): कमज़ोर देशों की सहायता के लिए महामारी के दौरान ऋण सेवा निलंबन पहल (डीएसएसआई) की शुरुआत की गई।
- कोविड-19 महामारी: वैश्विक सहयोग के माध्यम से वैक्सीन वितरण और आर्थिक सुधार योजनाओं को तैयार करने में भूमिका निभाई।
- मार्च 2020 में, जी-20 नेताओं ने कोरोनावायरस महामारी के आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था में 5 ट्रिलियन डॉलर डालने की प्रतिबद्धता जताई थी।
- डिजिटल परिवर्तन (2023): भारत की जी-20 अध्यक्षता के दौरान वैश्विक डिजिटल विभाजन को संबोधित करने के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- जी-20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के मुख्य अंश
- सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर ध्यान केंद्रित: सतत विकास लक्ष्यों को प्राथमिकता देने और वैश्विक दक्षिण की चिंताओं के लिए ब्राजील के एजेंडे की सराहना की गई।
- भारत की जी-20 अध्यक्षता की थीम: "एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य" की निरंतरता पर प्रकाश डाला गया।
- गरीबी उन्मूलन और खाद्य सुरक्षा में भारत की उपलब्धियाँ:
- पिछले दशक में 250 मिलियन व्यक्तियों को सफलतापूर्वक गरीबी से बाहर निकाला गया।
- 800 मिलियन नागरिकों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराता है।
- विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना से 550 मिलियन लोग लाभान्वित होते हैं।
- खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए 'बैक टू बेसिक्स एंड मार्च टू फ्यूचर' रणनीति को बढ़ावा दिया गया।
- वैश्विक योगदान और सहयोग: अफ्रीका में खाद्य सुरक्षा को मजबूत किया, मलावी, जाम्बिया और जिम्बाब्वे को मानवीय सहायता प्रदान की।
- 'भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन' बनाने की ब्राजील की पहल का समर्थन किया।
- वैश्विक दक्षिण के लिए समर्थन: वैश्विक दक्षिण के समक्ष आने वाले मुद्दों, विशेष रूप से वैश्विक संघर्षों के परिणामस्वरूप उत्पन्न खाद्य, ईंधन और उर्वरक की कमी के संबंध में समस्याओं के समाधान की आवश्यकता पर बल दिया गया।
- महिला-नेतृत्व विकास और पोषण: महिला-नेतृत्व विकास को बढ़ावा देने और खाद्य सुरक्षा प्रयासों के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में पोषण पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से भारत की पहल पर जोर दिया गया।
- विवादास्पद यूक्रेन युद्ध चर्चाएँ:
- संयुक्त वक्तव्य पर बातचीत करना कठिन रहा है, विशेषकर यूक्रेन की स्थिति के संबंध में।
- यूरोपीय नेता हाल ही में हुए रूसी हवाई हमले के बाद सख्त भाषा की वकालत कर रहे हैं, जबकि राष्ट्रपति बिडेन ने घोषणा की है कि अमेरिका रूस के भीतर हमलों के लिए यूक्रेन द्वारा अमेरिकी निर्मित हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंधों में ढील देगा।
- ब्राज़ील का जी-20 एजेंडा:
- ब्राजील के एजेंडे में सतत विकास, अमीरों पर कर लगाना, गरीबी से लड़ना और वैश्विक वित्तीय संस्थाओं में सुधार को प्राथमिकता दी गई है।
- कराधान सुधारों के संबंध में आने वाले अमेरिकी प्रशासन से प्रत्याशित प्रतिरोध चुनौतियां उत्पन्न कर सकता है।
- जलवायु एवं ऊर्जा प्रतिबद्धताएँ:
- राष्ट्रपति बिडेन ने विश्व बैंक के अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को वित्तीय सहायता देने का वादा किया और ब्राजील के साथ स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की।
- इसके विपरीत, शी जिनपिंग ने बेल्ट एंड रोड पहल को बढ़ावा दिया, जबकि ब्राजील ने इसमें भाग नहीं लेने का निर्णय लिया था।
- व्यापार तनाव और आर्थिक नीतियां:
- व्यापार वार्ता पर अमेरिका-चीन व्यापार संघर्ष बढ़ने की चिंता हावी रही, तथा नए टैरिफ की योजनाओं पर चर्चा की गई।
- धनी लोगों पर कर लागू करने के प्रयासों को, विशेष रूप से अर्जेंटीना से, विरोध का सामना करना पड़ा।
जीएस3/पर्यावरण
जीनस कोइमा
स्रोत: डीटीई

चर्चा में क्यों?
शोधकर्ताओं की एक टीम ने कोइमा नामक मीठे पानी की मछली की एक नई प्रजाति की पहचान की है, जो पश्चिमी घाट की मूल निवासी है।
जीनस कोइमा के बारे में:
- "कोइमा" नाम मलयालम भाषा से लिया गया है, जो विशेष रूप से लोचिस (loaches) को संदर्भित करता है।
- इस वंश में दो ज्ञात प्रजातियां शामिल हैं जिन्हें पहले नेमाचेइलस वंश के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।
कोइमा प्रजाति की विशेषताएं:
- इसकी विशेषता पीले-भूरे रंग के आधार के साथ एक विशिष्ट रंग है।
- पार्श्व रेखा के साथ काले धब्बों की एक पंक्ति होती है।
- सभी पंख पारदर्शी होते हैं।
- मछली के पृष्ठ भाग पर कोई समान पट्टियाँ नहीं होतीं।
प्राकृतिक वास:
- कोइमा प्रजातियाँ पश्चिमी घाट की कई नदियों में पाई जाती हैं, जिनमें कुंती, भवानी, मोयार, काबिनी और पम्बर नदियाँ शामिल हैं।
कोइमा वंश से संबंधित प्रजातियाँ:
- कोइमा रेमाडेवी:
- यह प्रजाति आमतौर पर चट्टानों, पत्थरों और बजरी सहित चट्टानी सब्सट्रेट वाली तेज बहने वाली धाराओं में पाई जाती है।
- यह बिखरे हुए रेत और गाद वाले क्षेत्रों में पनपता है।
- कोइमा रेमादेवी चट्टानों के बीच और पत्थरों के नीचे शरण लेती है, जो उन्हें पानी की तेज धाराओं से सुरक्षा प्रदान करता है।
- वर्तमान में, इसका दस्तावेजीकरण केवल कुन्ती नदी में इसके प्रकार के स्थान से ही किया गया है, जो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित है।
- इसका मूल्य क्या है:
- यह प्रजाति कावेरी नदी की विभिन्न सहायक नदियों में निवास करती है।
- यह बड़ी नदियों से लेकर छोटी, तेजी से बहने वाली जलधाराओं तक अनेक सूक्ष्म आवासों में पाया जाता है।
- कोइमा मोनिलिस 350 से 800 मीटर की ऊंचाई पर पाया जा सकता है।
जीएस2/शासन
शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक
स्रोत : पीआईबी
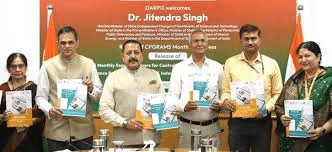
चर्चा में क्यों?
हाल ही में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने शिकायत निवारण मूल्यांकन एवं सूचकांक (जीआरएआई) 2023 लॉन्च किया है।
शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक के बारे में:
- जी.आर.ए.आई. की संकल्पना और विकास भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डी.ए.आर.पी.जी.) द्वारा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों के बाद किया गया था।
- जीआरएआई का प्राथमिक उद्देश्य संगठनों का तुलनात्मक विश्लेषण प्रदान करना है, जिसमें उनकी ताकत और शिकायत निवारण तंत्र में सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों पर प्रकाश डाला जाना है।
- GRAI का उद्घाटन संस्करण, जो GRAI 2022 है, 21 जून 2023 को जारी किया गया।
- कुल 89 केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों का मूल्यांकन किया गया और चार प्रमुख आयामों पर आधारित एक विस्तृत सूचकांक का उपयोग करके रैंकिंग दी गई:
- क्षमता
- प्रतिक्रिया
- कार्यक्षेत्र
- संगठनात्मक प्रतिबद्धता
- मूल्यांकन में वर्ष 2023 के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और प्रबंधन प्रणाली (CPGRAMS) से एकत्रित डेटा का उपयोग किया गया।
- कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय, तथा निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग को क्रमशः समूह ए, बी और सी में शीर्ष रैंकिंग प्राप्त हुई।
- रिपोर्ट विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में शिकायत निवारण की प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाले मूल कारणों की पहचान करने के लिए एक व्यापक द्वि-आयामी विश्लेषण (ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों) प्रदान करती है, जिसे आसानी से व्याख्या करने योग्य रंग-कोडित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है।
- इसके अतिरिक्त, रिपोर्ट में तकनीकी साझेदारियों का भी उल्लेख किया गया है, जो डीएआरपीजी ने शिकायत निवारण के साधन के रूप में सीपीजीआरएएमएस का प्रभावी उपयोग करने में मंत्रालयों और विभागों की सहायता के लिए की है।
- यह शिकायत प्रबंधन में सुधार के लिए मंत्रालयों और विभागों के लिए सीपीजीआरएएमएस और इसकी विशेषताओं, जैसे आईजीएमएस 2.0 और ट्रीडैशबोर्ड, का लाभ उठाने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप और सिफारिशें भी प्रस्तुत करता है।
- सुझाए गए रोडमैप में डेटा विश्लेषण, पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण और निवारक कार्रवाइयों को बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) सहित उन्नत प्रौद्योगिकियों के एकीकरण पर जोर दिया गया है, साथ ही बेहतर रिपोर्टिंग के लिए एटीआर प्रारूपों को अपडेट किया गया है।
- प्रमुख सिफारिशों में शिकायत निवारण अधिकारियों (जीआरओ) के लिए क्षमता निर्माण, नियमित ऑडिट के माध्यम से जवाबदेही बढ़ाना और सीपीजीआरएएमएस एकीकरण को सरकार के तीसरे स्तर तक विस्तारित करना शामिल है।
जीएस3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी
सिकल सेल उन्मूलन पर डाक टिकट जारी – 2047
स्रोत : पीआईबी

चर्चा में क्यों?
मध्य प्रदेश ने वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन के उद्देश्य से की गई पहल को समर्पित एक स्मारक डाक टिकट का अनावरण करके सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया है।
सिकल सेल रोग (एससीडी) क्या है?
- सिकल सेल रोग (SCD) एक आनुवंशिक विकार है, जिसमें लाल रक्त कोशिकाओं का असामान्य आकार होता है, जो अर्धचंद्राकार या दरांती जैसा दिखता है। यह आकार रक्त परिसंचरण को बाधित करता है और गंभीर स्वास्थ्य जटिलताओं को जन्म दे सकता है।
- एस.सी.डी. से जुड़ी जटिलताओं में क्रोनिक एनीमिया, अंग क्षति, सिकल सेल संकट के रूप में जानी जाने वाली दर्दनाक घटनाएं और कम जीवनकाल शामिल हैं।
- यह रोग मुख्य रूप से भारत में हाशिये पर पड़ी जनजातीय आबादी को प्रभावित करता है।
लक्षण :
- क्रोनिक एनीमिया, जिसमें लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है।
- दर्दनाक घटनाएं या संकट जो अचानक घटित हो सकते हैं।
- बच्चों में विकास एवं यौवन में देरी।
इलाज:
- वर्तमान उपचारों में रक्त आधान शामिल है, जिसका उपयोग गंभीर एनीमिया के प्रबंधन के लिए किया जाता है।
- हाइड्रोक्सीयूरिया एक दवा है जो दर्द की आवृत्ति को कम करने में मदद कर सकती है।
- जीन थेरेपी और स्टेम सेल प्रत्यारोपण जैसे उन्नत उपचार विकल्प कुछ रोगियों के लिए दीर्घकालिक समाधान प्रदान कर सकते हैं।
भारत का मिशन:
- वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की घोषणा की गई है, जिसमें 0-40 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए जागरूकता और जांच पर जोर दिया जाएगा।
- एनीमिया मुक्त भारत रणनीति का उद्देश्य पांच वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से द्वि-साप्ताहिक आयरन और फोलिक एसिड अनुपूरण उपलब्ध कराना है।
इस पहल के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?
- लक्ष्य और उद्देश्य:
- 2047 तक सिकल सेल एनीमिया का पूर्ण उन्मूलन।
- जनजातीय समुदायों में जागरूकता और जांच बढ़ाएँ।
- उच्च प्रदर्शन तरल क्रोमैटोग्राफी (एचपीएलसी) जैसे उपकरणों का उपयोग करके सुलभ निदान और उपचार सुनिश्चित करें।
- रोग की रोकथाम के लिए आनुवंशिक परामर्श प्रदान करें।
- मोबाइल ऐप और राष्ट्रीय सिकल सेल पोर्टल के माध्यम से प्रौद्योगिकी-संचालित निगरानी को लागू करना।
- कार्यक्रम की विशेषताएं:
- एम्स भोपाल में नवजात शिशुओं की जांच और प्रसव पूर्व निदान किया जाएगा।
- यह पहल लक्ष्य वर्ष 2047 तक देश भर के 17 राज्यों तक विस्तारित हो जाएगी।
- एचपीएलसी मशीनों का उपयोग करके उन्नत परीक्षण क्षमताओं का उपयोग किया जाएगा।
- सहायता समूहों और शैक्षिक पहलों के माध्यम से सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा दिया जाएगा।
- कार्यान्वयन:
- एम्स भोपाल और संकल्प इंडिया जैसे संस्थानों के साथ-साथ अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ सहयोग स्थापित किया जाएगा।
- यह कार्यक्रम चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा, जिसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के उच्च प्रसार दर वाले क्षेत्रों से होगी।
- सरकारी वित्तपोषण से बुनियादी ढांचे में सुधार और तकनीकी विकास को सहायता मिलेगी।
- डिजिटल प्रौद्योगिकी प्रभावी निगरानी के लिए डेटा संग्रहण और केस प्रबंधन को सुविधाजनक बनाएगी।
जीएस3/पर्यावरण
थाई सैकब्रूड वायरस
स्रोत: फ्रंटिनर्स

चर्चा में क्यों?
शोध से पता चला है कि प्रबंधित मधुमक्खी आबादी और जंगली परागणकों के बीच रोगाणुओं का संचरण होता है, जिसे रोगाणु स्पिलओवर और स्पिलबैक के रूप में जाना जाता है।
थाई सैकब्रूड वायरस का अवलोकन:
- थाई सैकब्रूड वायरस एशियाई मधुमक्खी आबादी के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है।
- पश्चिमी मधुमक्खियों को प्रभावित करने वाला विषाणुजनित वायरस एशियाई मधुमक्खियों की तुलना में कम हानिकारक है।
- इस वायरस के संक्रमण से मुख्यतः मधुमक्खियों के लार्वा की मृत्यु हो जाती है।
भौगोलिक विस्तार:
- 1991 और 1992 के बीच, थाई सैकब्रूड वायरस के प्रकोप के कारण दक्षिण भारत में लगभग 90% एशियाई मधुमक्खी कालोनियां नष्ट हो गईं।
- यह वायरस 2021 में तेलंगाना में फिर से सामने आया और चीन और वियतनाम जैसे अन्य देशों में भी इसकी पहचान की गई है।
भारतीय मधुमक्खियों के बारे में मुख्य तथ्य:
- भारत में मधुमक्खियों की 700 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें चार देशी मधुमक्खियां शामिल हैं:
- एपिस सेराना इंडिका (भारतीय शहद मधुमक्खी)
- एपिस डोर्सटा (विशाल चट्टान मधुमक्खी)
- एपिस फ्लोरिया (बौनी मधुमक्खी)
- ट्राइगोना प्रजाति (डंक रहित मधुमक्खी)
- शहद उत्पादन बढ़ाने के लिए 1983 में पश्चिमी मधुमक्खियां भारत में लाई गईं।
रोगजनक फैलाव को समझना:
- रोगजनक फैलाव से तात्पर्य उस घटना से है जब एक विशिष्ट रोगजनक, एक अलग, अतिसंवेदनशील मेज़बान को सफलतापूर्वक संक्रमित कर देता है।
- इसका एक उदाहरण चमगादड़ से सूअरों में निपाह वायरस का संचरण है।
रोगज़नक़ स्पिलबैक को समझना:
- रोगजनक स्पिलबैक तब होता है जब एक रोगजनक एक नई मेजबान प्रजाति से वापस अपने मूल मेजबान में स्थानांतरित हो जाता है।
- इसका एक उदाहरण मनुष्यों से जंगली चमगादड़ों में SARS-CoV-2 का संचरण है।
जीएस2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध
सूडान के बारे में मुख्य तथ्य
स्रोत : वर्ल्ड विज़न

चर्चा में क्यों?
ब्रिटेन और अमेरिका द्वारा कड़ी निंदा किए जाने के बाद रूस ने सूडान में युद्ध विराम के लिए ब्रिटेन समर्थित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के मसौदे पर वीटो लगा दिया है।
सूडान के बारे में:
- सूडान उत्तरपूर्वी अफ्रीका में स्थित है।
- इसकी सीमा दक्षिण सूडान, इथियोपिया, इरिट्रिया, मिस्र, लीबिया, चाड और मध्य अफ्रीकी गणराज्य से लगती है।
- यह देश उत्तर में सहारा रेगिस्तान से लेकर कांगो नदी बेसिन सहित पश्चिम अफ्रीका के जंगलों तक फैला हुआ है।
- सूडान की लाल सागर के किनारे एक महत्वपूर्ण तटरेखा है, जो स्वेज नहर के माध्यम से हिंद महासागर और भूमध्य सागर तक पहुंच के लिए महत्वपूर्ण है।
- राजधानी: राजधानी शहर खार्तूम, देश के लगभग मध्य में, ब्लू नील और व्हाइट नील नदियों के संगम पर स्थित है।
- मुद्रा: प्रयुक्त मुद्रा सूडानी पाउंड (एसडीजी) है।
औपनिवेशिक शासन:
- 19वीं सदी के आरम्भ में सूडान पर मिस्र का कब्ज़ा था।
- 1899 में एक समझौते के तहत संयुक्त ब्रिटिश-मिस्र प्रशासन की स्थापना हुई, जिससे सूडान प्रभावी रूप से एक ब्रिटिश उपनिवेश बन गया।
- 1956 में एंग्लो-मिस्र नियंत्रण से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से, इस्लाम-उन्मुख एजेंडे वाले सैन्य शासनों ने देश की राजनीति को प्रमुख रूप से प्रभावित किया है।
- 2011 में दक्षिण सूडान के अलग होने तक सूडान अफ्रीका का सबसे बड़ा देश था, जिसका क्षेत्रफल अफ्रीका के 8% से अधिक तथा वैश्विक भूमि क्षेत्र का लगभग 2% था।
- सूडान का एक महत्वपूर्ण भाग रेगिस्तान और शुष्क घास के मैदानों से युक्त है, तथा यहां विशाल मैदान और पठार फैले हुए हैं।
वर्तमान संकट:
- अप्रैल 2023 में सूडानी सेना और अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्सेज के बीच सत्ता संघर्ष शुरू हो गया, जो नागरिक शासन में एक योजनाबद्ध परिवर्तन से शुरू हुआ था।
- इस संघर्ष के परिणामस्वरूप हजारों लोगों की मृत्यु हुई है तथा विश्व में सबसे बड़ा विस्थापन संकट उत्पन्न हुआ है।
- वर्तमान में, सूडान की एक-तिहाई आबादी गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रही है, तथा अनुमान है कि यह संख्या बढ़कर 40% हो सकती है।
जीएस3/पर्यावरण
क्या जीवाश्म ईंधनों को परमाणु हथियारों की तरह विनियमित किया जाना चाहिए?
स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?
सरकारों और नागरिक समाज संगठनों का एक बढ़ता हुआ गठबंधन जीवाश्म ईंधन अप्रसार संधि (एफएफ-एनपीटी) की वकालत कर रहा है, जिसका उद्देश्य जीवाश्म ईंधनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना और नवीकरणीय ऊर्जा की ओर न्यायोचित बदलाव को बढ़ावा देना है।
के बारे में:
- एफएफ-एनपीटी की संकल्पना 2016 में की गई थी और इसे आधिकारिक तौर पर 2019 में लॉन्च किया गया था, जिसमें देशों के लिए जीवाश्म ईंधन निष्कर्षण को रोकना, मौजूदा उत्पादन को कम करना और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए एक न्यायोचित संक्रमण का प्रबंधन करना कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने का प्रस्ताव था।
- परमाणु हथियारों को विनियमित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संधियों से प्रेरित होकर, इस पहल का उद्देश्य जीवाश्म ईंधन के उत्पादन को सीमित करके और वैश्विक स्तर पर ऊर्जा तक समान पहुंच सुनिश्चित करके बढ़ते जलवायु संकट का समाधान करना है।
- पेरिस समझौते के समय से ही शुरू हुए एफएफ-एनपीटी को पूर्व संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून, स्वदेशी समुदायों और छोटे द्वीप राज्यों सहित उल्लेखनीय हस्तियों से समर्थन प्राप्त हुआ है।
- हाल के घटनाक्रमों में COP29 से लेकर बाकू में UNFCCC की चर्चाएं शामिल हैं, जहां 10 अतिरिक्त देश FF-NPT पर वार्ता में शामिल हुए, हालांकि उनके नामों का खुलासा नहीं किया गया है।
- इस संधि को प्रशांत क्षेत्र के 13 छोटे द्वीपीय विकासशील देशों, जैसे वानुअतु और तुवालु, के साथ-साथ कोलंबिया जैसे प्रमुख कोयला उत्पादक देशों ने भी समर्थन दिया है।
- ग्लोबल अलायंस फॉर बैंकिंग ऑन वैल्यूज़ के 25 सदस्यों का सामूहिक समर्थन इस पहल के लिए वित्तीय क्षेत्र का महत्वपूर्ण समर्थन दर्शाता है।
एफएफ-एनपीटी की आवश्यकता और महत्व:
- ज़रूरत:
- समर्थकों का तर्क है कि इसके महत्व के बावजूद, पेरिस समझौता जीवाश्म ईंधन उत्पादन को सीधे संबोधित नहीं करता है।
- एफएफ-एनपीटी पहल की अध्यक्ष त्ज़ेपोराह बर्मन ने सीओपी29 में वैश्विक उत्सर्जन की चिंताजनक प्रवृत्तियों का उल्लेख करते हुए भविष्यवाणी की कि 2024 में जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन 2015 के स्तर से 8% अधिक हो सकता है।
- अनुमान है कि 2024 अब तक का सबसे गर्म वर्ष होगा, क्योंकि जीवाश्म ईंधन का उत्पादन वैश्विक तापमान को 1.5°C तक सीमित रखने के लक्ष्य के अनुरूप नहीं है।
- वर्तमान नीतियों के कारण तापमान में 3°C तक की वृद्धि हो सकती है, जिससे मानवता के लिए भयावह खतरा उत्पन्न हो सकता है।
- जैसे-जैसे जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन बढ़ता जा रहा है, ग्रह के भविष्य के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है।
- महत्व:
- प्रस्तावित संधि का उद्देश्य पेरिस समझौते को सुदृढ़ बनाना है, विशेष रूप से नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य जैसी पहलों के माध्यम से, जिसका उद्देश्य 2025 के बाद विकासशील देशों में जलवायु संबंधी कार्यों को समर्थन देने के लिए नए वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करना है।
- इसका उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) और न्यायोचित परिवर्तन कार्य कार्यक्रमों को बढ़ाना भी है।
एफएफ-एनपीटी फ्रेमवर्क और चुनौतियों को समझना:
- रूपरेखा:
- एफएफ-एनपीटी तीन मुख्य स्तंभों पर आधारित है:
- अप्रसार: अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से कोयला, तेल और गैस उत्पादन में वृद्धि को रोकना।
- निष्पक्ष चरणबद्ध समाप्ति: मौजूदा जीवाश्म ईंधन उत्पादन को समान रूप से कम करना, ऐतिहासिक रूप से उच्च उत्सर्जन वाले धनी देशों को प्राथमिकता देना।
- न्यायोचित परिवर्तन: नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने को बढ़ावा देना तथा अर्थव्यवस्थाओं में विविधता लाना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी समुदाय, श्रमिक या राष्ट्र पीछे न छूट जाए।
- 2019 में अपने आधिकारिक शुभारंभ के बाद से, एफएफ-एनपीटी को महत्वपूर्ण वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, विशेष रूप से जलवायु-संवेदनशील देशों को जीवाश्म ईंधन से दूर जाने में सहायता करने में।
- पर्याप्त वित्तपोषण के बिना, विकासशील देशों को नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने या जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में कठिनाई होती है।
- एफएफ-एनपीटी तीन मुख्य स्तंभों पर आधारित है:
एफएफ-एनपीटी पर भारत की स्थिति और एफएफ-एनपीटी के लिए आगे की राह:
- भारत की स्थिति:
- यद्यपि भारत इसमें गहराई से शामिल नहीं रहा है, फिर भी एफएफ-एनपीटी पहल के महत्व को स्वीकार किया गया है।
- ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के अनुसार, एक प्रमुख जीवाश्म ईंधन उपभोक्ता के रूप में, भारत के उत्सर्जन में 2024 में 4.6% की वृद्धि होने का अनुमान है।
- अधिवक्ताओं का मानना है कि भारत इस संधि से लाभ उठा सकता है, जिससे वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन के दौरान न्याय और समानता सुनिश्चित हो सकेगी।
- पश्चिमी गोलार्ध:
- संधि को पेरिस समझौते के लक्ष्यों के अनुरूप होना चाहिए, तथा वित्तीय तंत्रों का समर्थन करना चाहिए...
निष्कर्ष:
- एफएफ-एनपीटी, परमाणु निरस्त्रीकरण के समान ही जीवाश्म ईंधन उत्पादन को विनियमित करके जलवायु संकट का समाधान करने के लिए एक साहसिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।
- सरकारों, वित्तीय संस्थाओं और कमजोर देशों से बढ़ते समर्थन के साथ, यह पहल वैश्विक सहयोग और न्यायसंगत समाधान की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।
- हालाँकि, इस दृष्टिकोण को कानूनी रूप से बाध्यकारी वास्तविकता में बदलने के लिए वित्तीय और राजनीतिक दोनों बाधाओं को दूर करना होगा।
जीएस1/भारतीय समाज
Ayushman Vay Vandana Yojana
स्रोत : मिंट
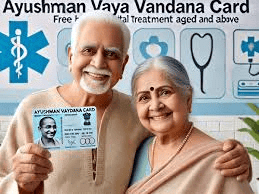
चर्चा में क्यों?
आयुष्मान वय वंदना योजना (AVVY) के लॉन्च होने के तीन सप्ताह के भीतर ही 10 लाख से ज़्यादा वरिष्ठ नागरिकों ने इसके लिए पंजीकरण करा लिया है। यह योजना विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाई गई है, जो उन्हें ज़रूरी स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है।
के बारे में
- आयुष्मान वय वंदना योजना भारत में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बीमा पॉलिसी के साथ जोड़ी गई पेंशन योजना है।
- इसे प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएम-वीवीवाई) से अलग करना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना खास तौर पर स्वास्थ्य सेवा लाभों पर केंद्रित है।
विशेषताएँ एवं प्रावधान
- 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक की कैशलेस स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करता है।
- लाभार्थियों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड दिया जाता है, जिससे उन्हें पूरे भारत में सूचीबद्ध अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है।
- कवरेज में चिकित्सा परामर्श, उपचार, अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद के खर्च तथा एंजियोप्लास्टी जैसी जटिल प्रक्रियाओं सहित सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है।
संरचनात्मक अधिदेश
- यह योजना पीएम-जेएवाई ढांचे के तहत संचालित की जाती है, जिससे भारत की स्वास्थ्य बीमा प्रणाली के साथ प्रभावी कार्यान्वयन और एकीकरण सुनिश्चित होता है।
- यह शहरी और ग्रामीण दोनों सूचीबद्ध अस्पतालों में कार्य करता है, तथा राष्ट्रव्यापी पहुंच प्रदान करता है।
- एक केंद्रीकृत डिजिटल प्रणाली उपचार, रोगी के विवरण और व्यय की निगरानी करती है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है।
- विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए तैयार की गई यह योजना उनकी विशिष्ट स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करती है।
लक्ष्य और उद्देश्य
- इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना है, तथा यह सुनिश्चित करना है कि उन्हें वित्तीय बोझ के बिना महत्वपूर्ण चिकित्सा उपचारों तक पहुंच प्राप्त हो।
- इसका उद्देश्य बुजुर्ग व्यक्तियों और उनके परिवारों के लिए जेब से होने वाले खर्च को कम करना है।
- आयु-संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए निवारक स्वास्थ्य देखभाल और शीघ्र चिकित्सा हस्तक्षेप को प्रोत्साहित करता है।
पात्रता मापदंड
- यह योजना 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी भारतीय नागरिकों के लिए खुली है।
- इसमें आय या परिवार के आकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, जिससे यह सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए उनकी आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना सुलभ है।
- लाभार्थियों को एवीवी कार्ड प्राप्त करने और लाभ प्राप्त करने के लिए पीएम-जेएवाई के तहत पंजीकरण कराना आवश्यक है।
जीएस3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी
एक दिन एक जीनोम पहल
स्रोत: पीआईबी

चर्चा में क्यों?
जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) और जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार परिषद (ब्रिक) ने भारत की विशाल सूक्ष्मजीव विविधता को उजागर करते हुए 'वन डे वन जीनोम' पहल शुरू की है।
- इस पहल का उद्देश्य भारत में मौजूद अद्वितीय जीवाणु प्रजातियों की ओर ध्यान आकर्षित करना है, तथा पर्यावरण, कृषि और मानव स्वास्थ्य में उनके महत्वपूर्ण योगदान पर ध्यान केंद्रित करना है।
- इसका समन्वय जैवप्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार परिषद-राष्ट्रीय जैवचिकित्सा जीनोमिक्स संस्थान (ब्रिक-एनआईबीएमजी) द्वारा किया जाता है, जो जैवप्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्य करता है।
- इस पहल के तहत भारत से पृथक किया गया पूर्णतः एनोटेट जीवाणु जीनोम जारी किया जाएगा, जिससे यह आम जनता के लिए निःशुल्क उपलब्ध हो जाएगा।
- इस विज्ञप्ति के साथ विस्तृत ग्राफिकल सारांश, इन्फोग्राफिक्स और जीनोम असेंबली/एनोटेशन विवरण भी होंगे।
- ये संसाधन इन सूक्ष्मजीवों के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुप्रयोगों के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे।
- इसका लक्ष्य माइक्रोबियल जीनोमिक्स डेटा की पहुंच को बढ़ाना है, जिससे आम जनता और शोधकर्ताओं को लाभ होगा, जिससे चर्चाओं और नवाचारों को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे समुदाय और पारिस्थितिकी तंत्र की भलाई में सुधार हो सकेगा।
सूक्ष्मजीवों की भूमिका
- पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन बनाए रखने के लिए सूक्ष्मजीव महत्वपूर्ण हैं।
- वे विभिन्न जैव-भू-रासायनिक चक्रों, मृदा निर्माण, खनिज शुद्धिकरण तथा कार्बनिक अपशिष्टों और विषाक्त पदार्थों के विघटन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
- सूक्ष्मजीव मीथेन उत्पादन में भी भूमिका निभाते हैं, तथा हमारे ग्रह के समग्र होमियोस्टैसिस को बनाए रखते हैं।
- कृषि में, वे पोषक चक्रण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं।
- वे कीट और खरपतवार नियंत्रण में सहायता करते हैं तथा पौधों को पर्यावरणीय तनाव का सामना करने में सहायता करते हैं।
- सूक्ष्मजीवों का पौधों के साथ सहजीवी संबंध होता है, जो पोषक तत्वों और जल अवशोषण में सहायता करते हैं।
- दिलचस्प बात यह है कि मानव शरीर में मानव कोशिकाओं की तुलना में अधिक सूक्ष्मजीव कोशिकाएं होती हैं, जो पाचन, प्रतिरक्षा कार्य और यहां तक कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- यद्यपि रोगजनक सूक्ष्मजीव संक्रामक रोगों के लिए जिम्मेदार होते हैं, किन्तु गैर-रोगजनक सूक्ष्मजीव भी ऐसे रोगों से हमारी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं।
जीएस2/शासन
CAG ने संसाधन-व्यय में 42% अंतर, 37% स्टाफ रिक्तियों की बात कही
स्रोत : इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने 18 राज्यों में शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के सामने आने वाली महत्वपूर्ण वित्तीय और परिचालन चुनौतियों को उजागर किया है, जो 241 मिलियन निवासियों की ज़रूरतें पूरी करते हैं। एक उल्लेखनीय निष्कर्ष यह है कि उनकी आय और व्यय के बीच 42% का अंतर है, जबकि विकास गतिविधियों के लिए बजट का केवल 29% ही आवंटित किया जाता है।
रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष
- संसाधन-व्यय अंतर : 18 राज्यों में शहरी स्थानीय निकायों की आय और व्यय के बीच काफी असमानता है, जहां केवल 29% व्यय ही विकास पहलों पर किया जाता है।
- राजस्व पर निर्भरता : ये निकाय अपने राजस्व का केवल 32% स्वतंत्र रूप से उत्पन्न करते हैं, तथा मुख्यतः केंद्र और राज्य सरकारों से प्राप्त धन पर निर्भर रहते हैं, तथा अपनी संपत्ति कर मांग का केवल 56% ही एकत्र कर पाते हैं।
- कर्मचारियों की कमी और सीमित भर्ती शक्तियां : शहरी स्थानीय निकायों को औसतन 37% कर्मचारियों की रिक्तियों का सामना करना पड़ता है, तथा 16 राज्यों ने उन्हें कर्मचारियों की भर्ती के लिए सीमित या कोई स्वायत्तता नहीं दी है।
- 74वें संशोधन का अपूर्ण कार्यान्वयन : यद्यपि औसतन 18 में से 17 कार्य हस्तांतरित कर दिए गए हैं, फिर भी अनुपालन अपर्याप्त बना हुआ है, विशेषकर शहरी नियोजन और अग्निशमन सेवाओं जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में।
संसाधन-व्यय अंतर के निहितार्थ
- विकास व्यय में कमी : केवल 29% व्यय आवश्यक कार्यक्रमों की ओर निर्देशित किया जाता है, जिससे स्वच्छता, आवास और बुनियादी ढांचे जैसी शहरी सेवाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- अनुदान पर निर्भरता में वृद्धि : केवल 32% राजस्व स्वतंत्र रूप से प्राप्त होने के कारण, शहरी स्थानीय निकाय राज्य और संघ सरकारों से प्राप्त होने वाले धन पर बहुत अधिक निर्भर हैं, जिससे उनकी वित्तीय स्वायत्तता प्रभावित होती है।
- खराब सेवा वितरण : सीमित संसाधन शहरी चुनौतियों का समाधान करने में यूएलबी की क्षमता को बाधित करते हैं, जिससे आवास, अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में समस्याएं पैदा होती हैं।
- शहरी नियोजन पर प्रभाव : वित्तीय बाधाएं शहरी नियोजन और महत्वपूर्ण सेवाओं में निवेश को प्रतिबंधित करती हैं, जिसके परिणामस्वरूप अनियमित विकास और बढ़ती हुई कमजोरियां होती हैं।
सरकारी कार्यों पर 37% स्टाफ रिक्ति दर का प्रभाव
- परिचालन अकुशलता : रिक्त पदों के कारण समय पर सेवा प्रदान करने और शहरी बुनियादी ढांचे के रखरखाव में बाधा आती है, जिससे शासन अकुशलता बढ़ती है।
- अत्यधिक कार्यभार से ग्रस्त कार्यबल : शेष कर्मचारियों को कार्यभार में वृद्धि का सामना करना पड़ेगा, जिससे थकान और उत्पादकता में कमी का खतरा रहेगा।
- संसाधन जुटाने की सीमित क्षमता : कर संग्रह कर्मचारियों की कमी के कारण संपत्ति कर की मांग का केवल 56% ही प्राप्त हो पाता है, जिससे राजस्व सृजन सीमित हो जाता है।
- कमजोर स्थानीय शासन : हस्तांतरित कार्यों के प्रबंधन के लिए पर्याप्त कार्मिकों की कमी शहरी विकास नीतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा डालती है।
शहरी स्थानीय निकाय क्या हैं?
- यूएलबी का गठन और संचालन 1992 में अधिनियमित भारतीय संविधान के 74वें संशोधन द्वारा शासित होता है, जो शहरी स्वशासन के लिए एक ढांचा स्थापित करता है।
- शहरी स्थानीय निकायों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: नगर निगम (बड़े शहरों के लिए), नगर पालिकाएं (छोटे शहरों के लिए), और नगर पंचायतें (संक्रमणकालीन क्षेत्रों के लिए)।
संसाधन जुटाने और प्रबंधन में सुधार के उपाय (आगे की राह)
- खुद का राजस्व सृजन बढ़ाना : शहरी स्थानीय निकायों को राजस्व संग्रह में सुधार करना चाहिए, खासकर संपत्ति कर में, जहां वे वर्तमान में मांग का केवल 56% ही प्राप्त कर पाते हैं। जीआईएस जैसी तकनीक को लागू करने से संग्रह दक्षता में वृद्धि हो सकती है।
- वित्तीय प्रबंधन प्रशिक्षण : वित्तीय प्रबंधन पर यूएलबी अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने से बजटीय कार्यप्रणाली में सुधार हो सकता है, तथा विकास परियोजनाओं के लिए धन का प्रभावी आवंटन सुनिश्चित हो सकता है।
- स्वायत्तता को सुदृढ़ बनाना : शहरी स्थानीय निकायों को भर्ती और वित्तीय निर्णयों में अधिक स्वायत्तता प्रदान करने से वे स्थानीय आवश्यकताओं को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा करने तथा सेवा वितरण को बढ़ाने में सक्षम होंगे।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) : निजी क्षेत्र की संस्थाओं के साथ भागीदारी को प्रोत्साहित करने से शहरी विकास के लिए अतिरिक्त संसाधन प्राप्त किए जा सकते हैं, साथ ही बड़े पैमाने पर निवेश के जोखिमों को भी साझा किया जा सकता है।
- सामुदायिक सहभागिता पहल : बजट प्रक्रिया में नागरिकों को शामिल करने से पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे सामुदायिक प्राथमिकताओं के अनुरूप संसाधनों का बेहतर आवंटन हो सकेगा।
मेन्स पीवाईक्यू
स्थानीय स्तर पर सुशासन प्रदान करने में स्थानीय निकायों की भूमिका का विश्लेषण करें तथा ग्रामीण स्थानीय निकायों को शहरी स्थानीय निकायों के साथ विलय करने के लाभ और हानि पर चर्चा करें। (यूपीएससी आईएएस/2024)
|
3127 docs|1043 tests
|
















