The Hindi Editorial Analysis- 19th June 2025 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC PDF Download
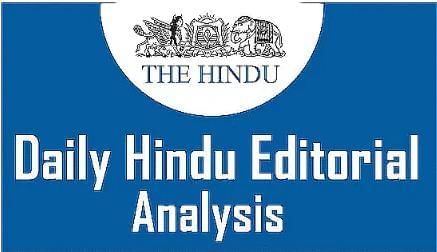
उचित हिस्सा
यह समाचार क्यों है?
सोलहवें वित्त आयोग (एसएफसी) पर चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि उसे 1 अप्रैल, 2026 से भारत में केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व का बंटवारा किस प्रकार किया जाए, इस पर निर्णय लेना है।
- 28 राज्यों में से 22 राज्यों, जिनमें भाजपा शासित राज्य भी शामिल हैं, की ओर से विभाज्य कर पूल में अपना हिस्सा 41% से बढ़ाकर 50% करने की महत्वपूर्ण मांग की गई है।
- यह मांग इसलिए आवश्यक मानी जा रही है, क्योंकि केंद्र गैर-साझाकरणीय उपकरों और अधिभारों पर अधिक निर्भर रहा है, जिससे राज्यों के कर राजस्व में वास्तविक हिस्सेदारी कम हो जाती है।
परिचय
सोलहवें वित्त आयोग (एसएफसी), जो 1 अप्रैल, 2026 से अपना काम शुरू करने वाला है, को भारत में राजकोषीय संघवाद को फिर से परिभाषित करने के चुनौतीपूर्ण कार्य का सामना करना पड़ रहा है। 28 में से 22 राज्यों की मांगों के कारण यह कार्य अत्यावश्यक हो गया है, जिनमें से कई भाजपा शासित हैं, जो विभाज्य कर पूल में अपने हिस्से को 41% से बढ़ाकर 50% करने की मांग कर रहे हैं।
ये मांगें गैर-साझा करने योग्य उपकरों और अधिभारों पर केंद्र की बढ़ती निर्भरता पर बढ़ती चिंता को उजागर करती हैं, जिसने राष्ट्रीय कर राजस्व में राज्यों के वास्तविक हिस्से को प्रभावी रूप से कम कर दिया है। केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों का उचित और संतुलित वितरण सुनिश्चित करने के लिए एसएफसी को इन जटिल मुद्दों पर काम करना होगा।
सोलहवां वित्त आयोग (एसएफसी)
- प्रभावी अवधि: 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल, 2026 से लागू होंगी।
- अध्यक्ष: अरविंद पनगढ़िया, जिन्होंने हाल ही में राज्यों द्वारा उठाई गई राजकोषीय चिंताओं को उजागर किया।
- केंद्रीय मुद्दा: बढ़ते राजकोषीय केंद्रीकरण के बीच ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण (केंद्र और राज्यों के बीच) और क्षैतिज हस्तांतरण (राज्यों के बीच) में संतुलन स्थापित करना।
राज्यों की प्रमुख मांगें
- राज्यों के हिस्से में वृद्धि: 28 में से 22 राज्य, जिनमें भाजपा शासित कई राज्य भी शामिल हैं, विभाज्य कर पूल में अपने हिस्से को 41% से बढ़ाकर 50% करने की मांग कर रहे हैं।
- तर्क: वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन के बाद राजकोषीय स्वायत्तता के क्षरण के कारण यह मांग वैध मानी जाती है।
विभाज्य पूल का सिकुड़ना
केंद्र के सकल कर राजस्व में उपकर और अधिभार का हिस्सा
| अवधि | केंद्र के सकल कर राजस्व में उपकर और अधिभार का हिस्सा |
|---|---|
| 2015-16 से 2019-20 (पूर्व-कोविड) | 12.8% |
| 2020-21 से 2023-24 (कोविड-पश्चात बजट वर्ष) | 18.5% |
निहितार्थ:
- गैर-साझाकरणीय उपकरों और अधिभारों में वृद्धि से केन्द्रीय कर राजस्व में राज्यों की प्रभावी हिस्सेदारी काफी कम हो गई है।
सकल कर राजस्व में राज्यों की प्रभावी हिस्सेदारी
| अवधि | सकल कर राजस्व में राज्यों की प्रभावी हिस्सेदारी |
|---|---|
| 2015-16 से 2019-20 | ~35% |
| 2020-21 से 2023-24 | ~31% |
जीएसटी और राज्यों की राजकोषीय स्वायत्तता
जीएसटी के बाद की चुनौतियाँ:
- सीमित राजस्व मार्ग: वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन के बाद से राज्यों के पास अपना राजस्व उत्पन्न करने के कम विकल्प हैं।
- जीएसटी राजस्व संबंधी मुद्दे: यद्यपि जीएसटी राजस्व में वृद्धि हो रही है, लेकिन इससे राज्यों को हुई राजकोषीय स्वतंत्रता की हानि की भरपाई नहीं हो पाती है।
- केंद्र पर निर्भरता: राज्य अब अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केंद्र से वित्तीय हस्तांतरण पर बहुत अधिक निर्भर हैं।
क्षैतिज हस्तांतरण: सूत्र संबंधी चिंताएं
- जनसंख्या मानदंड: यह मानदंड उच्च जनसंख्या वाले राज्यों को लाभ पहुंचाता है, लेकिन प्रगतिशील शासन और विकास वाले राज्यों को दंडित करता है।
- आय अंतर मानदंड: यह मानदंड गरीब राज्यों की मदद करता है, लेकिन इसे उन राज्यों को दंडित करने के रूप में माना जाता है जो कुशल हैं और जिनमें आय असमानताएं कम हैं।
- दक्षिणी और प्रगतिशील राज्यों का परिप्रेक्ष्य: इन राज्यों का तर्क है कि वर्तमान फार्मूला उनके सुशासन और विकास प्रयासों के लिए उन्हें दंडित करता है, जिससे क्षैतिज हस्तांतरण प्रक्रिया में असंतुलन पैदा होता है।
वित्त आयोग के समक्ष चुनौतियां
- 41% ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण को बनाए रखना: वर्तमान ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण दर को 41% बनाए रखने से सहकारी संघवाद कमजोर हो सकता है और संघीय समझौते को संशोधित करने का अवसर चूक सकता है।
- केंद्र की बाधाएं: केंद्र को रक्षा और पूंजीगत व्यय में वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है, जिससे वह अपने राजकोषीय हिस्से को कम करने में अनिच्छुक है। अरविंद पनगढ़िया ने बताया है कि विकेंद्रीकरण में उल्लेखनीय वृद्धि मौजूदा संतुलन को बिगाड़ सकती है और संघर्ष पैदा कर सकती है।
आगे बढ़ने का रास्ता
- राज्यों के हिस्से में मामूली वृद्धि: आयोग को केंद्र की व्यय आवश्यकताओं का सम्मान करते हुए राजकोषीय असंतुलन को दूर करने के लिए विभाज्य पूल में राज्यों के हिस्से को लगभग 44-45% तक बढ़ाने पर विचार करना चाहिए।
- उपकर और अधिभार का विनियमन: उपकर और अधिभार की सीमा तय करने के लिए सिफारिशें होनी चाहिए, तथा पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए किसी भी अधिशेष को विभाज्य पूल में शामिल करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- क्षैतिज हस्तांतरण सूत्र का संशोधन: समानता और प्रदर्शन को संतुलित करने के लिए सूत्र को संशोधित किया जाना चाहिए, कुशल शासन को पुरस्कृत करते हुए कम विकसित राज्यों का समर्थन करना चाहिए। इससे एक अधिक न्यायसंगत राजकोषीय ढांचा तैयार होगा और सहकारी संघवाद मजबूत होगा।
निष्कर्ष
सोलहवें वित्त आयोग के पास ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण को बढ़ाकर, गैर-पारदर्शी राजस्व साधनों को विनियमित करके और क्षैतिज वितरण में सुधार करके भारत में राजकोषीय संघवाद को नया आकार देने का अवसर है। ऐसा करके, यह राज्यों की राजकोषीय नींव को मजबूत कर सकता है, जो भारतीय लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है, और एक अधिक न्यायसंगत और सहकारी राजकोषीय ढांचा तैयार कर सकता है।
अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इज़रायली कार्रवाई की वैधता
यह समाचार क्यों है?
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस प्रश्न पर विचार कर रहा है कि क्या ईरान पर इजरायल के सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत वैध हैं।
- संयुक्त राष्ट्र चार्टर, विशेष रूप से अनुच्छेद 2(4), अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बल के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाता है, सिवाय अनुच्छेद 51 के अनुसार आत्मरक्षा जैसे विशिष्ट मामलों को छोड़कर।
- अनुच्छेद 51 केवल सशस्त्र हमले के जवाब में आत्मरक्षा की अनुमति देता है, और प्रतिक्रिया आवश्यक एवं आनुपातिक होनी चाहिए।
- कानूनी विशेषज्ञों का तर्क है कि यदि आत्मरक्षा की सख्ती से व्याख्या की जाए तो इजरायल की कार्रवाई को गैरकानूनी आक्रमण माना जा सकता है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत युद्ध अपराध है।
परिचय
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ईरान के खिलाफ इजरायल के सैन्य हमलों की वैधता पर विभाजित है, जिसमें मुख्य मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय कानून का अनुपालन है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर, विशेष रूप से अनुच्छेद 2(4), अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बल के उपयोग को प्रतिबंधित करता है, केवल अनुच्छेद 51 के तहत आत्मरक्षा जैसे मामलों में अपवाद की अनुमति देता है। अनुच्छेद 51 केवल सशस्त्र हमले के जवाब में आत्मरक्षा की अनुमति देता है, और प्रतिक्रिया को आवश्यकता और आनुपातिकता के मानदंडों को पूरा करना चाहिए। कानूनी विशेषज्ञों का सुझाव है कि यदि आत्मरक्षा की संकीर्ण रूप से व्याख्या की जाती है, तो इजरायल की कार्रवाई को गैरकानूनी आक्रमण माना जा सकता है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत युद्ध अपराध है।
पूर्व-निवारक आत्मरक्षा
इजराइल का तर्क है कि ईरान के खिलाफ उसकी सैन्य कार्रवाई पूर्व-प्रतिरोधक आत्मरक्षा पर आधारित है, जिसका उद्देश्य ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम को विफल करना है। तर्क यह है कि ईरान परमाणु हथियार विकसित करने की कगार पर है और उसने इजराइल के खिलाफ धमकियाँ जारी की हैं, जिसके लिए पूर्व-प्रतिरोधक हमला ज़रूरी है। इससे एक महत्वपूर्ण कानूनी सवाल उठता है: क्या किसी देश के लिए वास्तविक सशस्त्र हमला होने से पहले बल प्रयोग करना जायज़ है?
संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 51 आम तौर पर सशस्त्र हमले के बाद ही आत्मरक्षा की अनुमति देता है, जिससे पूर्व-प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई विरोधाभासी लगती है। हालांकि, रोज़लिन हिगिंस जैसे कुछ कानूनी विद्वानों का तर्क है कि समकालीन युद्ध में वास्तविक हमले की प्रतीक्षा करना अवास्तविक हो सकता है। यदि पूर्व-प्रतिक्रियात्मक आत्मरक्षा को स्वीकार किया जाता है, तो दुरुपयोग को रोकने के लिए इसके मापदंडों को संकीर्ण रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। एक अधिक व्यापक रूप से स्वीकृत अवधारणा प्रत्याशित आत्मरक्षा है, जिसे 1837 की कैरोलीन घटना जैसे ऐतिहासिक उदाहरणों में समर्थन मिलता है।
कैरोलीन सिद्धांत की व्याख्या
कैरोलीन सिद्धांत उन परिस्थितियों को रेखांकित करता है जिनके तहत अग्रिम आत्मरक्षा में बल का इस्तेमाल किया जा सकता है। इन परिस्थितियों में शामिल हैं:
- तात्कालिकता: खतरा तत्काल और भारी होना चाहिए।
- आवश्यकता: कोई वैकल्पिक कार्यवाही उपलब्ध नहीं होनी चाहिए, तथा विचार-विमर्श के लिए समय नहीं होना चाहिए।
- आनुपातिकता: प्रतिक्रिया खतरे के अनुपात में होनी चाहिए।
आत्मरक्षा से संबंधित कानूनी अवधारणाएँ
| अवधारणा | परिभाषा | अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत कानूनी स्थिति | उदाहरण / संदर्भ |
|---|---|---|---|
| आत्मरक्षा | वास्तविक सशस्त्र हमले के जवाब में बल का प्रयोग | संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत अनुमति दी गई | रॉकेट हमलों के बाद इजराइल |
| पूर्व-निवारक आत्मरक्षा | भविष्य में संभावित हमले के विरुद्ध बल प्रयोग | विवादास्पद, आम तौर पर अवैध माना जाता है | ईरान के विरुद्ध इजराइल का दावा |
| पूर्वानुमानित आत्मरक्षा | जब हमला आसन्न हो तो बल का प्रयोग | कैरोलीन सिद्धांत के तहत सशर्त स्वीकार किया गया | कैरोलीन घटना (1837) |
पूर्व-प्रतिरोधी आत्मरक्षा की अवधारणा कानूनी और नैतिक बहस का विषय बनी हुई है। यदि इसे अनुमति दी जानी है, तो इसके आवेदन को तत्कालता, आवश्यकता और आनुपातिकता सहित सख्त मानदंडों का पालन करना होगा। अत्यधिक व्यापक व्याख्या संयुक्त राष्ट्र चार्टर को कमजोर कर सकती है और राज्यों द्वारा आक्रामक कार्रवाइयों को वैध बनाने का जोखिम उठा सकती है।
आत्मरक्षा में 'आसन्न' की व्याख्या
| प्रकार | स्पष्टीकरण | आशय |
|---|---|---|
| प्रतिबंधात्मक (अस्थायी) | - हमला होने वाला है। - अस्थायी निकटता पर ध्यान केंद्रित करता है। | - पारंपरिक अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप है। - सीमित आत्मरक्षा का समर्थन करता है। |
| प्रशस्त | - हमला भविष्य में किसी समय हो सकता है। - समयबद्ध नहीं। | - शक्तिशाली राज्यों द्वारा एकतरफा कार्रवाई का जोखिम। - सशस्त्र आक्रमण को प्रोत्साहन। |
विस्तृत अर्थ के प्रति प्रमुख कानूनी आपत्तियाँ
- बल प्रयोग के निषेध पर संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।
- अनुमान आधारित कार्रवाई की अनुमति देकर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कमजोर करता है।
- यह कैरोलीन सिद्धांत का खंडन करता है, जो आत्मरक्षा के लिए कठोर शर्तें निर्धारित करता है:
- तत्काल होना चाहिए
- भाव विह्वल करने वाला
- विचार-विमर्श के लिए कोई जगह न छोड़ें
- 'आसन्न' की संकीर्ण, प्रतिबंधात्मक व्याख्या के लिए व्यापक समर्थन।
- संयम सुनिश्चित करता है, तथा संप्रभुता और कानूनी सुरक्षा को कायम रखता है।
इजराइल-ईरान संदर्भ में अनुप्रयोग
इजराइल का दावा
- ईरान के परमाणु खतरे के विरुद्ध पूर्व-प्रतिरोधी आत्मरक्षा
कानूनी मूल्यांकन
- आसन्नता के प्रतिबंधात्मक परीक्षण को पूरा करने में विफल रहता है।
- संभावित भावी खतरे पर आधारित, आसन्न खतरे पर नहीं।
परमाणु प्रगति के कारण अस्तित्व पर खतरा होने का दावा
- यह व्यापक अर्थ पर निर्भर करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून में समर्थित नहीं है।
निष्कर्ष
ईरान के खिलाफ इजरायल की सैन्य कार्रवाइयों के बारे में चल रही बहस अंतरराष्ट्रीय कानून और बल के इस्तेमाल को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की जटिलताओं को उजागर करती है। जबकि कुछ लोग तर्क दे सकते हैं कि इन कानूनी ढाँचों पर चर्चा करना एक ऐसी दुनिया में निरर्थक है जहाँ उन्हें अक्सर नज़रअंदाज़ किया जाता है, यह याद रखना ज़रूरी है कि अंतरराष्ट्रीय कानून राज्य के व्यवहार का आकलन करने और उन्हें जवाबदेह ठहराने का आधार प्रदान करता है। शक्तिशाली राज्यों द्वारा गंभीर उल्लंघन के मामलों में भी इन कानूनी मानदंडों को बनाए रखना और लागू करना, नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।
|
3101 docs|1040 tests
|
FAQs on The Hindi Editorial Analysis- 19th June 2025 - Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC
| 1. अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इज़रायली कार्रवाई की वैधता क्या है? |  |
| 2. इज़राइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष के प्रमुख ऐतिहासिक कारण क्या हैं? |  |
| 3. अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का इज़राइली कार्रवाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? |  |
| 4. संयुक्त राष्ट्र का इज़राइल के खिलाफ क्या रुख है? |  |
| 5. फिलिस्तीनी अधिकारों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयास क्या हैं? |  |















