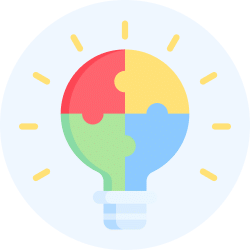ल्हासा की ओर NCERT Solutions | Hindi Class 9 (Kritika and Kshitij) PDF Download
| Table of contents |

|
| प्रश्न-अभ्यास |

|
| रचना और अभिव्यक्ति |

|
| भाषा-अध्ययन |

|
| पाठेतर-सक्रियता |

|
प्रश्न-अभ्यास
प्रश्न 1: थोंगला के पहले के आख़िरी गाँव पहुँचने पर भिखमंगे के वेश में होने के वावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों ?
उत्तर: इसका मुख्य कारण था — संबंधों का महत्व। तिब्बत में इस मार्ग पर यात्रियों के लिए एक जैसी व्यवस्थाएँ नहीं थीं। इसलिए वहाँ जान-पहचान के आधार पर ठहरने के लिए उचित स्थान मिल जाता था। पहली बार लेखक के साथ बौद्ध भिक्षु सुमति थे, जिनकी वहाँ अच्छी जान-पहचान थी। परंतु पाँच साल बाद बहुत कुछ बदल गया था। भद्र वेश में होने पर भी लेखक को उचित स्थान नहीं मिला और उन्हें बस्ती की सबसे गरीब झोपड़ी में रुकना पड़ा। यह सब वहाँ के लोगों की मनोवृत्ति में आए बदलाव के कारण हुआ होगा। वहाँ के लोग शाम होते ही छंङ पीकर होश खो देते थे, और इस बार सुमति भी साथ नहीं थे।
प्रश्न 2: उस समय के तिब्बत में हथियार का क़ानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था ?
उत्तर: उस समय के तिब्बत में हथियार रखने से संबंधित कोई क़ानून नहीं था। इस कारण लोग खुलेआम पिस्तौल, बंदूक आदि रखते थे। साथ ही, वहाँ अनेक निर्जन स्थान भी थे, जहाँ न तो पुलिस की व्यवस्था थी और न ही खुफिया विभाग का कोई नियंत्रण। ऐसे स्थानों पर डाकू किसी को भी आसानी से मार सकते थे। इसीलिए यात्रियों को हत्या और लूटपाट का भय बना रहता था।

प्रश्न 3: लेखक लङ्कोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गए थे?
उत्तर: लेखक का घोड़ा थक गया था, इसलिए वह धीरे चल रहा था और लेखक अकेले ही रास्ता भटक गए। वह रास्ता भूलकर एक से डेढ़ किलोमीटर गलत दिशा में चले गए, जहाँ से उन्हें वापस लौटना पड़ा। इसी कारण लेखक लङ्कोर के मार्ग में अपने साथियों से पिछड़ गए।
प्रश्न 4: लेखक ने शेकर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परन्तु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया ?
उत्तर: लेखक ने शेकर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से इसलिए रोका था ताकि वह वहाँ जाकर अधिक समय न लगाए, जिससे लेखक को एक सप्ताह तक उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती। परन्तु दूसरी बार लेखक को वहाँ के मंदिर में रखी अनेक मूल्यवान हस्तलिखित पुस्तकें मिल गई थीं। वह एकांत में उनका अध्ययन करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सुमति को यजमानों के पास जाने से नहीं रोका।
प्रश्न 5: अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाईयों का सामना करा पड़ा?
उत्तर: लेखक को इस यात्रा के दौरान अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा:
- जगह-जगह रास्ता कठिन था और परिवेश भी बिल्कुल नया था।
- उनका घोड़ा बहुत सुस्त था, जिसके कारण लेखक अपने साथियों से बिछड़ गया और अकेले में रास्ता भूल गया।
- डाकुओं जैसे दिखने वाले लोगों से भीख माँगनी पड़ी।
- भिखारी के वेश में यात्रा करनी पड़ी।
- समय से न पहुँच पाने पर सुमति के गुस्से का सामना करना पड़ा।
- तेज़ धूप में चलना पड़ा।
- वापस आते समय लेखक को रुकने के लिए उचित स्थान नहीं मिला।
प्रश्न 6: प्रस्तुत यात्रा-वृत्तान्त के आधार पर बताइए की उस समय का तिब्बती समाज कैसा था?
उत्तर: प्रस्तुत यात्रा-वृत्तान्त के आधार पर उस समय के तिब्बती समाज के बारे में निम्न बातें पता चलती हैं:
- तिब्बती समाज में छुआछूत, जाति-पाँति जैसी कुप्रथाएँ नहीं थीं।
- सारे प्रबंध की देखभाल कोई भिक्षु करता था, जिसे जागीर के लोगों में राजा के समान सम्मान प्राप्त था।
- तिब्बती महिलाएँ उस समय परदा नहीं करती थीं।
- तिब्बत की ज़मीन जागीरदारों में बँटी हुई थी, जिसका अधिकांश भाग मठों के पास होता था।
प्रश्न 7: 'मैं अब पुस्तकों के भीतर था ।'नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन -सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है?
(क) लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया।
(ख) लेखक पुस्तकों की शैल्फ़ के भीतर चला गया।
(ग) लेखक के चारों ओर पुस्तकें हैं थीं।
(घ) पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था।
उत्तर: (क) लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया।
रचना और अभिव्यक्ति
प्रश्न 8: सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गाँव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं?
उत्तर: सुमति के यजमानों और परिचितों के हर गाँव में मिलने से उनकी अनेक विशेषताओं का पता चलता है, जैसे:
- सुमति मिलनसार और हँसमुख व्यक्ति थे, जिनकी जान-पहचान का दायरा बहुत विस्तृत था।
- वे अपने यजमानों को बोधगया से लाए कपड़े के गंडे बनाकर देते थे और बदले में दक्षिणा लेते थे।
- सुमति लोगों की आस्था का अनुचित लाभ उठाते थे, लेकिन यह बात लोगों को पता नहीं चलने देते थे।
- वे बौद्ध धर्म में गहरी आस्था रखते थे।
प्रश्न 9: 'हालाँकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी खयाल करना चाहिए था'। - उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार-व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से यह उचित है अथवा अनुचित, विचार व्यक्त करें।
उत्तर: यह बात सच है कि हमारे आचार-व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। हम अच्छा पहनावा देखकर किसी को अपनाते हैं, तो गंदे कपड़े देखकर उसे दुत्कार देते हैं। लेखक भिखमंगों के वेश में यात्रा कर रहा था, इसलिए उसे यह अपेक्षा नहीं थी कि शेखर विहार का भिक्षु उसे सम्मानपूर्वक अपनाएगा।
मेरे विचार से वेशभूषा देखकर व्यवहार करना पूरी तरह उचित नहीं है। अनेक संत-महात्मा और भिक्षु साधारण वस्त्र पहनते हैं, किंतु वे उच्च चरित्र के व्यक्ति होते हैं और पूज्य होते हैं। परंतु यह बात भी सत्य है कि वेशभूषा से मनुष्य की एक पहली पहचान बनती है। हम पर पहला प्रभाव वेशभूषा के कारण ही पड़ता है और अक्सर उसी के आधार पर भले-बुरे की पहचान करते हैं।
प्रश्न 10: यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द -चित्र प्रस्तुत करें। वहाँ की स्थिति आपके राज्य/शहर से किस प्रकार भिन्न है ?
उत्तर: तिब्बत की सीमाएँ भारत और नेपाल से लगती हैं। तिब्बत भारत के उत्तर में स्थित है, जहाँ कुछ समय तक आने-जाने पर प्रतिबंध था। यह स्थान समुद्र तल से सत्रह–अठारह हजार फीट ऊँचे डाँड़ों पर स्थित है, जो खतरनाक क्षेत्र है। यहाँ एक ओर हिमालय की ऊँची चोटियाँ हैं तो दूसरी ओर नंगे पहाड़ हैं। यहाँ की जलवायु भी अनुपम है। एक ओर हजारों बर्फ से ढके श्वेत शिखर हैं, दूसरी ओर विशाल मैदान भी हजारों पहाड़ों से घिरे हुए हैं। यहाँ की जलवायु में सूर्य की ओर मुँह करके चलने पर माथा जलता है, जबकि कंधा और पीठ बर्फ की तरह ठंडी हो जाती है। यह स्थिति हमारे देश/राज्य से पूरी तरह भिन्न है।
प्रश्न 11: आपने भी किसी स्थान की यात्रा अवश्य की होगी? यात्रा के दौरान हुए अनुभवों को लिखकर प्रस्तुत करें।
उत्तर: गर्मी की छुट्टियों में इस बार मैं अपने माता-पिता और भाई के साथ वृंदावन घूमने गई। सबको मेरा प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा। हम सब 2 जून को अपनी गाड़ी में बैठकर प्रातः 5 बजे वृंदावन के लिए रवाना हुए। गाड़ी से वृंदावन तक का सफर लगभग 7 घंटे का है। जब तक हम वहाँ पहुँचे, तब तक हम सभी काफी थक चुके थे। वहाँ पहुँचकर हमने रहने के लिए धर्मशाला का इंतजाम किया। वहाँ हमने तरह-तरह के मंदिर घूमे। वहाँ के कुछ प्रसिद्ध मंदिर जैसे कि बाँके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर, निधिवन, इस्कॉन मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर भी देखे। हम वहाँ 3 दिनों तक रहे और फिर वापस आते समय हम आगरा की ओर रवाना हुए। आगरा पहुँचकर हमने ताजमहल देखा, जो बहुत ही सुंदर बना हुआ था। आगरा घूमते-घूमते हमारा पूरा दिन निकल गया। फिर रात को अपनी गाड़ी में बैठकर हम वापस अपने घर के लिए रवाना हुए। पूरा सफर बहुत ही सुखद रहा। पूरे परिवार को बहुत आनंद आया। जब भी हमारी रिश्तेदारों से बात होती है तो हम उन्हें वृंदावन जाने के लिए ज़रूर कहते हैं।
प्रश्न 12: यात्रा-वृत्तांत गद्य साहित्य की एक विधा है। आपकी इस पाठ्यपुस्तक में कौन -कौन सी विधाएँ हैं? प्रस्तुत विधा उनसे किन मायनों में अलग है ?
उत्तर: प्रस्तुत पाठ्यपुस्तक में महादेवी वर्मा द्वारा रचित "मेरे बचपन के दिन" एक संस्मरणहै। संस्मरण भी गद्य साहित्य की एक प्रमुख विधा है। इसमें लेखिका ने अपने बचपन की यादों का एक अंश प्रस्तुत किया है।
यात्रा-वृत्तांत और संस्मरण दोनों ही गद्य साहित्य की विधाएँ हैं, लेकिन दोनों में अंतर है:
- यात्रा-वृत्तांत किसी स्थान की यात्रा के अनुभवों पर आधारित होता है।
- जबकि संस्मरण किसी व्यक्ति, स्थान या जीवन की किसी विशेष घटना से जुड़ी स्मृतियों पर आधारित होता है।
इस प्रकार, संस्मरण का दायरा यात्रा-वृत्तांत से अधिक व्यापक होता है क्योंकि यह केवल यात्रा तक सीमित नहीं होता।
भाषा-अध्ययन
प्रश्न 13: किसी बात को अनेक प्रकार से कहा जा सकता है ; जैसे -
सुबह होने से पहले हम गाँव में थे।
पौ फटने वाला था कि हम गाँव में थे।
तारों की छाँव रहते-रहते हम गाँव पहुँच गए।
नीचे दिए गए वाक्य को अलग-अलग तरीकों में लिखिए -
' जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। '
उत्तर:
- यह पता ही नहीं चल पा रहा था कि घोड़ा चल भी रहा है या नहीं।
- कभी लगता था घोड़ा आगे जा रहा है, कभी लगता था पीछे जा रहा है।
प्रश्न 14: ऐसे शब्द जो किसी अंचल यानी क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त होते हैं उन्हें आंचलिक शब्द कहा जाता है। प्रस्तुत पाठ में से आंचलिक शब्द ढूँढकर लिखिए। पाठ में आए हुए आंचलिक शब्द -
उत्तर: कुची-कुची, भीटा, थुक्पा, खोटी, राहदारी
प्रश्न 15: पाठ में कागज़, अक्षर, मैदान के आगे क्रमश : मोटे, अच्छे और विशाल शब्दों का प्रयोग हुआ है। इन शब्दों से उनकी विशेषता उभर कर आती है। पाठ में से कुछ ऐसे ही और शब्द छाँटिए जो किसी की विशेषता बता रहे हों।
उत्तर: इस पाठ में प्रयुक्त विशेषण शब्द (जो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की विशेषता बताते हैं) निम्नलिखित हैं: मुख्य, व्यापारिक, सैनिक, फ़ौजी, चीनी, बहुत-से, परित्यक्त, टोटीदार, सारा, दोनों, आख़िरी, अच्छी, भद्र, ग़रीब, विकट, निर्जन, हज़ारों, श्वेत, बिल्कुल नंगे, सर्वोच्च, रंग-बिरंगे, थोड़ी, गरमागरम, विशाल, छोटी-सी, कितने-ही, पतली-पतली चिरी बत्तियाँ।
पाठेतर-सक्रियता
प्रश्न: यह यात्रा राहुल जी ने 1930 में की थी। आज के समय यदि तिब्बत की यात्रा की जाए तो राहुल जी की यात्रा से कैसे भिन्न होगी?
उत्तर: राहुल जी ने जब 1930 में तिब्बत की यात्रा की थी, तब रास्ते बहुत कठिन थे। उस समय न तो अच्छे वाहन थे और न ही सड़कें। उन्हें पैदल या खच्चरों पर बैठकर जाना पड़ा था। खाने-पीने की चीजें भी आसानी से नहीं मिलती थीं और मौसम से बचने के साधन भी कम थे।
लेकिन आज अगर कोई तिब्बत जाए, तो वह कार, ट्रेन या हवाई जहाज से आसानी से जा सकता है। आज अच्छे होटल, सड़कें और मोबाइल जैसी सुविधाएँ भी मिलती हैं। इसलिए आज की यात्रा पहले से कहीं ज़्यादा आसान, आरामदायक और सुरक्षित होगी।
प्रश्न: क्या आपके किसी परिचित को घुमक्कड़ी/यायावरी का शौक है? उसके इस शौक का उसकी पढ़ाई/काम आदि पर क्या प्रभाव पड़ता होगा, लिखें।
उत्तर: हाँ, मेरे एक परिचित को घुमक्कड़ी का बहुत शौक है। वह समय मिलते ही नई जगहों पर घूमने चले जाते हैं।
उनके इस शौक से उन्हें बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है — जैसे नई भाषाएँ, संस्कृति, रहन-सहन और लोगों से मिलना। इससे उनकी जानकारी बढ़ती है और पढ़ाई या काम में भी मदद मिलती है।
कभी-कभी ज्यादा घूमने से पढ़ाई या काम में थोड़ी रुकावट आ सकती है, लेकिन अगर समय को अच्छे से बाँटा जाए तो यह शौक बहुत फायदेमंद हो सकता है।
प्रश्न: अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए-
आम दिनों में समुद्र किनारे के इलाके बेहद खूबसूरत लगते हैं। समुद्र लाखों लोगों को भोजन देता है और लाखों उससे जुड़े दूसरे कारोबारों में लगे हैं। दिसंबर 2004 को सुनामी या समुद्री भूकंप से उठने वाली तूफ़ानी लहरों के प्रकोप ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि कुदरत की यह देन सबसे बड़े विनाश का कारण भी बन सकती है।
प्रकृति कब अपने ही ताने-बाने को उलट कर रख देगी, कहना मुश्किल है। हम उसके बदलते मिजाज को उसका कोप कह लें या कुछ और, मगर यह अबूझ पहेली अकसर हमारे विश्वास के चीथड़े कर देती है और हमें यह अहसास करा जाती है कि हम एक कदम आगे नहीं, चार कदम पीछे हैं। एशिया के एक बड़े हिस्से में आने वाले उस भूकंप ने कई द्वीपों को इधर-उधर खिसकाकर एशिया का नक्शा ही बदल डाला। प्रकृति ने पहले भी अपनी ही दी हुई कई अद्भुत चीजें इंसान से वापस ले ली हैं जिसकी कसक अभी तक है।
दुख जीवन को माँजता है, उसे आगे बढ़ने का हुनर सिखाता है। वह हमारे जीवन में ग्रहण लाता है, ताकि हम पूरे प्रकाश की अहमियत जान सकें और रोशनी को बचाए रखने के लिए जतन करें। इस जतन से सभ्यता और संस्कृति का निर्माण होता है। सुनामी के कारण दक्षिण भारत और विश्व के अन्य देशों में जो पीड़ा हम देख रहे हैं, उसे निराशा के चश्मे से न देखें। ऐसे समय में भी मेघना, अरुण और मैगी जैसे बच्चे हमारे जीवन में जोश, उत्साह और शक्ति भर देते हैं। 13 वर्षीय मेघना और अरुण
दो दिन अकेले खारे समुद्र में तैरते हुए जीव-जंतुओं से मुकाबला करते हुए किनारे आ लगे। इंडोनेशिया की रिजा पड़ोसी के दो बच्चों को पीठ पर लादकर पानी के बीच तैर रही थी कि एक विशालकाय साँप ने उसे किनारे का रास्ता दिखाया। मछुआरे की बेटी मैगी ने रविवार को समुद्र का भयंकर शोर सुना, उसकी शरारत को समझा, तुरंत अपना बेड़ा उठाया और अपने परिजनों को उस पर बिठा उतर आई समुद्र में, 41 लोगों को लेकर। महज 18 साल की जलपरी चल पड़ी पगलाए सागर से दो-दो हाथ करने। दस मीटर से ज्यादा ऊँची सुनामी लहरें जो कोई बाधा, रुकावट मानने को तैयार नहीं थीं, इस लड़की के बुलंद इरादों के सामने बौनी ही साबित हुईं।
जिस प्रकृति ने हमारे सामने भारी तबाही मचाई है, उसी ने हमें ऐसी ताकत और सूझ दे रखी है कि हम फिर से खड़े होते हैं और चुनौतियों से लड़ने का एक रास्ता ढूंढ निकालते हैं। इस त्रासदी से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए जिस तरह पूरी दुनिया एकजुट हुई है, वह इस बात का सबूत है कि मानवती हार नहीं मानती।
(1) कौन-सी आपदा को सुनामी कहा जाता है?
उत्तर: भीषण भूकंप के कारण समुद्र में आने वाली तूफ़ानी लहरों को सुनामी कहा जाता है। यह आसपास के इलाकों को नष्ट कर देता है।
(2) ‘दुख जीवन को माँजता है, उसे आगे बढ़ने का हुनर सिखाता है’-आशय स्पष्ट कीजिए।
उत्तर: दुख जीवन को साफ़-सुथरा बनाता है। अर्थात् व्यक्ति दुख से निपटने के उपाय सोचता है, उनसे छुटकारा पाता है। भविष्य में इससे बचने की तैयारी कर लेता है और नई आशा, उमंग और उल्लास के साथ जीवन शुरू करता है।
(3) मैगी, मेघना और अरुण ने सुनामी जैसी आपदा का सामना किस प्रकार किया?
उत्तर: मेघना और अरुण सुनामी में फँस गए थे, वे दो दिन तक समुद्र में तैरते रहे। कई बार वे समुद्री जीवों का शिकार होने से बचे और अंत में किनारे लगकर बच गए। मैगी ने समुद्र में उठ रही दस मीटर ऊँची लहरों के बीच अपना बेड़ा उतार दिया। उसमें अपने परिजनों को बिठाकर किनारे आने के लिए संघर्ष करने लगी। उसके बेड़े में 41 लोग और भी थे।
(4) प्रस्तुत गद्यांश में ‘दृढ़ निश्चय’ और ‘महत्त्व’ के लिए किन शब्दों का प्रयोग हुआ है?
उत्तर: बुलंद इरादे, अहमियत।
(5) इस गद्यांश के लिए शीर्षक ‘नाराज़ समुद्र’ हो सकती है। आप कोई अन्य शीर्षक दीजिए।
उत्तर: “सुनामी का कहर’ या प्रकृति का क्रोध-सुनामी।
|
16 videos|226 docs|43 tests
|
FAQs on ल्हासा की ओर NCERT Solutions - Hindi Class 9 (Kritika and Kshitij)
| 1. क्या ल्हासा भारत में स्थित है? |  |
| 2. ल्हासा किस देश की राजधानी है? |  |
| 3. क्या ल्हासा के बारे में और अधिक जानकारी मिल सकती है? |  |
| 4. ल्हासा का मुख्य धर्मस्थल कौन-कौन से हैं? |  |
| 5. ल्हासा के मौसम कैसे होते हैं? |  |